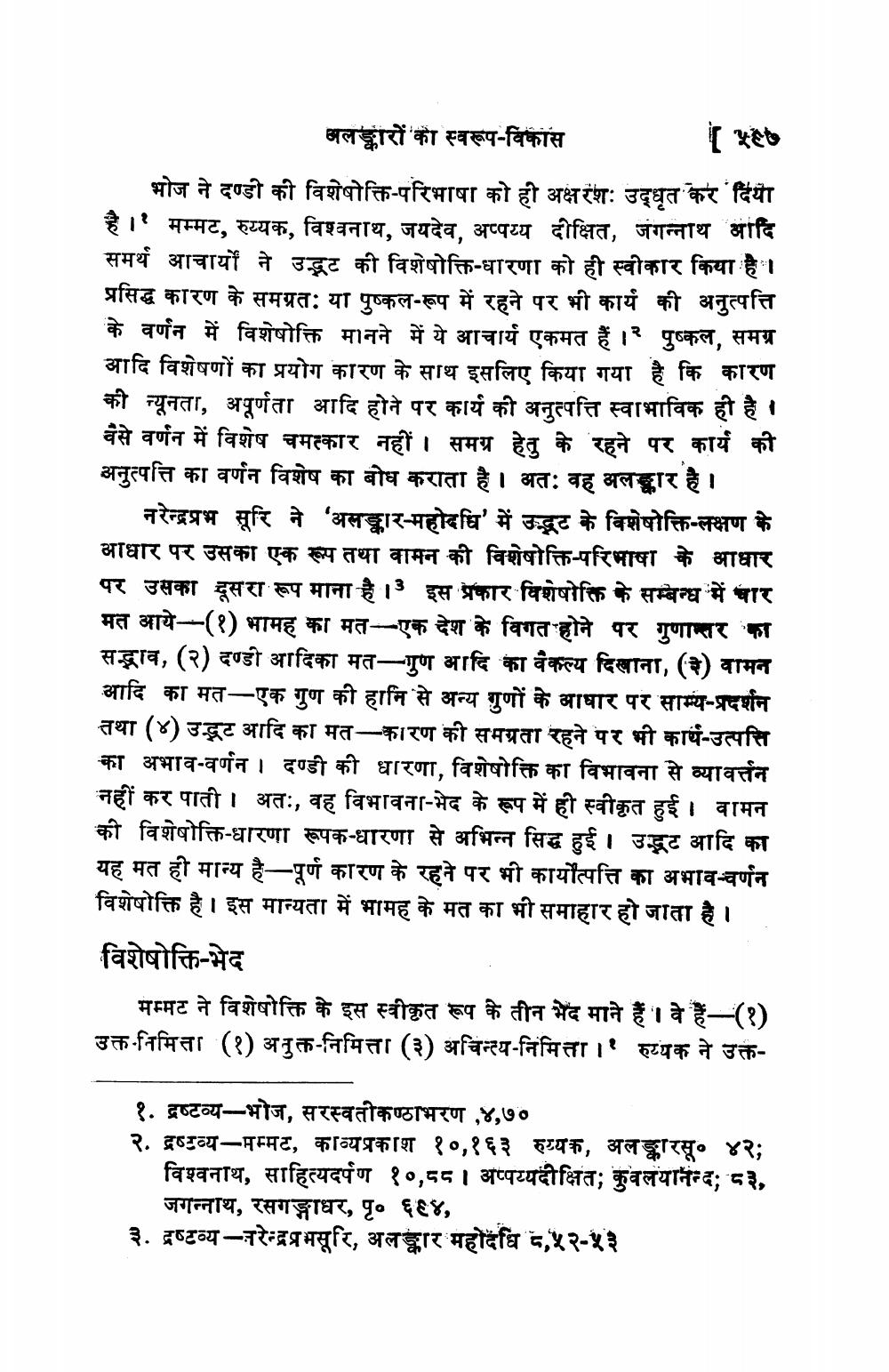________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[५६७ भोज ने दण्डी की विशेषोक्ति-परिभाषा को ही अक्षरशः उद्धृत कर दिया है।' मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, जयदेव, अप्पय्य दीक्षित, जंगन्नाथ आदि समर्थ आचार्यों ने उद्भट की विशेषोक्ति-धारणा को ही स्वीकार किया है । प्रसिद्ध कारण के समग्रत: या पुष्कल-रूप में रहने पर भी कार्य की अनुत्पत्ति के वर्णन में विशेषोक्ति मानने में ये आचार्य एकमत हैं ।२ पुष्कल, समग्र आदि विशेषणों का प्रयोग कारण के साथ इसलिए किया गया है कि कारण की न्यूनता, अपूर्णता आदि होने पर कार्य की अनुत्पत्ति स्वाभाविक ही है। वैसे वर्णन में विशेष चमत्कार नहीं। समग्र हेतु के रहने पर कार्य की अनुत्पत्ति का वर्णन विशेष का बोध कराता है। अत: वह अलङ्कार है। ___ नरेन्द्रप्रभ सूरि ने 'असङ्कार-महोदधि' में उद्धृट के विशेषोक्ति-लक्षण के आधार पर उसका एक रूप तथा वामन की विशेषोक्ति-परिभाषा के आधार पर उसका दूसरा रूप माना है। इस प्रकार विशेषोक्ति के सम्बन्ध में चार मत आये-(१) भामह का मत-एक देश के विगत होने पर गुणान्तर का सद्भाव, (२) दण्डी आदिका मत-गुण आदि का वैकल्य दिखाना, (३) वामन आदि का मत-एक गुण की हानि से अन्य गुणों के आधार पर साम्य-प्रदर्शन तथा (४) उद्भट आदि का मत-कारण की समग्रता रहने पर भी कार्य-उत्पत्ति का अभाव-वर्णन। दण्डी की धारणा, विशेषोक्ति का विभावना से व्यावर्त्तन नहीं कर पाती। अतः, वह विभावना-भेद के रूप में ही स्वीकृत हुई। वामन की विशेषोक्ति-धारणा रूपक-धारणा से अभिन्न सिद्ध हुई। उद्भट आदि का यह मत ही मान्य है-पूर्ण कारण के रहने पर भी कार्योत्पत्ति का अभाव-वर्णन विशेषोक्ति है। इस मान्यता में भामह के मत का भी समाहार हो जाता है। विशेषोक्ति-भेद
मम्मट ने विशेषोक्ति के इस स्वीकृत रूप के तीन भेद माने हैं। वे हैं-(१) उक्त निमिता (१) अनुक्त-निमित्ता (३) अचिन्त्य-निमित्ता।' रुय्यक ने उक्त
१. द्रष्टव्य-भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण ,४,७० २. द्रष्टव्य-मम्मट, काव्यप्रकाश १०,१६३ रुय्यक, अलङ्कारसू. ४२; विश्वनाथ, साहित्यदर्पण १०,८८ । अप्पय्यदीक्षित; कुवलयानन्द; ८३,
जगन्नाथ, रसगङ्गाधर, पृ० ६६४, ३. द्रष्टव्य-जरेन्द्रप्रभसूरि, अलङ्कार महोदधि ८,५२-५३