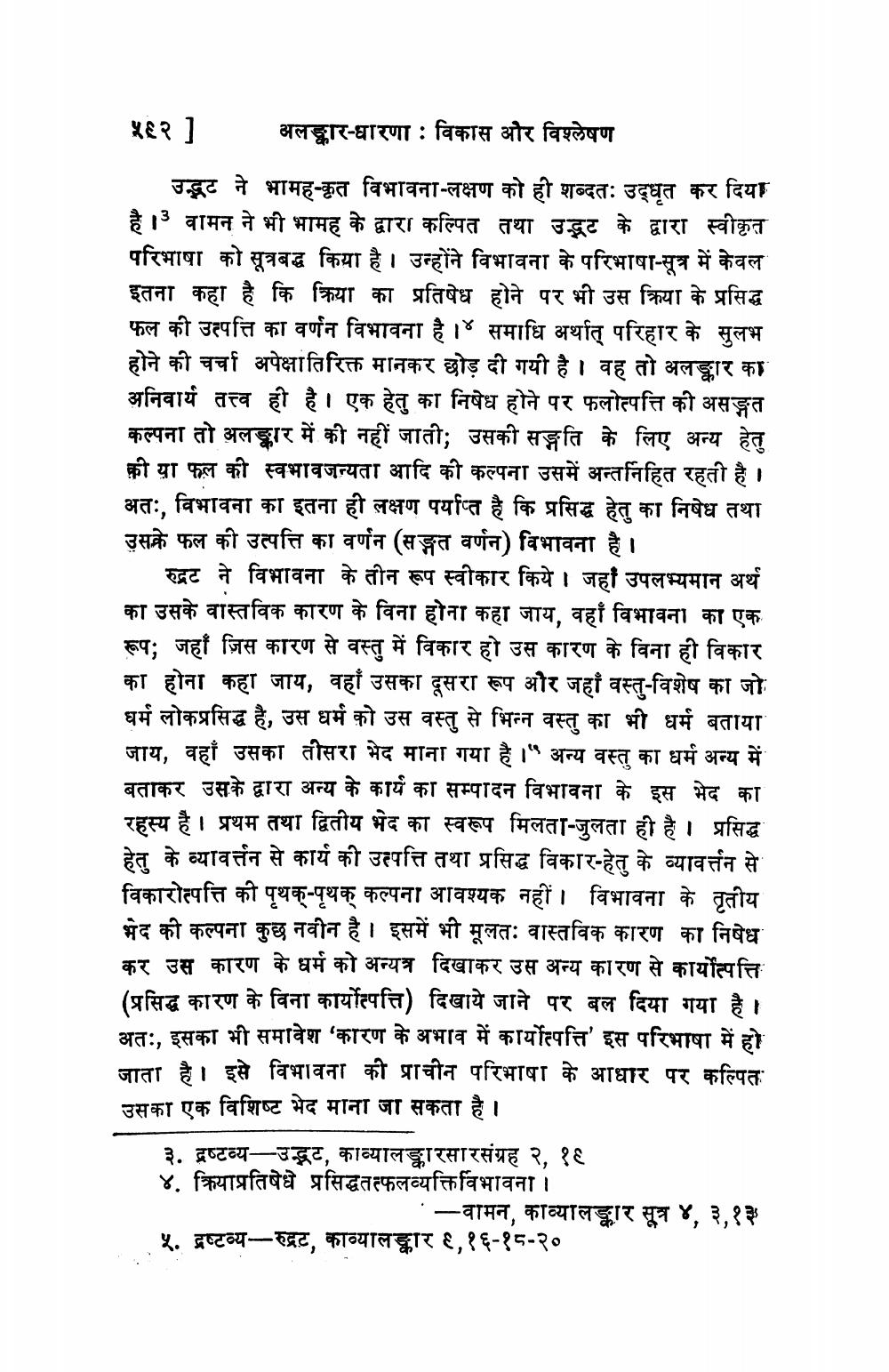________________
५६२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
उद्भट ने भामह-कृत विभावना-लक्षण को ही शब्दतः उद्धृत कर दिया है।3 वामन ने भी भामह के द्वारा कल्पित तथा उद्भट के द्वारा स्वीकृत परिभाषा को सूत्रबद्ध किया है। उन्होंने विभावना के परिभाषा-सूत्र में केवल इतना कहा है कि क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी उस क्रिया के प्रसिद्ध फल की उत्पत्ति का वर्णन विभावना है। समाधि अर्थात् परिहार के सुलभ होने की चर्चा अपेक्षा तिरिक्त मानकर छोड़ दी गयी है। वह तो अलङ्कार का अनिवार्य तत्त्व ही है। एक हेतु का निषेध होने पर फलोत्पत्ति की असङ्गत कल्पना तो अलङ्कार में की नहीं जाती; उसकी सङ्गति के लिए अन्य हेतु की या फल की स्वभावजन्यता आदि की कल्पना उसमें अन्तर्निहित रहती है। अतः, विभावना का इतना ही लक्षण पर्याप्त है कि प्रसिद्ध हेतु का निषेध तथा उसके फल की उत्पत्ति का वर्णन (सङ्गत वर्णन) विभावना है। ___ रुद्रट ने विभावना के तीन रूप स्वीकार किये। जहां उपलभ्यमान अर्थ का उसके वास्तविक कारण के विना होना कहा जाय, वहाँ विभावना का एक रूप; जहाँ जिस कारण से वस्तु में विकार हो उस कारण के विना ही विकार का होना कहा जाय, वहाँ उसका दूसरा रूप और जहाँ वस्तु-विशेष का जो धर्म लोकप्रसिद्ध है, उस धर्म को उस वस्तु से भिन्न वस्तु का भी धर्म बताया जाय, वहाँ उसका तीसरा भेद माना गया है। अन्य वस्तु का धर्म अन्य में बताकर उसके द्वारा अन्य के कार्य का सम्पादन विभावना के इस भेद का रहस्य है। प्रथम तथा द्वितीय भेद का स्वरूप मिलता-जुलता ही है। प्रसिद्ध हेत के व्यावर्तन से कार्य की उत्पत्ति तथा प्रसिद्ध विकार-हेतु के व्यावर्तन से विकारोत्पत्ति की पृथक्-पृथक् कल्पना आवश्यक नहीं। विभावना के तृतीय भेद की कल्पना कुछ नवीन है। इसमें भी मूलतः वास्तविक कारण का निषेध कर उस कारण के धर्म को अन्यत्र दिखाकर उस अन्य कारण से कार्योत्पत्ति (प्रसिद्ध कारण के विना कार्योत्पत्ति) दिखाये जाने पर बल दिया गया है। अतः, इसका भी समावेश 'कारण के अभाव में कार्योत्पत्ति' इस परिभाषा में हो जाता है। इसे विभावना की प्राचीन परिभाषा के आधार पर कल्पित उसका एक विशिष्ट भेद माना जा सकता है।
३. द्रष्टव्य-उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह २, १६ ४. क्रियाप्रतिषेधे प्रसिद्धतत्फलव्यक्तिविभावना।
-वामन, काव्यालङ्कार सूत्र ४, ३,१३ ५. द्रष्टव्य-रुद्रट, काव्यालङ्कार ६,१६-१८-२०