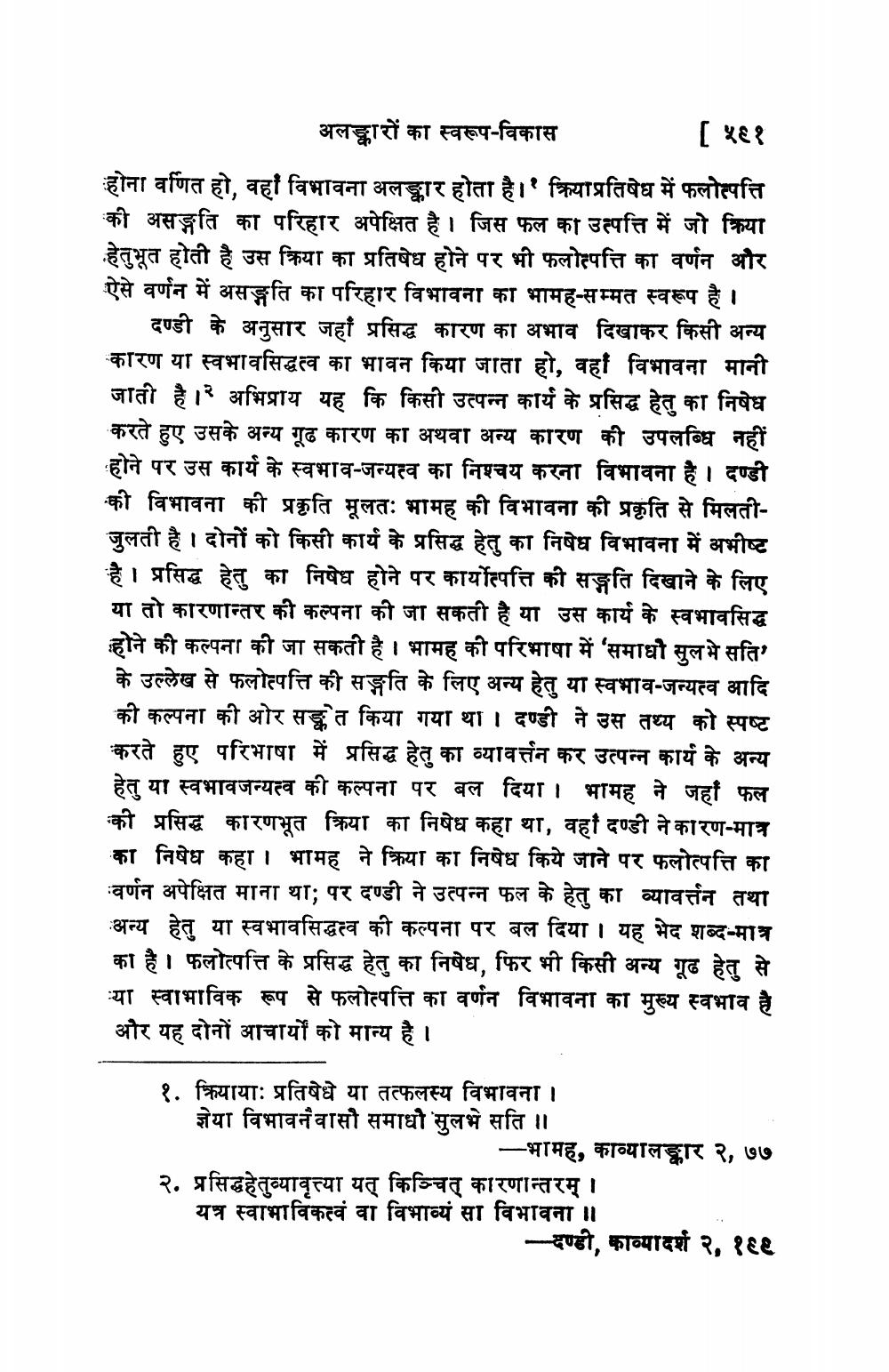________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ५६१ होना वर्णित हो, वहां विभावना अलङ्कार होता है। क्रियाप्रतिषेध में फलोत्पत्ति की असङ्गति का परिहार अपेक्षित है। जिस फल का उत्पत्ति में जो क्रिया हेतुभूत होती है उस क्रिया का प्रतिषेध होने पर भी फलोत्पत्ति का वर्णन और ऐसे वर्णन में असङ्गति का परिहार विभावना का भामह-सम्मत स्वरूप है।
दण्डी के अनुसार जहां प्रसिद्ध कारण का अभाव दिखाकर किसी अन्य कारण या स्वभावसिद्धत्व का भावन किया जाता हो, वहीं विभावना मानी जाती है। अभिप्राय यह कि किसी उत्पन्न कार्य के प्रसिद्ध हेतु का निषेध करते हुए उसके अन्य गूढ कारण का अथवा अन्य कारण की उपलब्धि नहीं होने पर उस कार्य के स्वभाव-जन्यत्व का निश्चय करना विभावना है। दण्डी की विभावना की प्रकृति मूलतः भामह की विभावना की प्रकृति से मिलतीजुलती है। दोनों को किसी कार्य के प्रसिद्ध हेतु का निषेध विभावना में अभीष्ट है। प्रसिद्ध हेतु का निषेध होने पर कार्योत्पत्ति की सङ्गति दिखाने के लिए या तो कारणान्तर की कल्पना की जा सकती है या उस कार्य के स्वभावसिद्ध होने की कल्पना की जा सकती है । भामह की परिभाषा में 'समाधी सुलभे सति' के उल्लेख से फलोत्पत्ति की सङ्गति के लिए अन्य हेतु या स्वभाव-जन्यत्व आदि की कल्पना की ओर सङ्कत किया गया था। दण्डी ने उस तथ्य को स्पष्ट करते हुए परिभाषा में प्रसिद्ध हेतु का व्यावर्तन कर उत्पन्न कार्य के अन्य हेतु या स्वभावजन्यत्व की कल्पना पर बल दिया। भामह ने जहाँ फल की प्रसिद्ध कारणभूत क्रिया का निषेध कहा था, वहाँ दण्डी ने कारण-मात्र का निषेध कहा। भामह ने क्रिया का निषेध किये जाने पर फलोत्पत्ति का वर्णन अपेक्षित माना था; पर दण्डी ने उत्पन्न फल के हेतु का व्यावर्त्तन तथा अन्य हेतु या स्वभावसिद्धत्व की कल्पना पर बल दिया। यह भेद शब्द-मात्र का है। फलोत्पत्ति के प्रसिद्ध हेतु का निषेध, फिर भी किसी अन्य गूढ हेतु से या स्वाभाविक रूप से फलोत्पत्ति का वर्णन विभावना का मुख्य स्वभाव है और यह दोनों आचार्यों को मान्य है।
१. क्रियायाः प्रतिषेधे या तत्फलस्य विभावना। ज्ञेया विभावनवासी समाधी सुलभे सति ॥
–भामह, काव्यालङ्कार २, ७७ २. प्रसिद्धहेतुव्यावृत्त्या यत् किञ्चित् कारणान्तरम् । यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना ॥
-दण्डी, काव्यादर्श २, १९९