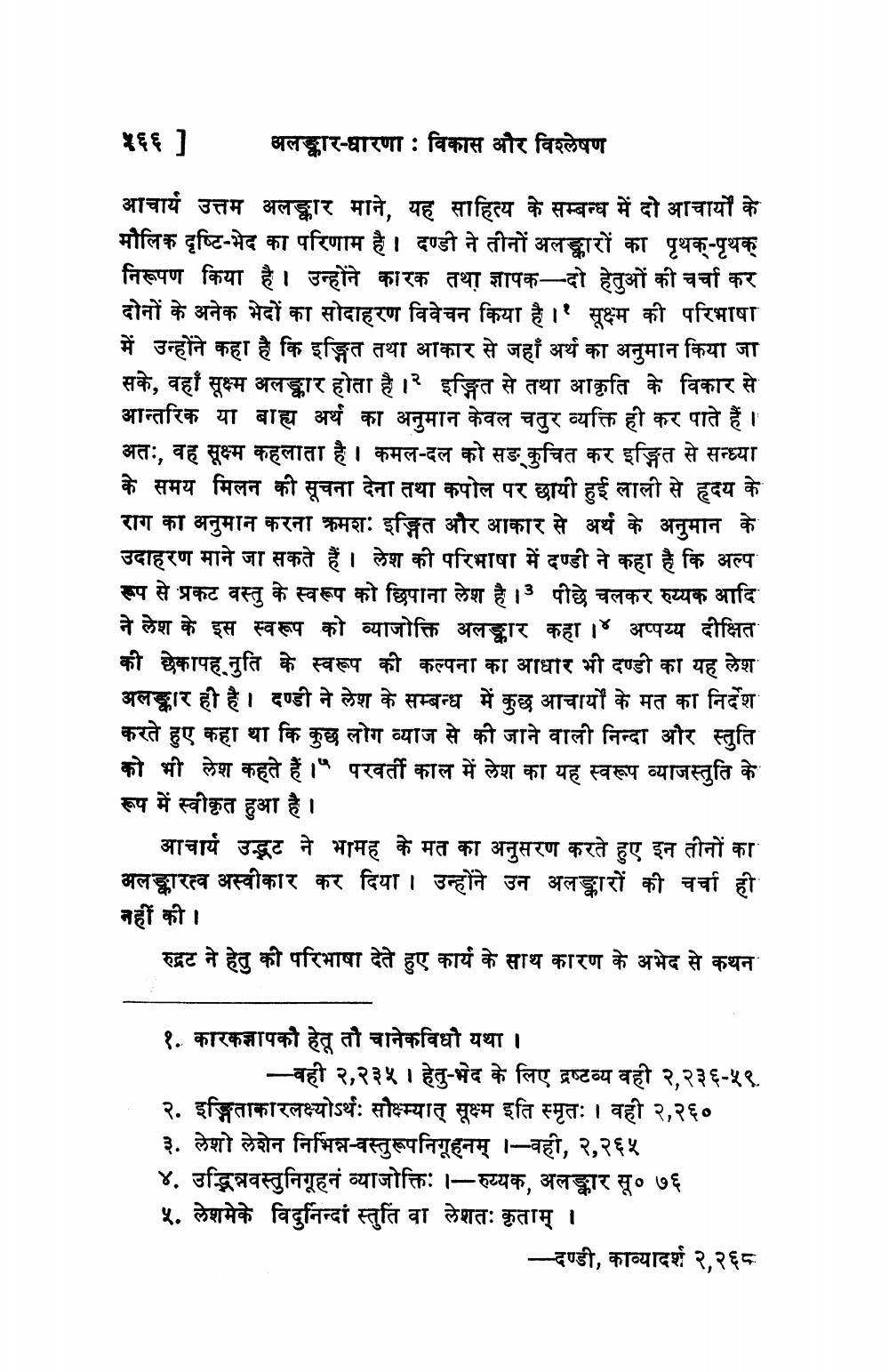________________
५६६ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
ર
आचार्य उत्तम अलङ्कार माने, यह साहित्य के सम्बन्ध में दो आचार्यों के मौलिक दृष्टि-भेद का परिणाम है । दण्डी ने तीनों अलङ्कारों का पृथक्-पृथक् निरूपण किया है । उन्होंने कारक तथा ज्ञापक — दो हेतुओं की चर्चा कर दोनों के अनेक भेदों का सोदाहरण विवेचन किया है। सूक्ष्म की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि इङ्गित तथा आकार से जहाँ अर्थ का अनुमान किया जा सके, वहाँ सूक्ष्म अलङ्कार होता है । २ इङ्गित से तथा आकृति के विकार से आन्तरिक या बाह्य अर्थ का अनुमान केवल चतुर व्यक्ति ही कर पाते हैं । अतः, वह सूक्ष्म कहलाता है । कमल-दल को सङ कुचित कर इङ्गित से सन्ध्या के समय मिलन की सूचना देना तथा कपोल पर छायी हुई लाली से हृदय के राग का अनुमान करना क्रमशः इङ्गित और आकार से अर्थ के अनुमान के उदाहरण माने जा सकते हैं । लेश की परिभाषा में दण्डी ने कहा है कि अल्प रूप से प्रकट वस्तु के स्वरूप को छिपाना लेश है । 3 पीछे चलकर रुय्यक आदि ने लेश के इस स्वरूप को व्याजोक्ति अलङ्कार कहा । अप्पय्य दीक्षित की छेकापह नुति के स्वरूप की कल्पना का आधार भी दण्डी का यह लेश अलङ्कार ही है । दण्डी ने लेश के सम्बन्ध में कुछ आचार्यों के मत का निर्देश करते हुए कहा था कि कुछ लोग व्याज से की जाने वाली निन्दा और स्तुति को भी लेश कहते हैं । " परवर्ती काल में लेश का यह स्वरूप व्याजस्तुति के रूप में स्वीकृत हुआ है ।
आचार्य उद्भट ने भामह के मत का अनुसरण करते हुए इन तीनों का अलङ्कारत्व अस्वीकार कर दिया । उन्होंने उन अलङ्कारों की चर्चा ही नहीं की ।
रुद्रट ने हेतु की परिभाषा देते हुए कार्य के साथ कारण के अभेद से कथन
१. कारकज्ञापको हेतू तो चानेकविधो यथा ।
— वही २,२३५ । हेतु-भेद के लिए द्रष्टव्य वही २, २३६-५९. २. इङ्गिताकारलक्ष्योऽर्थः सौक्ष्म्यात् सूक्ष्म इति स्मृतः । वही २,२६० ३. लेशो लेशेन निभिन्न वस्तुरूप निगूहनम् । - वही, २,२६५ ४. उद्भिन्नवस्तुनिगूहनं व्याजोक्तिः । - रुय्यक, अलङ्कार सू० ७६ ५. लेशमेके विदुनिन्दां स्तुतिं वा लेशतः कृताम् ।
दण्डी, काव्यादर्श २,२६८