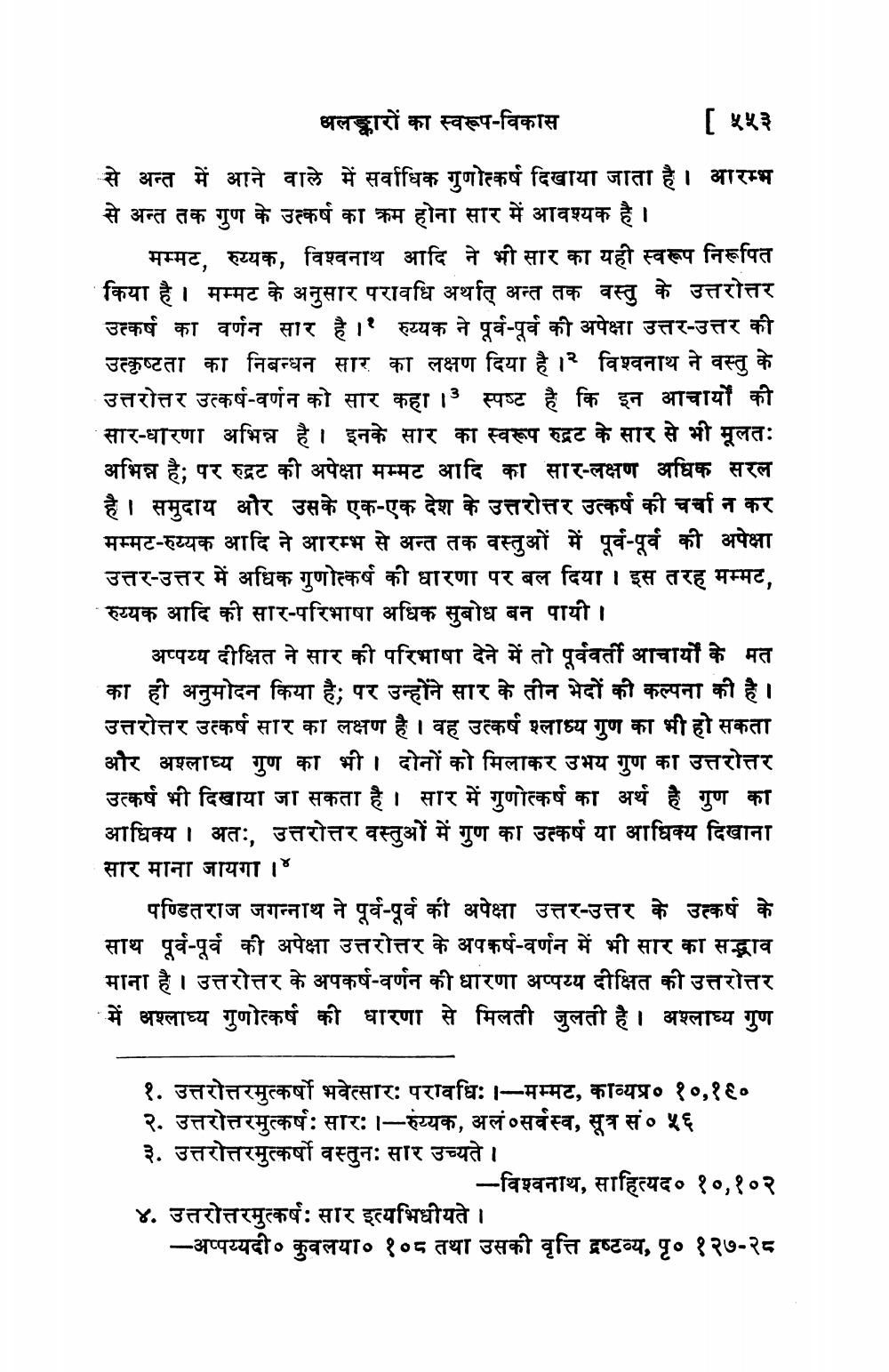________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ५५३ से अन्त में आने वाले में सर्वाधिक गुणोत्कर्ष दिखाया जाता है। आरम्भ से अन्त तक गुण के उत्कर्ष का क्रम होना सार में आवश्यक है। ____ मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि ने भी सार का यही स्वरूप निरूपित किया है। मम्मट के अनुसार परावधि अर्थात् अन्त तक वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष का वर्णन सार है।' रुय्यक ने पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर की उत्कृष्टता का निबन्धन सार का लक्षण दिया है ।२ विश्वनाथ ने वस्तु के उत्तरोत्तर उत्कर्ष-वर्णन को सार कहा । स्पष्ट है कि इन आचार्यों की सार-धारणा अभिन्न है। इनके सार का स्वरूप रुद्रट के सार से भी मूलतः अभिन्न है; पर रुद्रट की अपेक्षा मम्मट आदि का सार-लक्षण अधिक सरल है। समुदाय और उसके एक-एक देश के उत्तरोत्तर उत्कर्ष की चर्चा न कर मम्मट-रुय्यक आदि ने आरम्भ से अन्त तक वस्तुओं में पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर में अधिक गुणोत्कर्ष की धारणा पर बल दिया । इस तरह मम्मट, रुय्यक आदि की सार-परिभाषा अधिक सुबोध बन पायी। __ अप्पय्य दीक्षित ने सार की परिभाषा देने में तो पूर्ववर्ती आचार्यों के मत का ही अनुमोदन किया है; पर उन्होंने सार के तीन भेदों की कल्पना की है। उत्तरोत्तर उत्कर्ष सार का लक्षण है । वह उत्कर्ष श्लाध्य गुण का भी हो सकता और अश्लाघ्य गुण का भी। दोनों को मिलाकर उभय गुण का उत्तरोत्तर उत्कर्ष भी दिखाया जा सकता है। सार में गुणोत्कर्ष का अर्थ है गुण का आधिक्य । अतः, उत्तरोत्तर वस्तुओं में गुण का उत्कर्ष या आधिक्य दिखाना सार माना जायगा ।
पण्डितराज जगन्नाथ ने पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तर-उत्तर के उत्कर्ष के साथ पूर्व-पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर के अपकर्ष-वर्णन में भी सार का सद्भाव माना है। उत्तरोत्तर के अपकर्ष-वर्णन की धारणा अप्पय्य दीक्षित की उत्तरोत्तर में अश्लाघ्य गुणोत्कर्ष की धारणा से मिलती जुलती है। अश्लाघ्य गुण
१. उत्तरोत्तरमुत्कर्षो भवेत्सारः परावधिः।-मम्मट, काव्यप्र० १०,१६० २. उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सारः।-रुय्यक, अलं०सर्वस्व, सूत्र सं० ५६ ३. उत्तरोत्तरमुत्कर्षो वस्तुनः सार उच्यते।।
-विश्वनाथ, साहित्यद० १०,१०२ ४. उत्तरोत्तरमुत्कर्षः सार इत्यभिधीयते।
-अप्पय्यदी० कुवलया० १०८ तथा उसकी वृत्ति द्रष्टव्य, पृ० १२७-२८