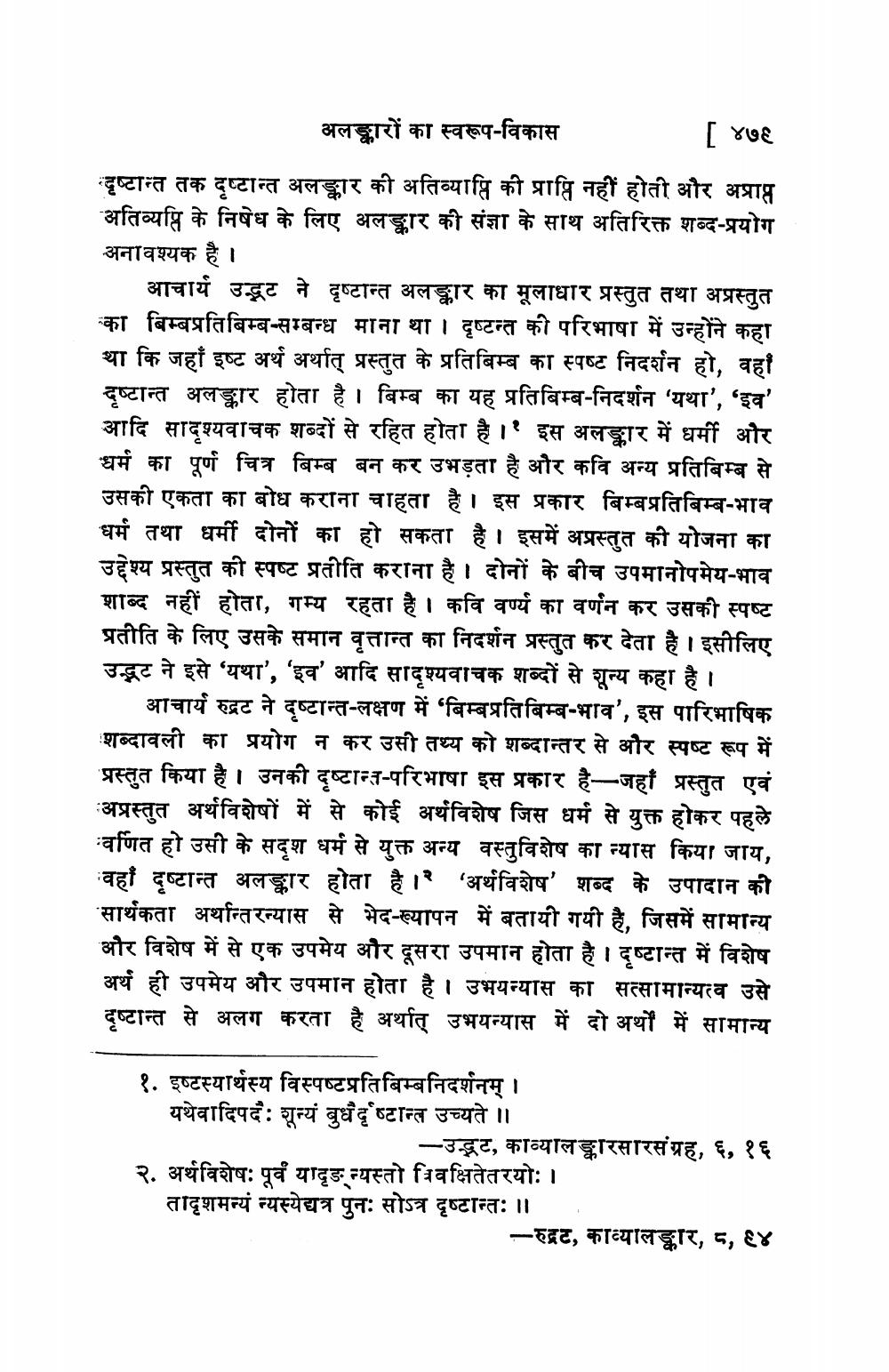________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ४७ दृष्टान्त तक दृष्टान्त अलङ्कार की अतिव्याप्ति की प्राप्ति नहीं होती और अप्राप्त अतिव्याप्ति के निषेध के लिए अलङ्कार की संज्ञा के साथ अतिरिक्त शब्द प्रयोग अनावश्यक है ।
आचार्य उद्भट ने दृष्टान्त अलङ्कार का मूलाधार प्रस्तुत तथा अप्रस्तुत ACT बिम्बप्रतिबिम्ब-सम्बन्ध माना था । दृष्टन्त की परिभाषा में उन्होंने कहा था कि जहाँ इष्ट अर्थ अर्थात् प्रस्तुत के प्रतिबिम्ब का स्पष्ट निदर्शन हो, वहाँ दृष्टान्त अलङ्कार होता है । बिम्ब का यह प्रतिबिम्ब - निदर्शन 'यथा', 'इव' आदि सादृश्यवाचक शब्दों से रहित होता है । इस अलङ्कार में धर्मी और धर्म का पूर्ण चित्र बिम्ब बन कर उभड़ता है और कवि अन्य प्रतिबिम्ब से उसकी एकता का बोध कराना चाहता है । इस प्रकार बिम्बप्रतिबिम्ब - भाव धर्म तथा धर्मी दोनों का हो सकता है। इसमें अप्रस्तुत की योजना का उद्देश्य प्रस्तुत की स्पष्ट प्रतीति कराना है । दोनों के बीच उपमानोपमेय - भाव शाब्द नहीं होता, गम्य रहता है । कवि वर्ण्य का वर्णन कर उसकी स्पष्ट प्रतीति के लिए उसके समान वृत्तान्त का निदर्शन प्रस्तुत कर देता है । इसीलिए उद्भट ने इसे 'यथा', 'इव' आदि सादृश्यवाचक शब्दों से शून्य कहा है ।
आचार्य रुद्रट ने दृष्टान्त - लक्षण में 'बिम्बप्रतिबिम्ब-भाव' इस पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग न कर उसी तथ्य को शब्दान्तर से और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत किया है । उनकी दृष्टान्त परिभाषा इस प्रकार है— जहाँ प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अर्थविशेषों में से कोई अर्थविशेष जिस धर्म से युक्त होकर पहले वर्णित हो उसी के सदृश धर्म से युक्त अन्य वस्तुविशेष का न्यास किया जाय, वहाँ दृष्टान्त अलङ्कार होता है ।" 'अर्थविशेष' शब्द के उपादान की सार्थकता अर्थान्तरन्यास से भेद - ख्यापन में बतायी गयी है, जिसमें सामान्य और विशेष में से एक उपमेय और दूसरा उपमान होता है । दृष्टान्त में विशेष अर्थ ही उपमेय और उपमान होता है । उभयन्यास का सत्सामान्यत्व उसे दृष्टान्त से अलग करता है अर्थात् उभयन्यास में दो अर्थों में सामान्य
१. इष्टस्यार्थस्य विस्पष्टप्रतिबिम्ब निदर्शनम् । वादिपदैः शून्यं बुधैर्दृष्टान्त उच्यते ॥
—उद्भट, काव्यालङ्कारसारसंग्रह, ६, १६
२. अर्थविशेषः पूर्वं यादृङ्न्यस्तो विवक्षितेतरयोः । तादृशमन्यं न्यस्येद्यत्र पुनः सोऽत्र दृष्टान्तः ।।
—– रुद्रट, काव्यालङ्कार, ८, ६४