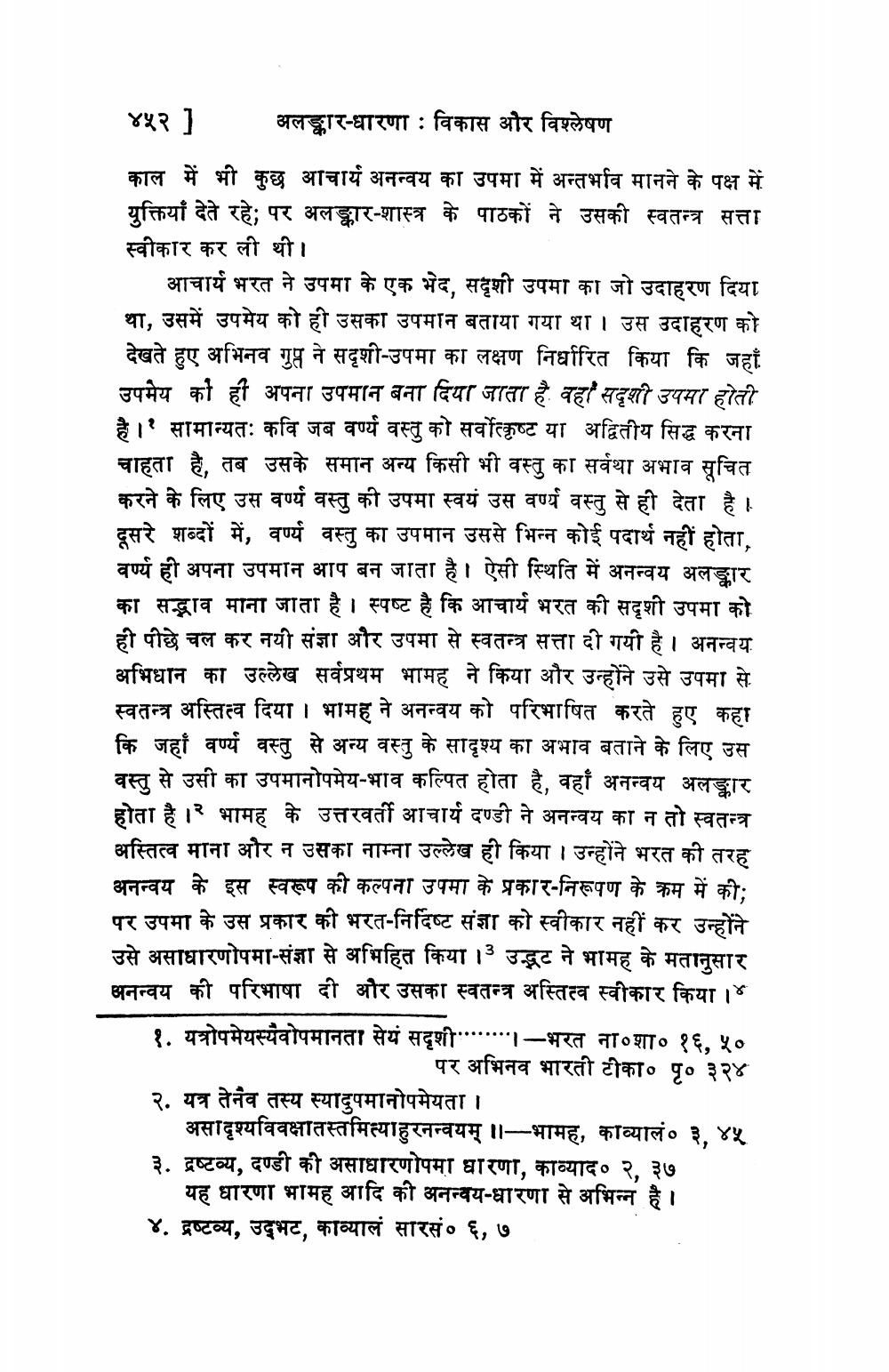________________
४५२ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
काल में भी कुछ आचार्य अनन्वय का उपमा में अन्तर्भाव मानने के पक्ष में युक्तियाँ देते रहे; पर अलङ्कार-शास्त्र के पाठकों ने उसकी स्वतन्त्र सत्ता स्वीकार कर ली थी।
आचार्य भरत ने उपमा के एक भेद, सदृशी उपमा का जो उदाहरण दिया था, उसमें उपमेय को ही उसका उपमान बताया गया था। उस उदाहरण को देखते हुए अभिनव गुप्त ने सदृशी-उपमा का लक्षण निर्धारित किया कि जहाँ उपमेय को ही अपना उपमान बना दिया जाता है वहाँ सदृशी उपमा होती है।' सामान्यतः कवि जब वर्ण्य वस्तु को सर्वोत्कृष्ट या अद्वितीय सिद्ध करना चाहता है, तब उसके समान अन्य किसी भी वस्तु का सर्वथा अभाव सूचित करने के लिए उस वर्ण्य वस्तु की उपमा स्वयं उस वर्ण्य वस्तु से ही देता है। दूसरे शब्दों में, वर्ण्य वस्तु का उपमान उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं होता, वर्ण्य ही अपना उपमान आप बन जाता है। ऐसी स्थिति में अनन्वय अलङ्कार का सद्भाव माना जाता है। स्पष्ट है कि आचार्य भरत की सदृशी उपमा को ही पीछे चल कर नयी संज्ञा और उपमा से स्वतन्त्र सत्ता दी गयी है। अनन्वय अभिधान का उल्लेख सर्वप्रथम भामह ने किया और उन्होंने उसे उपमा से स्वतन्त्र अस्तित्व दिया। भामह ने अनन्वय को परिभाषित करते हुए कहा कि जहाँ वर्ण्य वस्तु से अन्य वस्तु के सादृश्य का अभाव बताने के लिए उस वस्तु से उसी का उपमानोपमेय-भाव कल्पित होता है, वहाँ अनन्वय अलङ्कार होता है। भामह के उत्तरवर्ती आचार्य दण्डी ने अनन्वय का न तो स्वतन्त्र अस्तित्व माना और न उसका नाम्ना उल्लेख ही किया। उन्होंने भरत की तरह अनन्वय के इस स्वरूप की कल्पना उपमा के प्रकार-निरूपण के क्रम में की; पर उपमा के उस प्रकार की भरत-निर्दिष्ट संज्ञा को स्वीकार नहीं कर उन्होंने उसे असाधारणोपमा-संज्ञा से अभिहित किया। उद्भट ने भामह के मतानुसार अनन्वय की परिभाषा दी और उसका स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार किया। १. यत्रोपमेयस्यैवोपमानता सेयं सदृशी......"। -भरत ना०शा० १६, ५०
पर अभिनव भारती टीका० पृ० ३२४ २. यत्र तेनैव तस्य स्यादुपमानोपमेयता। ___ असादृश्यविवक्षातस्तमित्याहुरनन्वयम् ॥-भामह, काव्यालं० ३, ४५ ३. द्रष्टव्य, दण्डी की असाधारणोपमा धारणा, काव्याद० २, ३७
यह धारणा भामह आदि की अनन्वय-धारणा से अभिन्न है। ४. द्रष्टव्य, उद्भट, काव्यालं सारसं० ६, ७