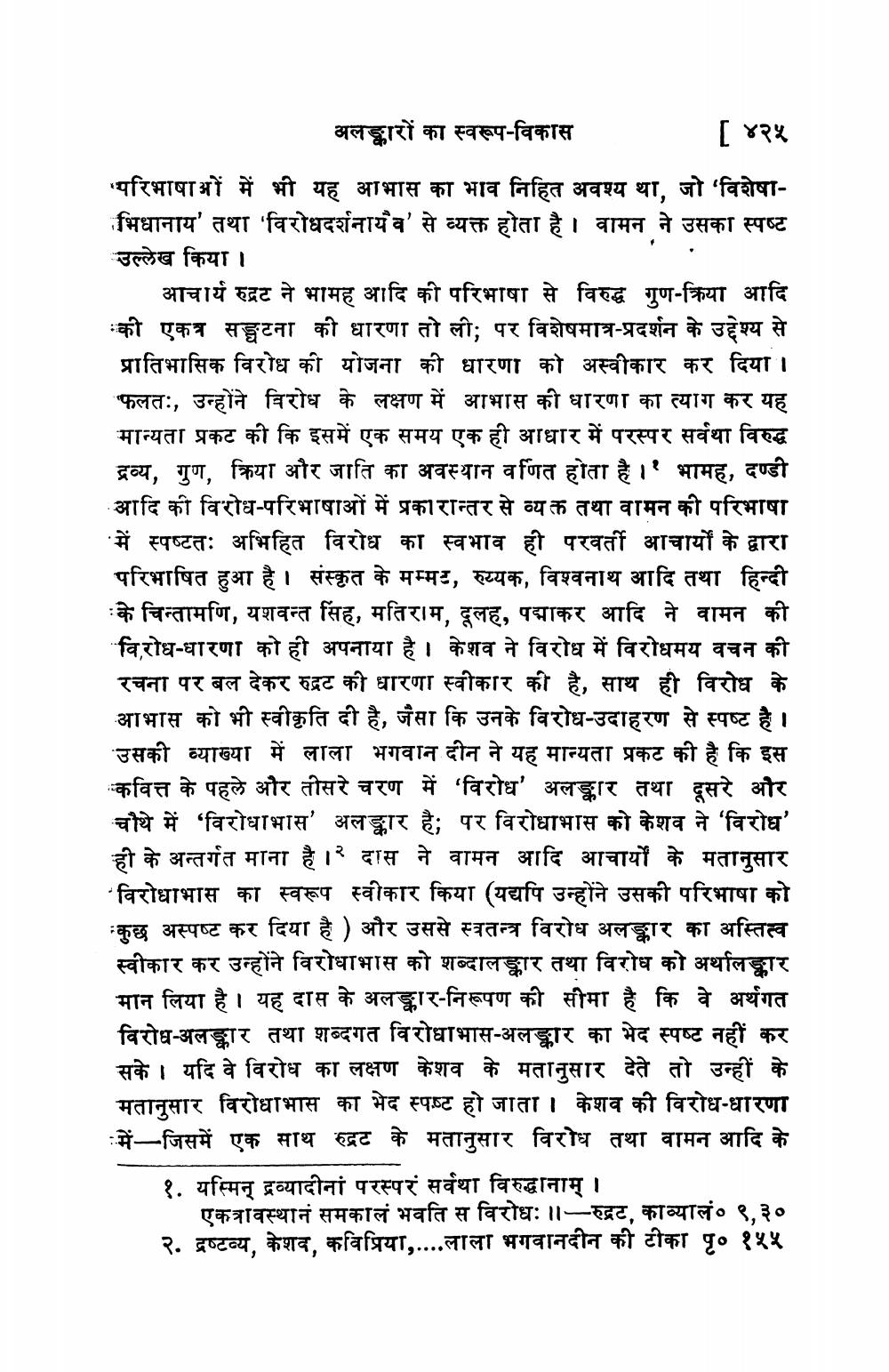________________
अलङ्कारों का स्वरूप - विकास
[ ४२५ 'परिभाषाओं में भी यह आभास का भाव निहित अवश्य था, जो 'विशेषाभिधानाय' तथा 'विरोधदर्शनाय व' से व्यक्त होता है । वामन ने उसका स्पष्ट उल्लेख किया ।
आचार्य रुद्रट ने भामह आदि की परिभाषा से विरुद्ध गुण-क्रिया आदि की एकत्र सङ्घटना की धारणा तो ली; पर विशेषमात्र प्रदर्शन के उद्देश्य से प्रातिभासिक विरोध की योजना की धारणा को अस्वीकार कर दिया । फलतः, उन्होंने विरोध के लक्षण में आभास की धारणा का त्याग कर यह मान्यता प्रकट की कि इसमें एक समय एक ही आधार में परस्पर सर्वथा विरुद्ध द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति का अवस्थान वर्णित होता है । १ भामह, दण्डी • आदि की विरोध- परिभाषाओं में प्रकारान्तर से व्यक्त तथा वामन की परिभाषा ' में स्पष्टतः अभिहित विरोध का स्वभाव ही परवर्ती आचार्यों के द्वारा परिभाषित हुआ है । संस्कृत के मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ आदि तथा हिन्दी के चिन्तामणि, यशवन्त सिंह, मतिराम, दूलह, पद्माकर आदि ने वामन की विरोध- धारणा को ही अपनाया है । केशव ने विरोध में विरोधमय वचन की रचना पर बल देकर रुद्रट की धारणा स्वीकार की है, साथ ही विरोध के आभास को भी स्वीकृति दी है, जैसा कि उनके विरोध - उदाहरण से स्पष्ट है । उसकी व्याख्या में लाला भगवान दीन ने यह मान्यता प्रकट की है कि इस कवित्त के पहले और तीसरे चरण में 'विरोध' अलङ्कार तथा दूसरे और चौथे में 'विरोधाभास' अलङ्कार है; पर विरोधाभास को केशव ने 'विरोध' ही के अन्तर्गत माना है । २ दास ने वामन आदि आचार्यों के मतानुसार 'विरोधाभास का स्वरूप स्वीकार किया (यद्यपि उन्होंने उसकी परिभाषा को कुछ अस्पष्ट कर दिया है ) और उससे स्वतन्त्र विरोध अलङ्कार का अस्तित्व स्वीकार कर उन्होंने विरोधाभास को शब्दालङ्कार तथा विरोध को अर्थालङ्कार मान लिया है । यह दास के अलङ्कार - निरूपण की सीमा है कि वे अर्थगत विरोध- अलङ्कार तथा शब्दगत विरोधाभास - अलङ्कार का भेद स्पष्ट नहीं कर सके । यदि वे विरोध का लक्षण केशव के मतानुसार देते तो उन्हीं के मतानुसार विरोधाभास का भेद स्पष्ट हो जाता । केशव की विरोध-धारणा : में — जिसमें एक साथ रुद्रट के मतानुसार विरोध तथा वामन आदि के
१. यस्मिन् द्रव्यादीनां परस्परं सर्वथा विरुद्धानाम् ।
एकत्रावस्थानं समकालं भवति स विरोधः ॥ - रुद्रट, काव्यालं० ९,३० २. द्रष्टव्य, केशव, कविप्रिया,....लाला भगवानदीन की टीका पृ० १५५