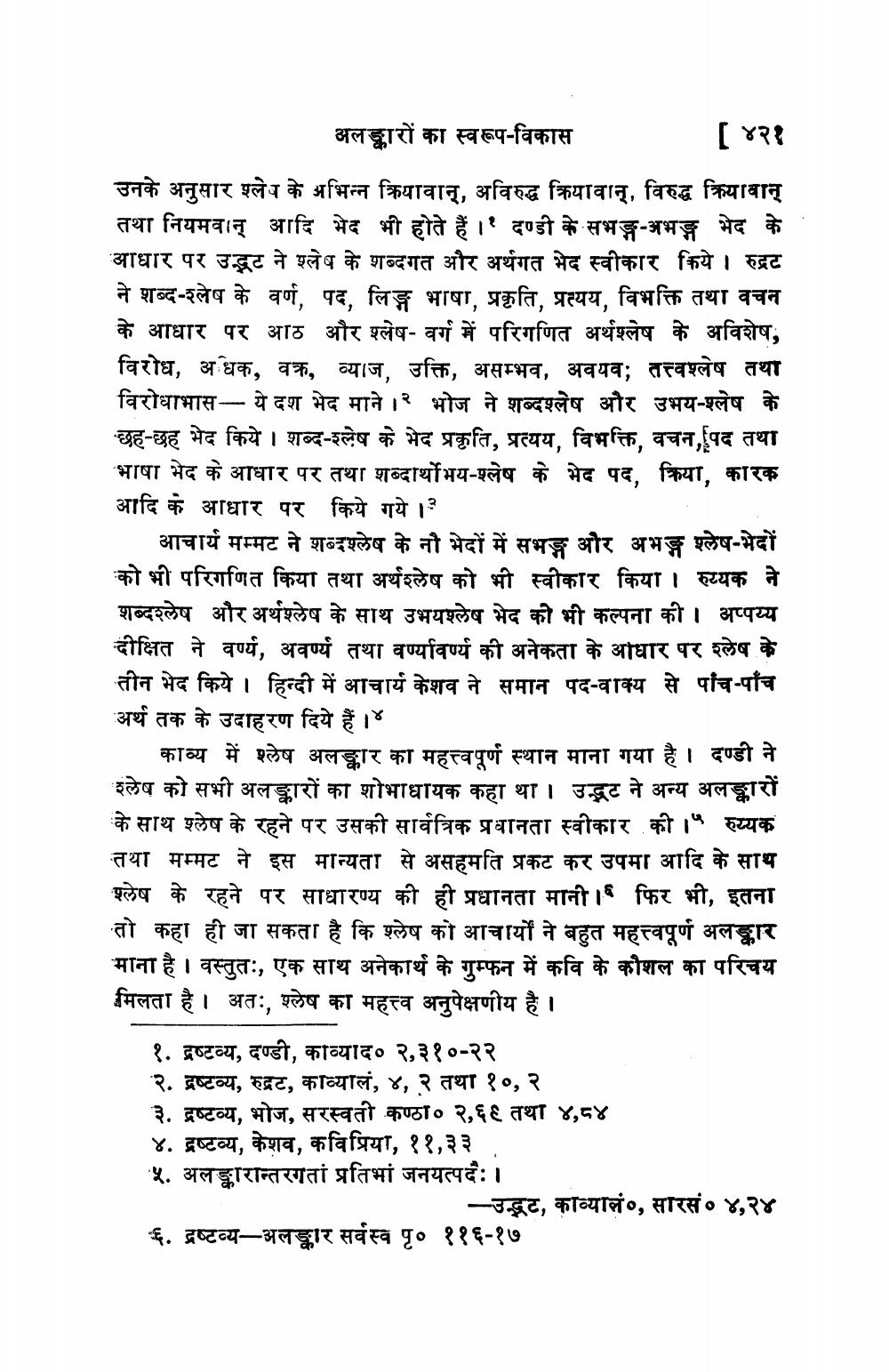________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[४२१ उनके अनुसार श्लेष के अभिन्न क्रियावान्, अविरुद्ध क्रियावान्, विरुद्ध क्रियावान् तथा नियमवान् आदि भेद भी होते हैं।' दण्डी के सभङ्ग-अभङ्ग भेद के आधार पर उद्भट ने श्लेष के शब्दगत और अर्थगत भेद स्वीकार किये। रुद्रट ने शब्द-श्लेष के वर्ण, पद, लिङ्ग भाषा, प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति तथा वचन के आधार पर आठ और श्लेष- वर्ग में परिगणित अर्थश्लेष के अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असम्भव, अवयव; तत्त्वश्लेष तथा विरोधाभास- ये दश भेद माने ।२ भोज ने शब्दश्लेष और उभय-श्लेष के 'छह-छह भेद किये । शब्द-श्लेष के भेद प्रकृति, प्रत्यय, विभक्ति, वचन, पद तथा भाषा भेद के आधार पर तथा शब्दार्थोभय-श्लेष के भेद पद, क्रिया, कारक आदि के आधार पर किये गये। ___ आचार्य मम्मट ने शब्दश्लेष के नौ भेदों में सभङ्ग और अभङ्ग श्लेष-भेदों को भी परिगणित किया तथा अर्थश्लेष को भी स्वीकार किया। रुय्यक ने शब्दश्लेष और अर्थश्लेष के साथ उभयश्लेष भेद को भी कल्पना की। अप्पय्य दीक्षित ने वर्ण्य, अवर्ण्य तथा वावर्ण्य की अनेकता के आधार पर श्लेष के तीन भेद किये। हिन्दी में आचार्य केशव ने समान पद-वाक्य से पांच-पाँच अर्थ तक के उदाहरण दिये हैं।
काव्य में श्लेष अलङ्कार का महत्त्वपूर्ण स्थान माना गया है। दण्डी ने श्लेष को सभी अलङ्कारों का शोभाधायक कहा था। उद्भट ने अन्य अलङ्कारों के साथ श्लेष के रहने पर उसकी सार्वत्रिक प्रधानता स्वीकार की।" रुय्यक तथा मम्मट ने इस मान्यता से असहमति प्रकट कर उपमा आदि के साथ श्लेष के रहने पर साधारण्य की ही प्रधानता मानी। फिर भी, इतना तो कहा ही जा सकता है कि श्लेष को आचार्यों ने बहुत महत्त्वपूर्ण अलङ्कार माना है । वस्तुतः, एक साथ अनेकार्थ के गुम्फन में कवि के कौशल का परिचय मिलता है। अतः, श्लेष का महत्त्व अनुपेक्षणीय है।
१. द्रष्टव्य, दण्डी, काव्याद० २,३१०-२२ । २. द्रष्टव्य, रुद्रट, काव्यालं, ४,२ तथा १०, २ ३. द्रष्टव्य, भोज, सरस्वती कण्ठा० २,६६ तथा ४,८४ ४. द्रष्टव्य, केशव, कविप्रिया, ११,३३ . ५. अलङ्कारान्तरगतां प्रतिभां जनयत्पदैः ।
-उद्भट, काव्यालं०, सारसं० ४,२४ ६. द्रष्टव्य-अलङ्कार सर्वस्व पृ० ११६-१७