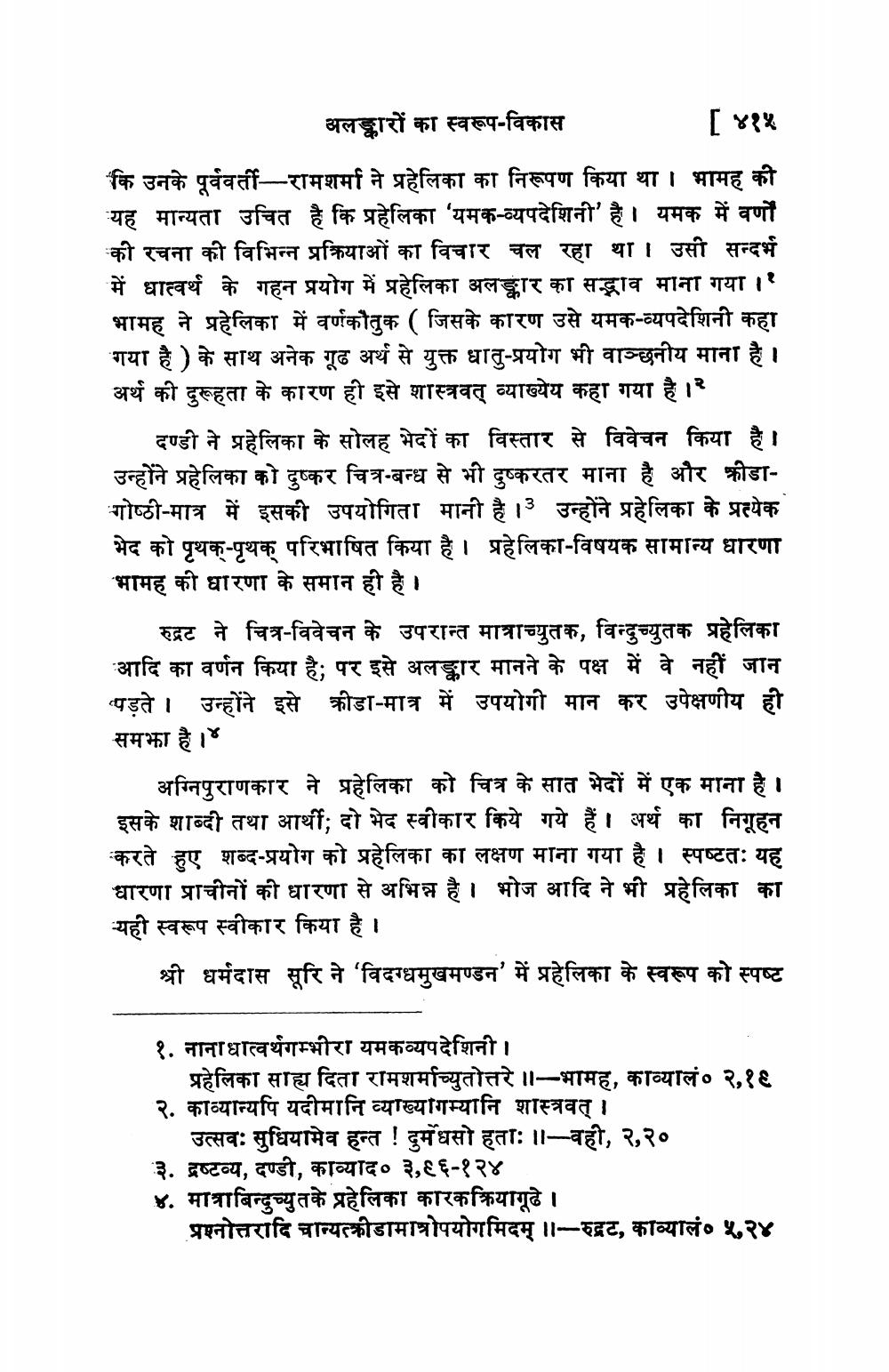________________
अलङ्कारों का स्वरूप-विकास
[ ४१५
कि उनके पूर्ववर्ती-रामशर्मा ने प्रहेलिका का निरूपण किया था। भामह की यह मान्यता उचित है कि प्रहेलिका 'यमक-व्यपदेशिनी' है। यमक में वर्णों की रचना की विभिन्न प्रक्रियाओं का विचार चल रहा था। उसी सन्दर्भ में धात्वर्थ के गहन प्रयोग में प्रहेलिका अलङ्कार का सद्भाव माना गया।' भामह ने प्रहेलिका में वर्णकौतुक ( जिसके कारण उसे यमक-व्यपदेशिनी कहा गया है) के साथ अनेक गूढ अर्थ से युक्त धातु-प्रयोग भी वाञ्छनीय माना है। अर्थ की दुरूहता के कारण ही इसे शास्त्रवत् व्याख्येय कहा गया है। ___ दण्डी ने प्रहेलिका के सोलह भेदों का विस्तार से विवेचन किया है। उन्होंने प्रहेलिका को दुष्कर चित्र-बन्ध से भी दुष्करतर माना है और क्रीडागोष्ठी-मात्र में इसकी उपयोगिता मानी है। उन्होंने प्रहेलिका के प्रत्येक भेद को पृथक्-पृथक् परिभाषित किया है। प्रहेलिका-विषयक सामान्य धारणा भामह की धारणा के समान ही है।
रुद्रट ने चित्र-विवेचन के उपरान्त मात्राच्युतक, विन्दुच्युतक प्रहेलिका आदि का वर्णन किया है; पर इसे अलङ्कार मानने के पक्ष में वे नहीं जान पड़ते। उन्होंने इसे क्रीडा-मात्र में उपयोगी मान कर उपेक्षणीय ही समझा है।
अग्निपुराणकार ने प्रहेलिका को चित्र के सात भेदों में एक माना है। इसके शाब्दी तथा आर्थी; दो भेद स्वीकार किये गये हैं। अर्थ का निगहन करते हुए शब्द-प्रयोग को प्रहेलिका का लक्षण माना गया है। स्पष्टतः यह धारणा प्राचीनों की धारणा से अभिन्न है। भोज आदि ने भी प्रहेलिका का यही स्वरूप स्वीकार किया है।
श्री धर्मदास सूरि ने 'विदग्धमुखमण्डन' में प्रहेलिका के स्वरूप को स्पष्ट
१. नानाधात्वर्थगम्भीरा यमकव्यपदेशिनी।
प्रहेलिका साह्य दिता रामशर्माच्युतोत्तरे ॥-भामह, काव्यालं० २,१६ २. काव्यान्यपि यदीमानि व्याख्यागम्यानि शास्त्रवत् ।
उत्सवः सुधियामेव हन्त ! दुर्मेधसो हताः ॥-वही, २,२० ३. द्रष्टव्य, दण्डी, काव्याद० ३,६६-१२४ ४. मात्राबिन्दुच्युतके प्रहेलिका कारकक्रियागूढे ।
प्रश्नोत्तरादि चान्यत्क्रीडामात्रोपयोगमिदम् ।।-रुद्रट, काव्यालं०५.२४