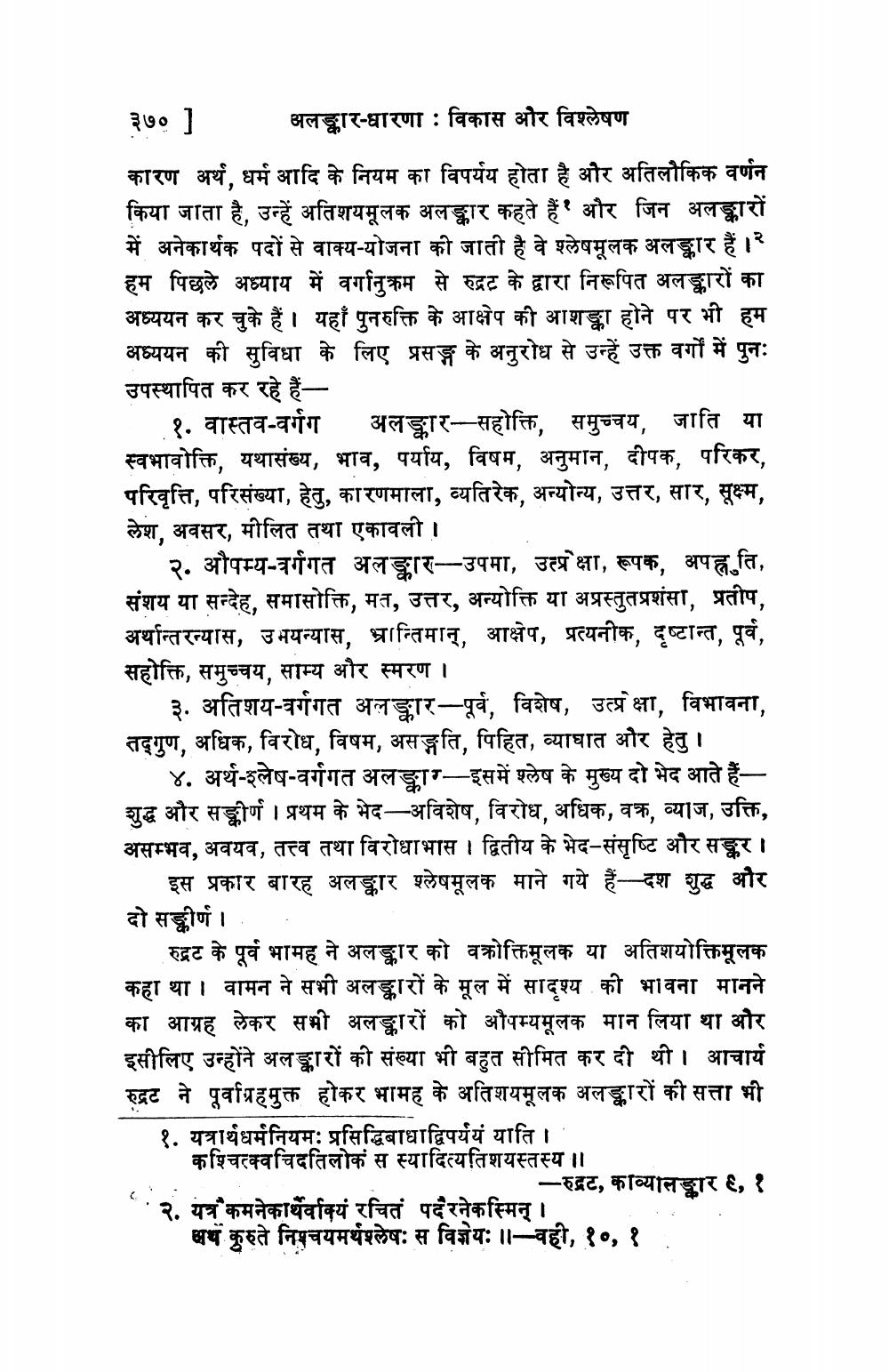________________
३७० ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण कारण अर्थ, धर्म आदि के नियम का विपर्यय होता है और अतिलौकिक वर्णन किया जाता है, उन्हें अतिशयमूलक अलङ्कार कहते हैं। और जिन अलङ्कारों में अनेकार्थक पदों से वाक्य-योजना की जाती है वे श्लेषमूलक अलङ्कार हैं। हम पिछले अध्याय में वर्गानुक्रम से रुद्रट के द्वारा निरूपित अलङ्कारों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ पुनरुक्ति के आक्षेप की आशङ्का होने पर भी हम अध्ययन की सुविधा के लिए प्रसङ्ग के अनुरोध से उन्हें उक्त वर्गों में पुनः उपस्थापित कर रहे हैं
१. वास्तव-वर्गग अलङ्कार-सहोक्ति, समुच्चय, जाति या स्वभावोक्ति, यथासंख्य, भाव, पर्याय, विषम, अनुमान, दीपक, परिकर, परिवृत्ति, परिसंख्या, हेतु, कारणमाला, व्यतिरेक, अन्योन्य, उत्तर, सार, सूक्ष्म, लेश, अवसर, मीलित तथा एकावली।
२. औपम्य-वर्गगत अलङ्कार-उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अपह्नति, संशय या सन्देह, समासोक्ति, मत, उत्तर, अन्योक्ति या अप्रस्तुतप्रशंसा, प्रतीप, अर्थान्तरन्यास, उभयन्यास, भ्रान्तिमान्, आक्षेप, प्रत्यनीक, दृष्टान्त, पूर्व, सहोक्ति, समुच्चय, साम्य और स्मरण।
३. अतिशय-वर्गगत अलङ्कार-पूर्व, विशेष, उत्प्रेक्षा, विभावना, तद्गुण, अधिक, विरोध, विषम, असङ्गति, पिहित, व्याघात और हेतु।
४. अर्थ-श्लेष-वर्गगत अलङ्कार-इसमें श्लेष के मुख्य दो भेद आते हैंशुद्ध और सङ्कीर्ण । प्रथम के भेद-अविशेष, विरोध, अधिक, वक्र, व्याज, उक्ति, असम्भव, अवयव, तत्त्व तथा विरोधाभास । द्वितीय के भेद-संसृष्टि और सङ्कर । ___इस प्रकार बारह अलङ्कार श्लेषमूलक माने गये हैं—दश शुद्ध और दो सङ्कीर्ण।
रुद्रट के पूर्व भामह ने अलङ्कार को वक्रोक्तिमूलक या अतिशयोक्तिमूलक कहा था। वामन ने सभी अलङ्कारों के मूल में सादृश्य की भावना मानने का आग्रह लेकर सभी अलङ्कारों को औपम्यमूलक मान लिया था और इसीलिए उन्होंने अलङ्कारों की संख्या भी बहुत सीमित कर दी थी। आचार्य रुद्रट ने पूर्वाग्रहमुक्त होकर भामह के अतिशयमूलक अलङ्कारों की सत्ता भी १. यत्रार्थधर्मनियमः प्रसिद्धिबाधाद्विपर्ययं याति । कश्चित्क्वचिदतिलोकं स स्यादित्यतिशयस्तस्य ॥
-रुद्रट, काव्यालङ्कार ६, १ " . २. यत्र कमनेकार्थक्यं रचितं पदैरनेकस्मिन् ।
अर्थ कुरुते निश्चयमर्थश्लेषः स विजेयः ॥ वही, १०, १ .