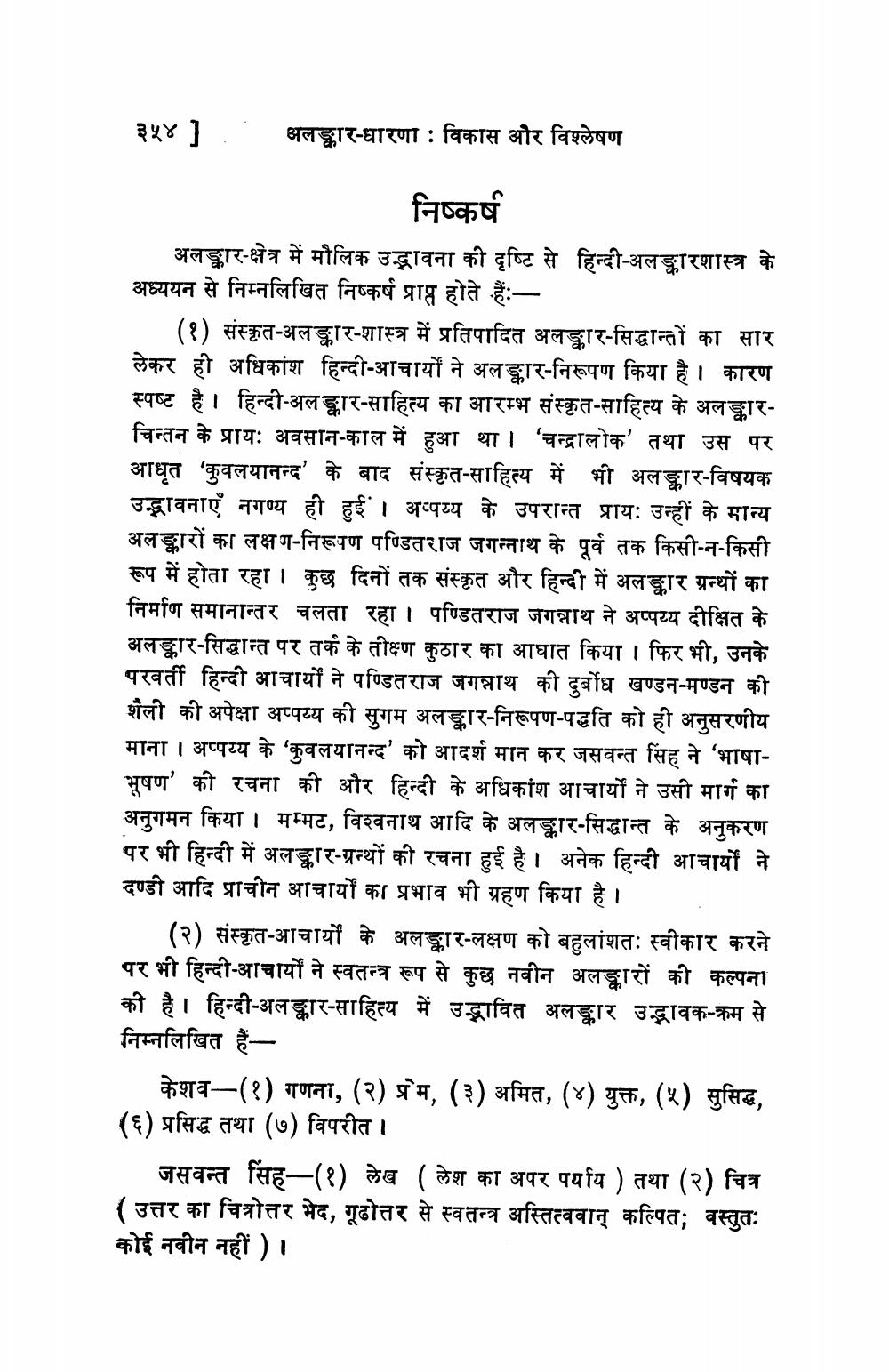________________
३५४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
निष्कर्ष अलङ्कार-क्षेत्र में मौलिक उद्भावना की दृष्टि से हिन्दी-अलङ्कारशास्त्र के अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त होते हैं:
(१) संस्कृत-अलङ्कार-शास्त्र में प्रतिपादित अलङ्कार-सिद्धान्तों का सार लेकर ही अधिकांश हिन्दी-आचार्यों ने अलङ्कार-निरूपण किया है। कारण स्पष्ट है। हिन्दी-अलङ्कार-साहित्य का आरम्भ संस्कृत-साहित्य के अलङ्कारचिन्तन के प्रायः अवसान-काल में हुआ था। 'चन्द्रालोक' तथा उस पर आधुत 'कुवलयानन्द' के बाद संस्कृत-साहित्य में भी अलङ्कार-विषयक उद्भावनाएँ नगण्य ही हुई। अप्पय्य के उपरान्त प्रायः उन्हीं के मान्य अलङ्कारों का लक्षण-निरूपण पण्डितराज जगन्नाथ के पूर्व तक किसी-न-किसी रूप में होता रहा। कुछ दिनों तक संस्कृत और हिन्दी में अलङ्कार ग्रन्थों का निर्माण समानान्तर चलता रहा। पण्डितराज जगन्नाथ ने अप्पय्य दीक्षित के अलङ्कार-सिद्धान्त पर तर्क के तीक्ष्ण कुठार का आघात किया । फिर भी, उनके परवर्ती हिन्दी आचार्यों ने पण्डितराज जगन्नाथ की दुर्बोध खण्डन-मण्डन की शैली की अपेक्षा अप्पय्य की सुगम अलङ्कार-निरूपण-पद्धति को ही अनुसरणीय माना । अप्पय्य के 'कुवलयानन्द' को आदर्श मान कर जसवन्त सिंह ने 'भाषाभूषण' की रचना की और हिन्दी के अधिकांश आचार्यों ने उसी मार्ग का अनुगमन किया। मम्मट, विश्वनाथ आदि के अलङ्कार-सिद्धान्त के अनुकरण पर भी हिन्दी में अलङ्कार-ग्रन्थों की रचना हुई है। अनेक हिन्दी आचार्यों ने दण्डी आदि प्राचीन आचार्यों का प्रभाव भी ग्रहण किया है।
(२) संस्कृत-आचार्यों के अलङ्कार-लक्षण को बहुलांशतः स्वीकार करने पर भी हिन्दी-आचार्यों ने स्वतन्त्र रूप से कुछ नवीन अलङ्कारों की कल्पना की है। हिन्दी-अलङ्कार-साहित्य में उद्भावित अलङ्कार उद्भावक-क्रम से निम्नलिखित हैं
केशव-(१) गणना, (२) प्रेम, (३) अमित, (४) युक्त, (५) सुसिद्ध, (६) प्रसिद्ध तथा (७) विपरीत ।
जसवन्त सिंह-(१) लेख ( लेश का अपर पर्याय ) तथा (२) चित्र ( उत्तर का चित्रोत्तर भेद, गूढोत्तर से स्वतन्त्र अस्तित्ववान् कल्पित; वस्तुतः कोई नवीन नहीं)।