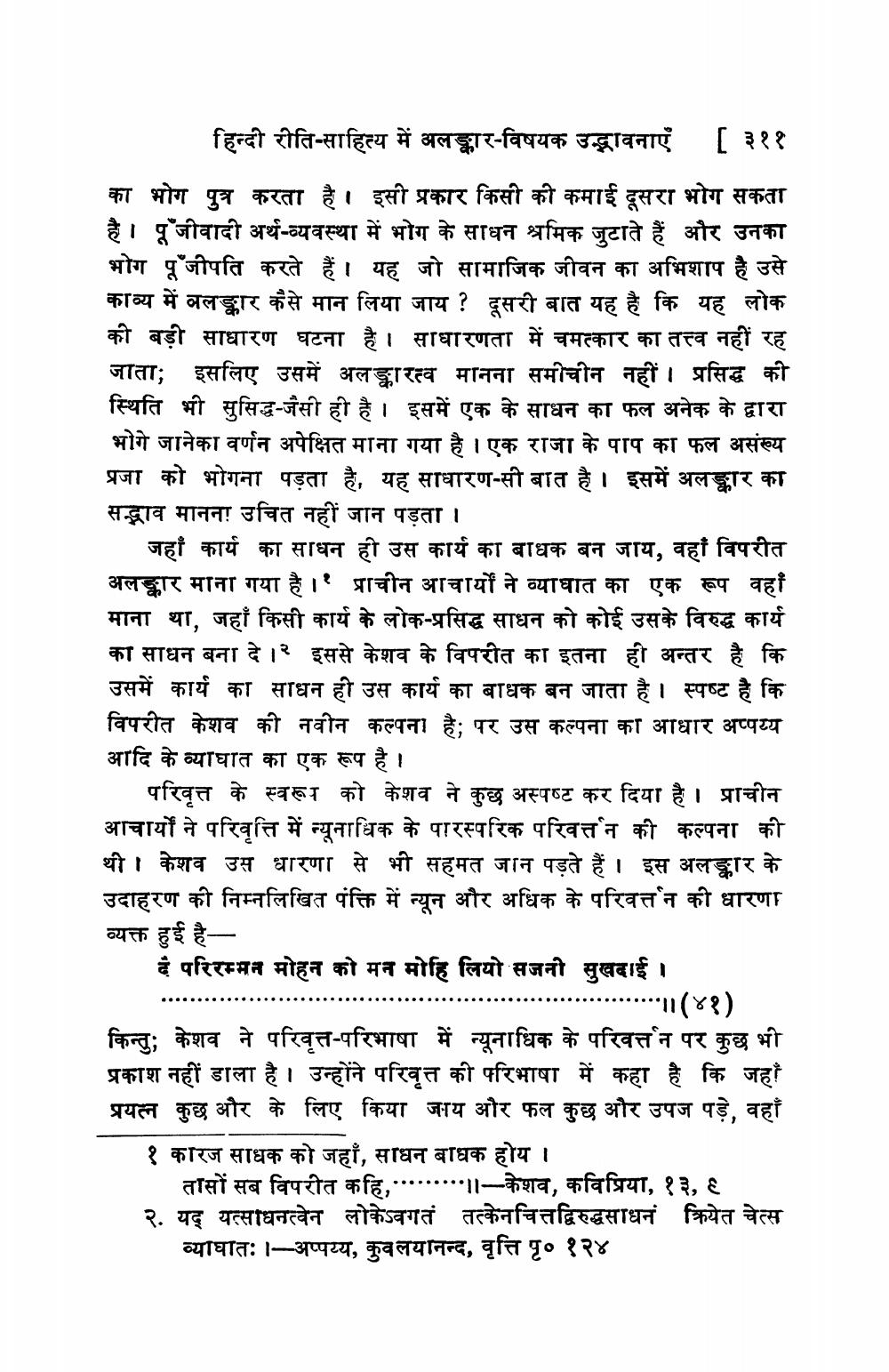________________
हिन्दी रीति-साहित्य में अलङ्कार-विषयक उद्भावनाएँ [ ३११ का भोग पुत्र करता है। इसी प्रकार किसी की कमाई दूसरा भोग सकता है। पूजीवादी अर्थ-व्यवस्था में भोग के साधन श्रमिक जुटाते हैं और उनका भोग पूजीपति करते हैं। यह जो सामाजिक जीवन का अभिशाप है उसे काव्य में बलङ्कार कैसे मान लिया जाय ? दूसरी बात यह है कि यह लोक की बड़ी साधारण घटना है। साधारणता में चमत्कार का तत्त्व नहीं रह जाता; इसलिए उसमें अलङ्कारत्व मानना समीचीन नहीं। प्रसिद्ध की स्थिति भी सुसिद्ध-जैसी ही है। इसमें एक के साधन का फल अनेक के द्वारा भोगे जानेका वर्णन अपेक्षित माना गया है । एक राजा के पाप का फल असंख्य प्रजा को भोगना पड़ता है, यह साधारण-सी बात है। इसमें अलङ्कार का सद्भाव मानना उचित नहीं जान पड़ता।
जहाँ कार्य का साधन ही उस कार्य का बाधक बन जाय, वहाँ विपरीत अलङ्कार माना गया है। प्राचीन आचार्यों ने व्याघात का एक रूप वहाँ माना था, जहाँ किसी कार्य के लोक-प्रसिद्ध साधन को कोई उसके विरुद्ध कार्य का साधन बना दे ।२ इससे केशव के विपरीत का इतना ही अन्तर है कि उसमें कार्य का साधन ही उस कार्य का बाधक बन जाता है। स्पष्ट है कि विपरीत केशव की नवीन कल्पना है; पर उस कल्पना का आधार अप्पय्य आदि के व्याघात का एक रूप है।
परिवृत्त के स्वरूप को केशव ने कुछ अस्पष्ट कर दिया है। प्राचीन आचार्यों ने परिवृत्ति में न्यूनाधिक के पारस्परिक परिवर्तन की कल्पना की थी। केशव उस धारणा से भी सहमत जान पड़ते हैं। इस अलङ्कार के उदाहरण की निम्नलिखित पंक्ति में न्यून और अधिक के परिवर्तन की धारणा व्यक्त हुई हैदै परिरम्मन मोहन को मन मोहि लियो सजनी सुखदाई।
...............॥(४१) किन्तु; केशव ने परिवृत्त-परिभाषा में न्यूनाधिक के परिवर्तन पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला है। उन्होंने परिवृत्त की परिभाषा में कहा है कि जहाँ प्रयत्न कुछ और के लिए किया जाय और फल कुछ और उपज पड़े, वहाँ १ कारज साधक को जहाँ, साधन बाधक होय ।
तासों सब विपरीत कहि,.........॥-केशव, कविप्रिया, १३, ६ २. यद् यत्साधनत्वेन लोकेऽवगतं तत्केनचित्तद्विरुद्धसाधनं क्रियेत चेत्स
व्याघातः।-अप्पय्य, कुवलयानन्द, वृत्ति पृ० १२४