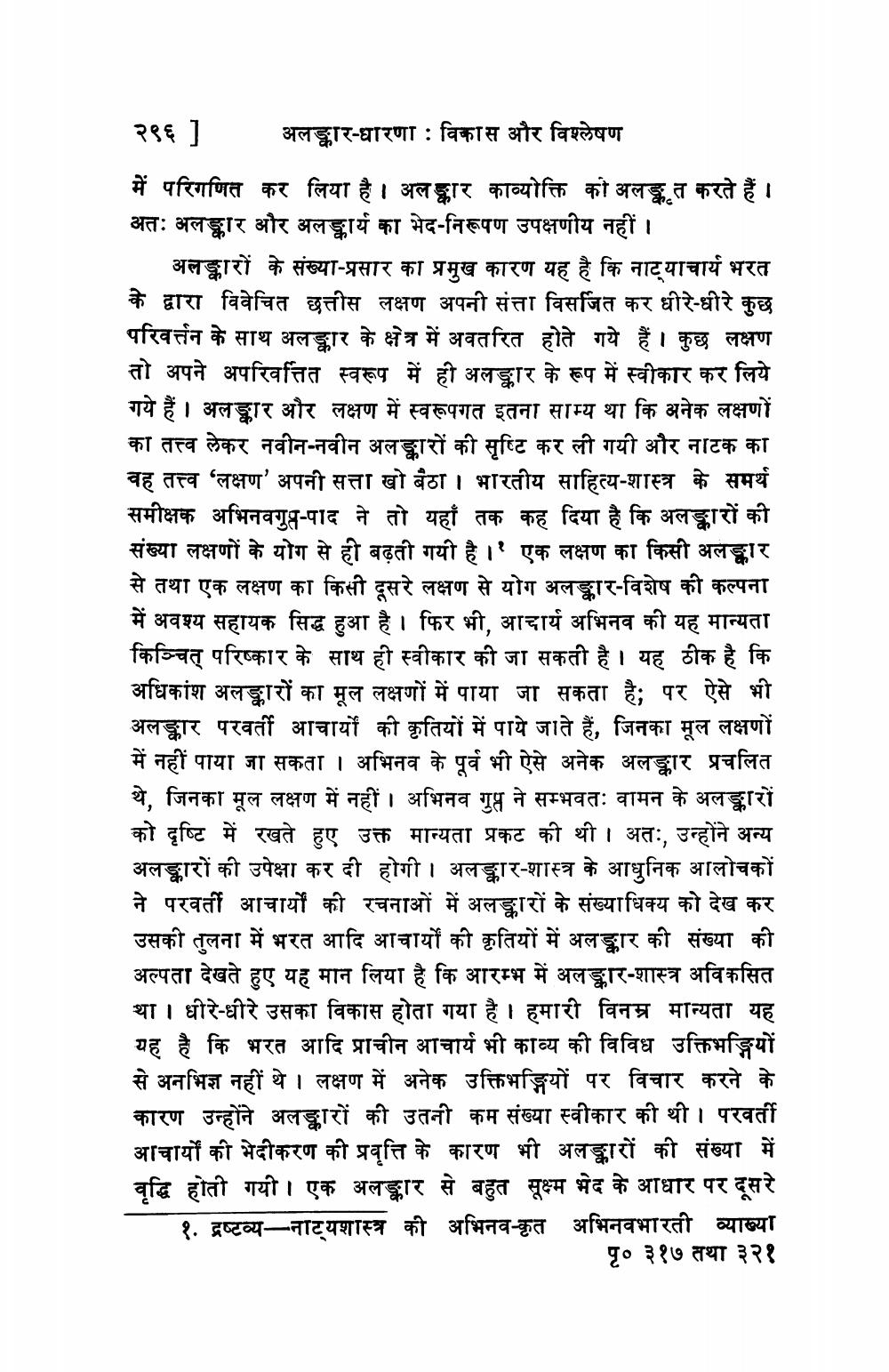________________
२९६ ] अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण में परिगणित कर लिया है। अलङ्कार काव्योक्ति को अलङ्कत करते हैं । अतः अलङ्कार और अलङ्कार्य का भेद-निरूपण उपक्षणीय नहीं। ___ अलङ्कारों के संख्या-प्रसार का प्रमुख कारण यह है कि नाट्याचार्य भरत के द्वारा विवेचित छत्तीस लक्षण अपनी संत्ता विसर्जित कर धीरे-धीरे कुछ परिवर्तन के साथ अलङ्कार के क्षेत्र में अवतरित होते गये हैं। कुछ लक्षण तो अपने अपरिवर्तित स्वरूप में ही अलङ्कार के रूप में स्वीकार कर लिये गये हैं। अलङ्कार और लक्षण में स्वरूपगत इतना साम्य था कि अनेक लक्षणों का तत्त्व लेकर नवीन-नवीन अलङ्कारों की सृष्टि कर ली गयी और नाटक का वह तत्त्व 'लक्षण' अपनी सत्ता खो बैठा। भारतीय साहित्य-शास्त्र के समर्थ समीक्षक अभिनवगुप्त-पाद ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अलङ्कारों की संख्या लक्षणों के योग से ही बढ़ती गयी है।' एक लक्षण का किसी अलङ्कार से तथा एक लक्षण का किसी दूसरे लक्षण से योग अलङ्कार-विशेष की कल्पना में अवश्य सहायक सिद्ध हुआ है। फिर भी, आचार्य अभिनव की यह मान्यता किञ्चित् परिष्कार के साथ ही स्वीकार की जा सकती है। यह ठीक है कि अधिकांश अलङ्कारों का मूल लक्षणों में पाया जा सकता है; पर ऐसे भी अलङ्कार परवर्ती आचार्यों की कृतियों में पाये जाते हैं, जिनका मूल लक्षणों में नहीं पाया जा सकता । अभिनव के पूर्व भी ऐसे अनेक अलङ्कार प्रचलित थे, जिनका मूल लक्षण में नहीं। अभिनव गुप्त ने सम्भवतः वामन के अलङ्कारों को दृष्टि में रखते हुए उक्त मान्यता प्रकट की थी। अतः, उन्होंने अन्य अलङ्कारों की उपेक्षा कर दी होगी। अलङ्कार-शास्त्र के आधुनिक आलोचकों ने परवर्ती आचार्यों की रचनाओं में अलङ्कारों के संख्याधिक्य को देख कर उसकी तुलना में भरत आदि आचार्यों की कृतियों में अलङ्कार की संख्या की अल्पता देखते हुए यह मान लिया है कि आरम्भ में अलङ्कार-शास्त्र अविकसित था। धीरे-धीरे उसका विकास होता गया है। हमारी विनम्र मान्यता यह यह है कि भरत आदि प्राचीन आचार्य भी काव्य की विविध उक्तिभङ्गियों से अनभिज्ञ नहीं थे। लक्षण में अनेक उक्तिभङ्गियों पर विचार करने के कारण उन्होंने अलङ्कारों की उतनी कम संख्या स्वीकार की थी। परवर्ती आचार्यों की भेदीकरण की प्रवृत्ति के कारण भी अलङ्कारों की संख्या में वृद्धि होती गयी। एक अलङ्कार से बहुत सूक्ष्म भेद के आधार पर दूसरे १. द्रष्टव्य-नाट्यशास्त्र की अभिनव-कृत अभिनवभारती व्याख्या
पृ० ३१७ तथा ३२१