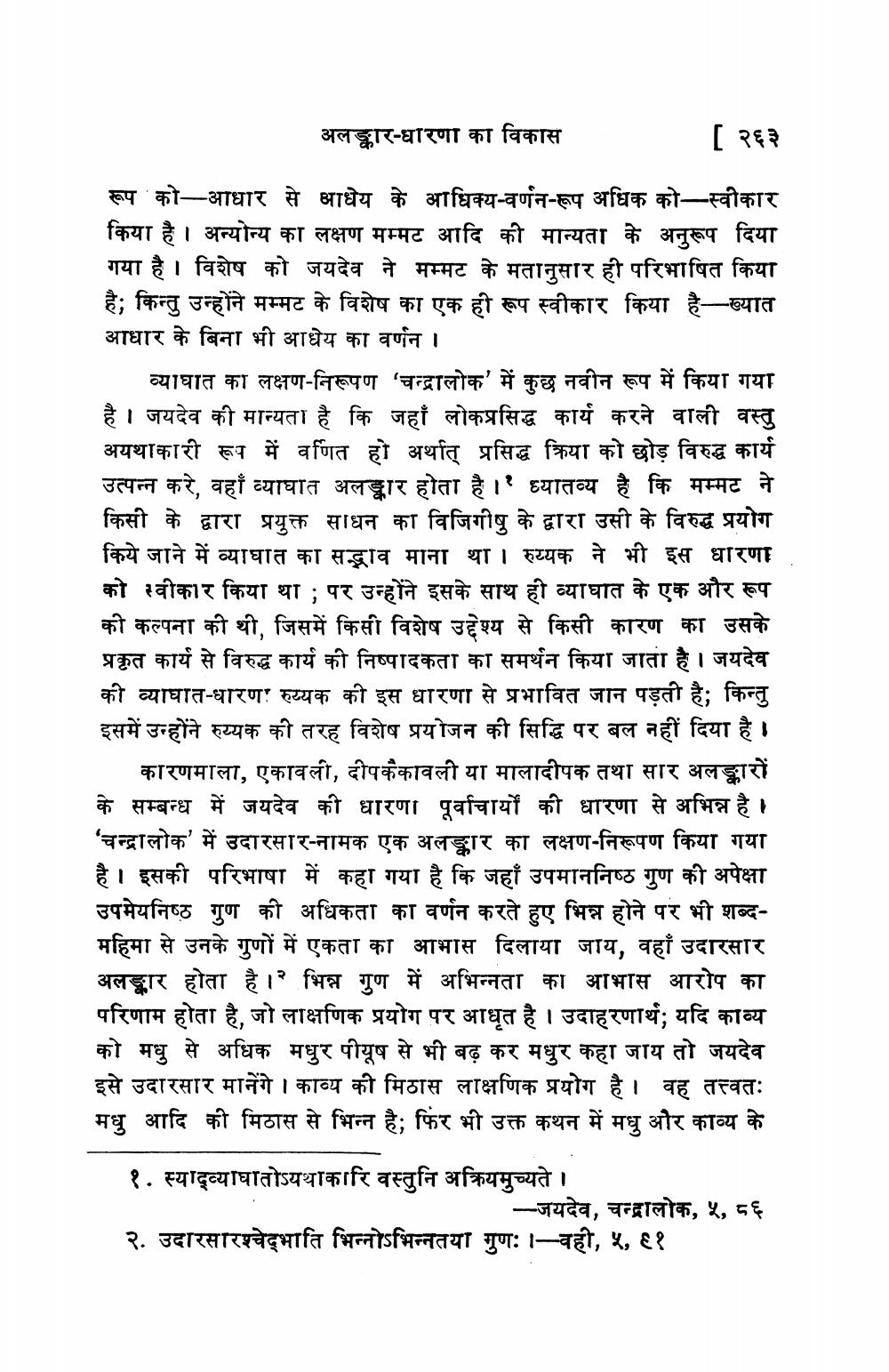________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[२६३
रूप को-आधार से आधेय के आधिक्य-वर्णन-रूप अधिक को-स्वीकार किया है। अन्योन्य का लक्षण मम्मट आदि की मान्यता के अनुरूप दिया गया है। विशेष को जयदेव ने मम्मट के मतानुसार ही परिभाषित किया है; किन्तु उन्होंने मम्मट के विशेष का एक ही रूप स्वीकार किया है—ख्यात आधार के बिना भी आधेय का वर्णन ।
व्याघात का लक्षण-निरूपण 'चन्द्रालोक' में कुछ नवीन रूप में किया गया है । जयदेव की मान्यता है कि जहाँ लोकप्रसिद्ध कार्य करने वाली वस्तु अयथाकारी रूप में वर्णित हो अर्थात् प्रसिद्ध क्रिया को छोड़ विरुद्ध कार्य उत्पन्न करे, वहाँ व्याघात अलङ्कार होता है। ध्यातव्य है कि मम्मट ने किसी के द्वारा प्रयुक्त साधन का विजिगीषु के द्वारा उसी के विरुद्ध प्रयोग किये जाने में व्याघात का सद्भाव माना था। रुय्यक ने भी इस धारणा को स्वीकार किया था ; पर उन्होंने इसके साथ ही व्याघात के एक और रूप की कल्पना की थी, जिसमें किसी विशेष उद्देश्य से किसी कारण का उसके प्रकृत कार्य से विरुद्ध कार्य की निष्पादकता का समर्थन किया जाता है । जयदेव की व्याघात-धारणा रुय्यक की इस धारणा से प्रभावित जान पड़ती है; किन्तु इसमें उन्होंने रुय्यक की तरह विशेष प्रयोजन की सिद्धि पर बल नहीं दिया है।
कारणमाला, एकावली, दीपकैकावली या मालादीपक तथा सार अलङ्कारों के सम्बन्ध में जयदेव की धारणा पूर्वाचार्यों की धारणा से अभिन्न है । 'चन्द्रालोक' में उदारसार-नामक एक अलङ्कार का लक्षण-निरूपण किया गया है। इसकी परिभाषा में कहा गया है कि जहाँ उपमाननिष्ठ गुण की अपेक्षा उपमेयनिष्ठ गुण की अधिकता का वर्णन करते हुए भिन्न होने पर भी शब्दमहिमा से उनके गुणों में एकता का आभास दिलाया जाय, वहाँ उदारसार अलङ्कार होता है।२ भिन्न गुण में अभिन्नता का आभास आरोप का परिणाम होता है, जो लाक्षणिक प्रयोग पर आधृत है । उदाहरणार्थ; यदि काव्य को मधु से अधिक मधुर पीयूष से भी बढ़ कर मधुर कहा जाय तो जयदेव इसे उदारसार मानेंगे । काव्य की मिठास लाक्षणिक प्रयोग है। वह तत्त्वतः मधु आदि की मिठास से भिन्न है; फिर भी उक्त कथन में मधु और काव्य के १. स्याद्व्याघातोऽयथाकारि वस्तुनि अक्रियमुच्यते।
-जयदेव, चन्द्रालोक, ५, ८६ २. उदारसारश्चेद्भाति भिन्नोऽभिन्नतया गुणः । वही, ५, ६१