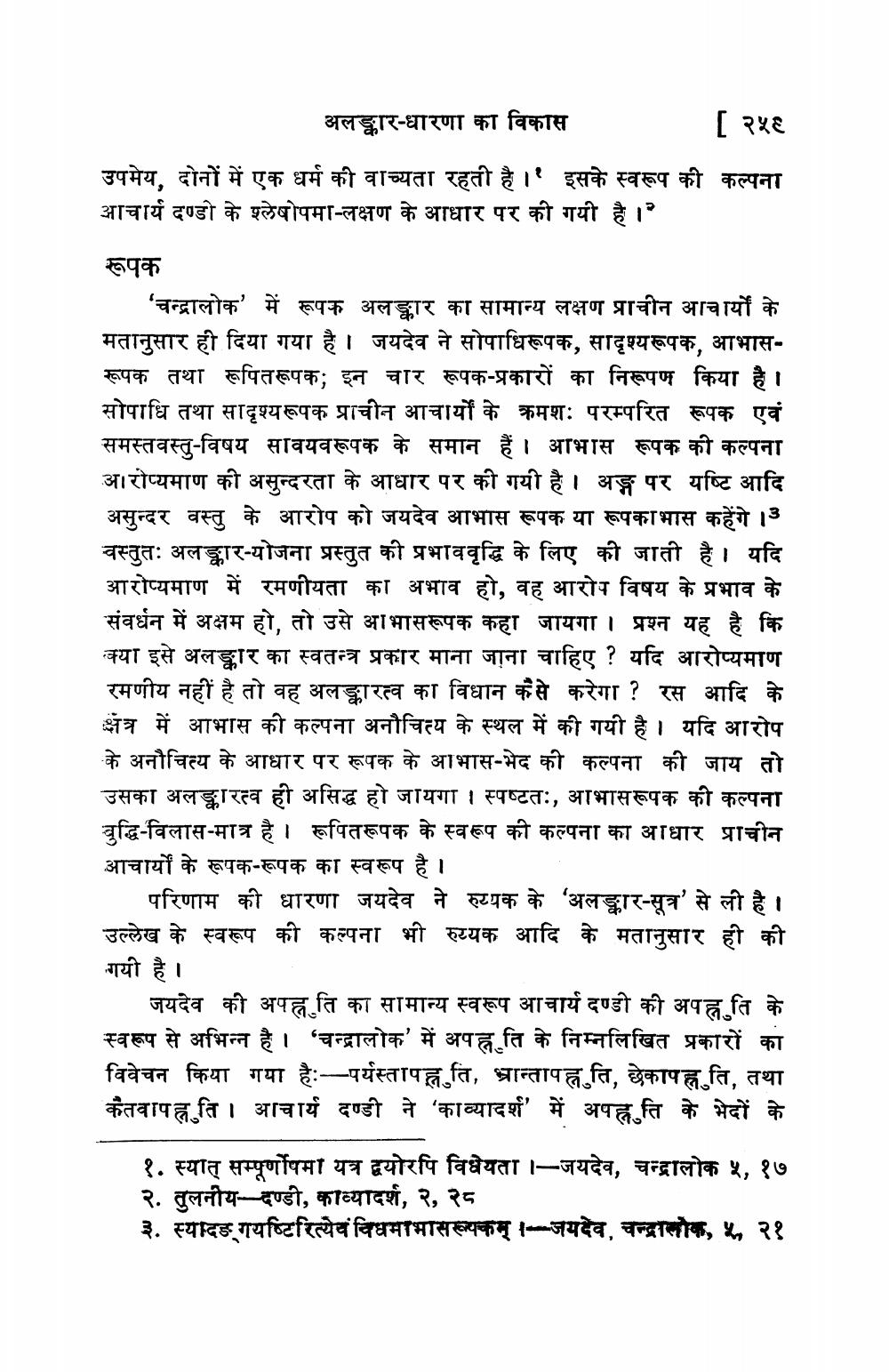________________
अलङ्कार-धारणा का विकास
[ २५६ उपमेय, दोनों में एक धर्म की वाच्यता रहती है।' इसके स्वरूप की कल्पना आचार्य दण्डी के श्लेषोपमा-लक्षण के आधार पर की गयी है।'
रूपक
'चन्द्रालोक' में रूपक अलङ्कार का सामान्य लक्षण प्राचीन आचार्यों के मतानुसार ही दिया गया है। जयदेव ने सोपाधिरूपक, सादृश्यरूपक, आभासरूपक तथा रूपितरूपक; इन चार रूपक-प्रकारों का निरूपण किया है। सोपाधि तथा सादृश्यरूपक प्राचीन आचार्यों के क्रमशः परम्परित रूपक एवं समस्तवस्तु-विषय सावयवरूपक के समान हैं। आभास रूपक की कल्पना आरोप्यमाण की असुन्दरता के आधार पर की गयी है। अङ्ग पर यष्टि आदि असुन्दर वस्तु के आरोप को जयदेव आभास रूपक या रूपकाभास कहेंगे । वस्तुतः अलङ्कार-योजना प्रस्तुत की प्रभाववृद्धि के लिए की जाती है। यदि आरोप्यमाण में रमणीयता का अभाव हो, वह आरोप विषय के प्रभाव के संवर्धन में अक्षम हो, तो उसे आभासरूपक कहा जायगा। प्रश्न यह है कि क्या इसे अलङ्कार का स्वतन्त्र प्रकार माना जाना चाहिए ? यदि आरोप्यमाण रमणीय नहीं है तो वह अलङ्कारत्व का विधान कैसे करेगा ? रस आदि के क्षेत्र में आभास की कल्पना अनौचित्य के स्थल में की गयी है। यदि आरोप के अनौचित्य के आधार पर रूपक के आभास-भेद की कल्पना की जाय तो उसका अलङ्कारत्व ही असिद्ध हो जायगा । स्पष्टतः, आभासरूपक की कल्पना बुद्धि-विलास-मात्र है। रूपितरूपक के स्वरूप की कल्पना का आधार प्राचीन आचार्यों के रूपक-रूपक का स्वरूप है।
परिणाम की धारणा जयदेव ने रुय्यक के 'अलङ्कार-सूत्र' से ली है। उल्लेख के स्वरूप की कल्पना भी रुय्यक आदि के मतानुसार ही की गयी है।
जयदेव की अपह्न ति का सामान्य स्वरूप आचार्य दण्डी की अपह्नति के स्वरूप से अभिन्न है। 'चन्द्रालोक' में अपह्नति के निम्नलिखित प्रकारों का विवेचन किया गया है:-पर्यस्तापह्न ति, भ्रान्तापह्न ति, छेकापह्न ति, तथा कैतवापह्नति । आचार्य दण्डी ने 'काव्यादर्श' में अपह्नति के भेदों के
१. स्यात् सम्पूर्णोपमा यत्र द्वयोरपि विधेयता । जयदेव, चन्द्रालोक ५, १७ २. तुलनीय-दण्डी, काव्यादर्श, २, २८ ३. स्यादङ गयष्टिरित्येवं विधमाभासख्यकम् ।-जयदेव, चन्द्रालोक, ५, २१