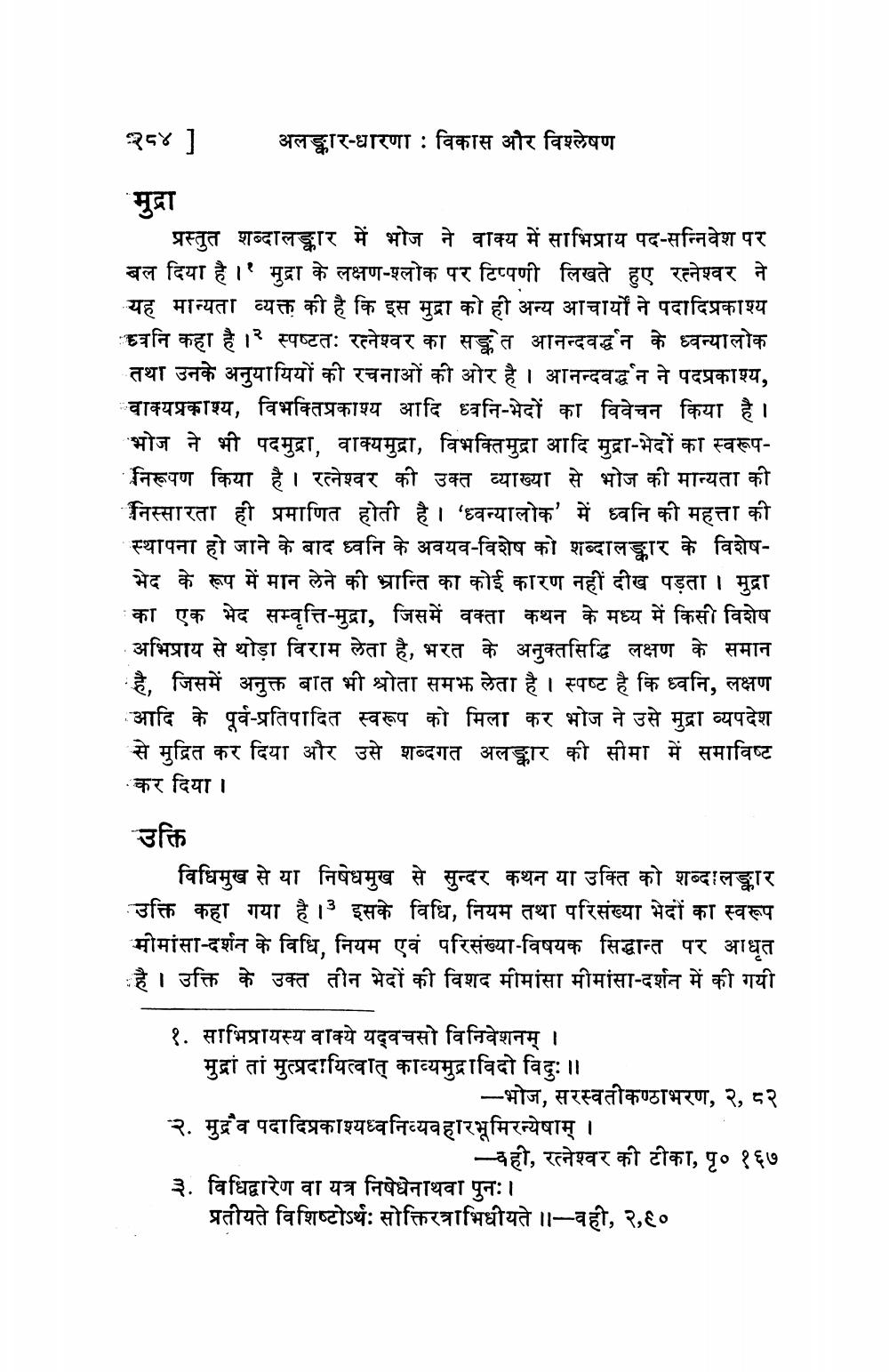________________
२८४ ]
अलङ्कार-धारणा : विकास और विश्लेषण
मुद्रा
प्रस्तुत शब्दालङ्कार में भोज ने वाक्य में साभिप्राय पद-सन्निवेश पर बल दिया है । ' मुद्रा के लक्षण-श्लोक पर टिप्पणी लिखते हुए रत्नेश्वर ने यह मान्यता व्यक्त की है कि इस मुद्रा को ही अन्य आचार्यों ने पदादिप्रकाश्य 'ध्वनि कहा है ।२ स्पष्टतः रत्नेश्वर का सङ्कत आनन्दवर्द्धन के ध्वन्यालोक तथा उनके अनुयायियों की रचनाओं की ओर है । आनन्दवद्धन ने पदप्रकाश्य, वाक्यप्रकाश्य, विभक्तिप्रकाश्य आदि ध्वनि-भेदों का विवेचन किया है। भोज ने भी पदमुद्रा, वाक्यमुद्रा, विभक्तिमुद्रा आदि मुद्रा-भेदों का स्वरूपनिरूपण किया है। रत्नेश्वर की उक्त व्याख्या से भोज की मान्यता की निस्सारता ही प्रमाणित होती है। 'ध्वन्यालोक' में ध्वनि की महत्ता की स्थापना हो जाने के बाद ध्वनि के अवयव-विशेष को शब्दालङ्कार के विशेषभेद के रूप में मान लेने की भ्रान्ति का कोई कारण नहीं दीख पड़ता। मुद्रा का एक भेद सम्वृत्ति-मुद्रा, जिसमें वक्ता कथन के मध्य में किसी विशेष अभिप्राय से थोड़ा विराम लेता है, भरत के अनुक्तसिद्धि लक्षण के समान है, जिसमें अनुक्त बात भी श्रोता समझ लेता है । स्पष्ट है कि ध्वनि, लक्षण आदि के पूर्व-प्रतिपादित स्वरूप को मिला कर भोज ने उसे मुद्रा व्यपदेश से मुद्रित कर दिया और उसे शब्दगत अलङ्कार की सीमा में समाविष्ट कर दिया। उक्ति
विधिमुख से या निषेधमुख से सुन्दर कथन या उक्ति को शब्दालङ्कार उक्ति कहा गया है। इसके विधि, नियम तथा परिसंख्या भेदों का स्वरूप मीमांसा-दर्शन के विधि, नियम एवं परिसंख्या-विषयक सिद्धान्त पर आधृत है। उक्ति के उक्त तीन भेदों की विशद मीमांसा मीमांसा-दर्शन में की गयी
१. साभिप्रायस्य वाक्ये यद्वचसो विनिवेशनम् । मुद्रां तां मुत्प्रदायित्वात् काव्यमुद्राविदो विदुः॥ ।
___-भोज, सरस्वतीकण्ठाभरण, २, ८२ २. मुद्रव पदादिप्रकाश्यध्वनिव्यवहारभूमिरन्येषाम् ।
-वही, रत्नेश्वर की टीका, पृ० १६७ ३. विधिद्वारेण वा यत्र निषेधेनाथवा पुनः।
प्रतीयते विशिष्टोऽर्थः सोक्तिरत्राभिधीयते ॥-वही, २,६०