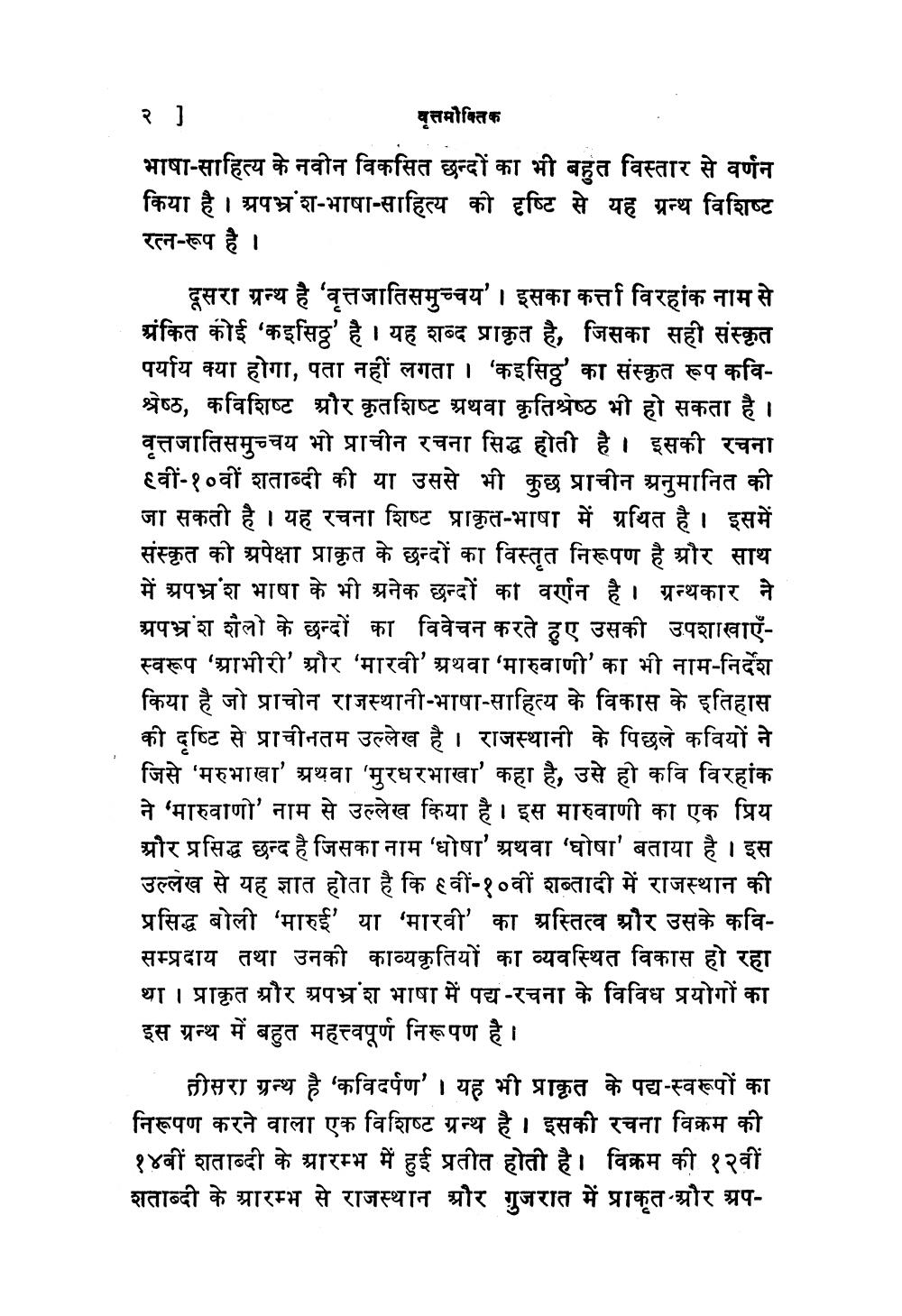________________
२ ]
वृत्तमौक्तिक भाषा-साहित्य के नवीन विकसित छन्दों का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। अपभ्रंश-भाषा-साहित्य की दृष्टि से यह ग्रन्थ विशिष्ट रत्न-रूप है।
दूसरा ग्रन्थ है 'वृत्तजातिसमुच्चय'। इसका कर्ता विरहांक नाम से अंकित कोई 'कइसिट्ठ' है । यह शब्द प्राकृत है, जिसका सही संस्कृत पर्याय क्या होगा, पता नहीं लगता। 'कइसिठ्ठ' का संस्कृत रूप कविश्रेष्ठ, कविशिष्ट और कृतशिष्ट अथवा कृतिश्रेष्ठ भी हो सकता है। वृत्तजातिसमुच्चय भी प्राचीन रचना सिद्ध होती है। इसकी रचना हवीं-१०वीं शताब्दी की या उससे भी कुछ प्राचीन अनुमानित की जा सकती है। यह रचना शिष्ट प्राकृत-भाषा में ग्रथित है। इसमें संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत के छन्दों का विस्तृत निरूपण है और साथ में अपभ्रंश भाषा के भी अनेक छन्दों का वर्णन है। ग्रन्थकार ने अपभ्रश शैलो के छन्दों का विवेचन करते हुए उसकी उपशाखाएँस्वरूप 'पाभीरी' और 'मारवी' अथवा 'मारुवाणी' का भी नाम-निर्देश किया है जो प्राचीन राजस्थानी-भाषा-साहित्य के विकास के इतिहास की दृष्टि से प्राचीनतम उल्लेख है। राजस्थानी के पिछले कवियों ने जिसे 'मरुभाखा' अथवा 'मुरधरभाखा' कहा है, उसे ही कवि विरहांक ने 'मारुवाणो' नाम से उल्लेख किया है। इस मारुवाणी का एक प्रिय और प्रसिद्ध छन्द है जिसका नाम 'धोषा' अथवा 'घोषा' बताया है । इस उल्लेख से यह ज्ञात होता है कि हवीं-१०वीं शब्तादी में राजस्थान की प्रसिद्ध बोली 'मारुई' या 'मारवी' का अस्तित्व और उसके कविसम्प्रदाय तथा उनकी काव्यकृतियों का व्यवस्थित विकास हो रहा था । प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में पद्य-रचना के विविध प्रयोगों का इस ग्रन्थ में बहुत महत्त्वपूर्ण निरूपण है।
तीसरा ग्रन्थ है 'कविदर्पण' । यह भी प्राकृत के पद्य-स्वरूपों का निरूपण करने वाला एक विशिष्ट ग्रन्थ है। इसकी रचना विक्रम की १४वीं शताब्दी के प्रारम्भ में हुई प्रतीत होती है। विक्रम की १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ से राजस्थान और गुजरात में प्राकृत और अप