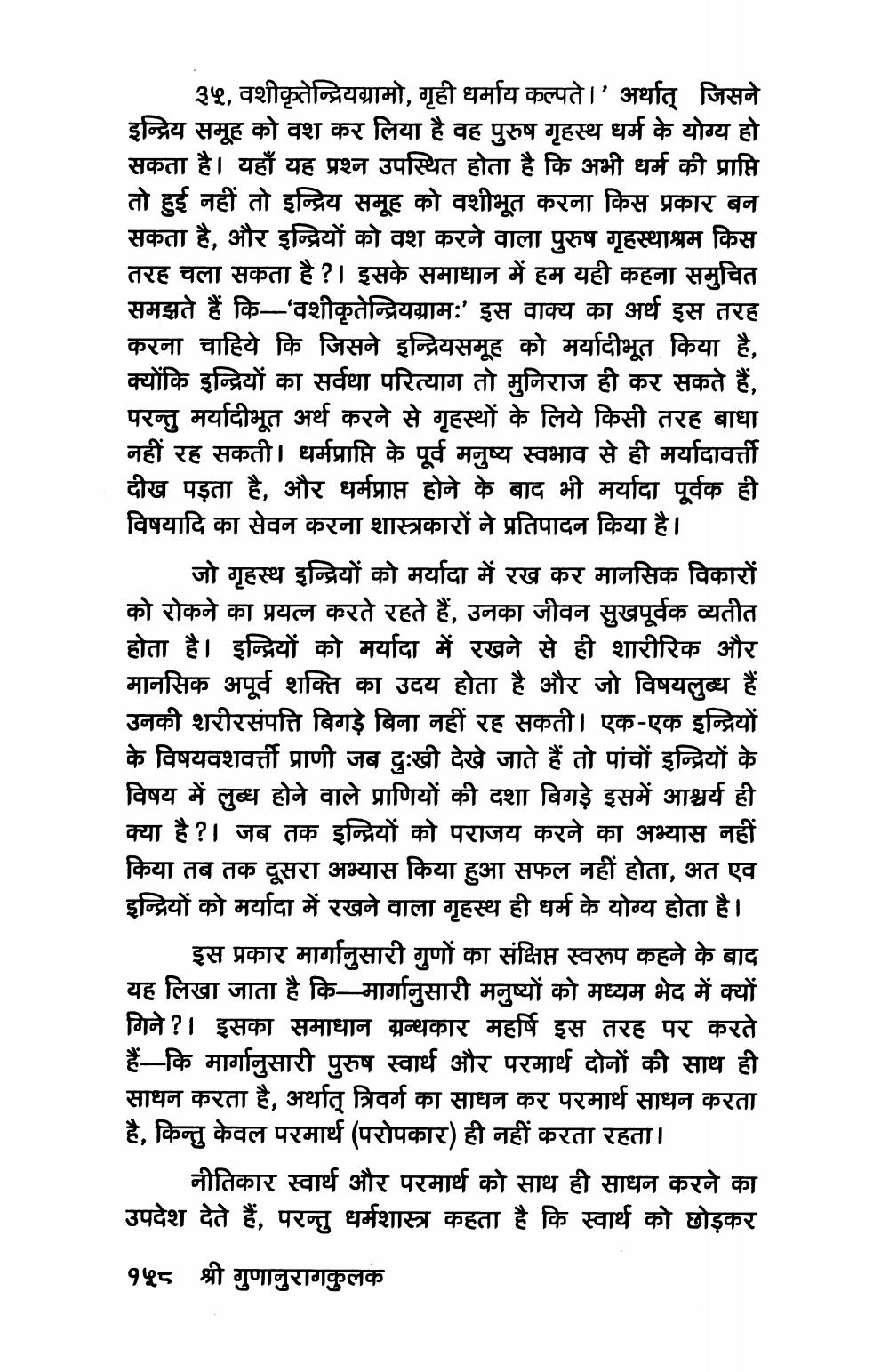________________
३५, वशीकृतेन्द्रियग्रामो, गृही धर्माय कल्पते ।' अर्थात् जिसने इन्द्रिय समूह को वश कर लिया है वह पुरुष गृहस्थ धर्म के योग्य हो सकता है। यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अभी धर्म की प्राप्ति तो हुई नहीं तो इन्द्रिय समूह को वशीभूत करना किस प्रकार बन सकता है, और इन्द्रियों को वश करने वाला पुरुष गृहस्थाश्रम किस तरह चला सकता है ? । इसके समाधान में हम यही कहना समुचित समझते हैं कि-'वशीकृतेन्द्रियग्राम:' इस वाक्य का अर्थ इस तरह करना चाहिये कि जिसने इन्द्रियसमूह को मर्यादीभूत किया है, क्योंकि इन्द्रियों का सर्वथा परित्याग तो मुनिराज ही कर सकते हैं, परन्तु मर्यादीभूत अर्थ करने से गृहस्थों के लिये किसी तरह बाधा नहीं रह सकती। धर्मप्राप्ति के पूर्व मनुष्य स्वभाव से ही मर्यादावर्त्ती दीख पड़ता है, और धर्मप्राप्त होने के बाद भी मर्यादा पूर्वक ही विषयादि का सेवन करना शास्त्रकारों ने प्रतिपादन किया है।
जो गृहस्थ इन्द्रियों को मर्यादा में रख कर मानसिक विकारों को रोकने का प्रयत्न करते रहते हैं, उनका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता है । इन्द्रियों को मर्यादा में रखने से ही शारीरिक और मानसिक अपूर्व शक्ति का उदय होता है और जो विषयलुब्ध हैं उनकी शरीरसंपत्ति बिगड़े बिना नहीं रह सकती। एक-एक इन्द्रियों के विषयवशवर्त्ती प्राणी जब दुःखी देखे जाते हैं तो पांचों इन्द्रियों के विषय में लुब्ध होने वाले प्राणियों की दशा बिगड़े इसमें आश्चर्य ही क्या है ? | जब तक इन्द्रियों को पराजय करने का अभ्यास नहीं किया तब तक दूसरा अभ्यास किया हुआ सफल नहीं होता, अत एव इन्द्रियों को मर्यादा में रखने वाला गृहस्थ ही धर्म के योग्य होता है ।
इस प्रकार मार्गानुसारी गुणों का संक्षिप्त स्वरूप कहने के बाद यह लिखा जाता है कि – मार्गानुसारी मनुष्यों को मध्यम भेद में क्यों गिने ? | इसका समाधान ग्रन्थकार महर्षि इस तरह पर करते हैं— कि मार्गानुसारी पुरुष स्वार्थ और परमार्थ दोनों की साथ ही साधन करता है, अर्थात् त्रिवर्ग का साधन कर परमार्थ साधन करता है, किन्तु केवल परमार्थ (परोपकार) ही नहीं करता रहता ।
नीतिकार स्वार्थ और परमार्थ को साथ ही साधन करने का उपदेश देते हैं, परन्तु धर्मशास्त्र कहता है कि स्वार्थ को छोड़कर
१५८ श्री गुणानुरागकुलक