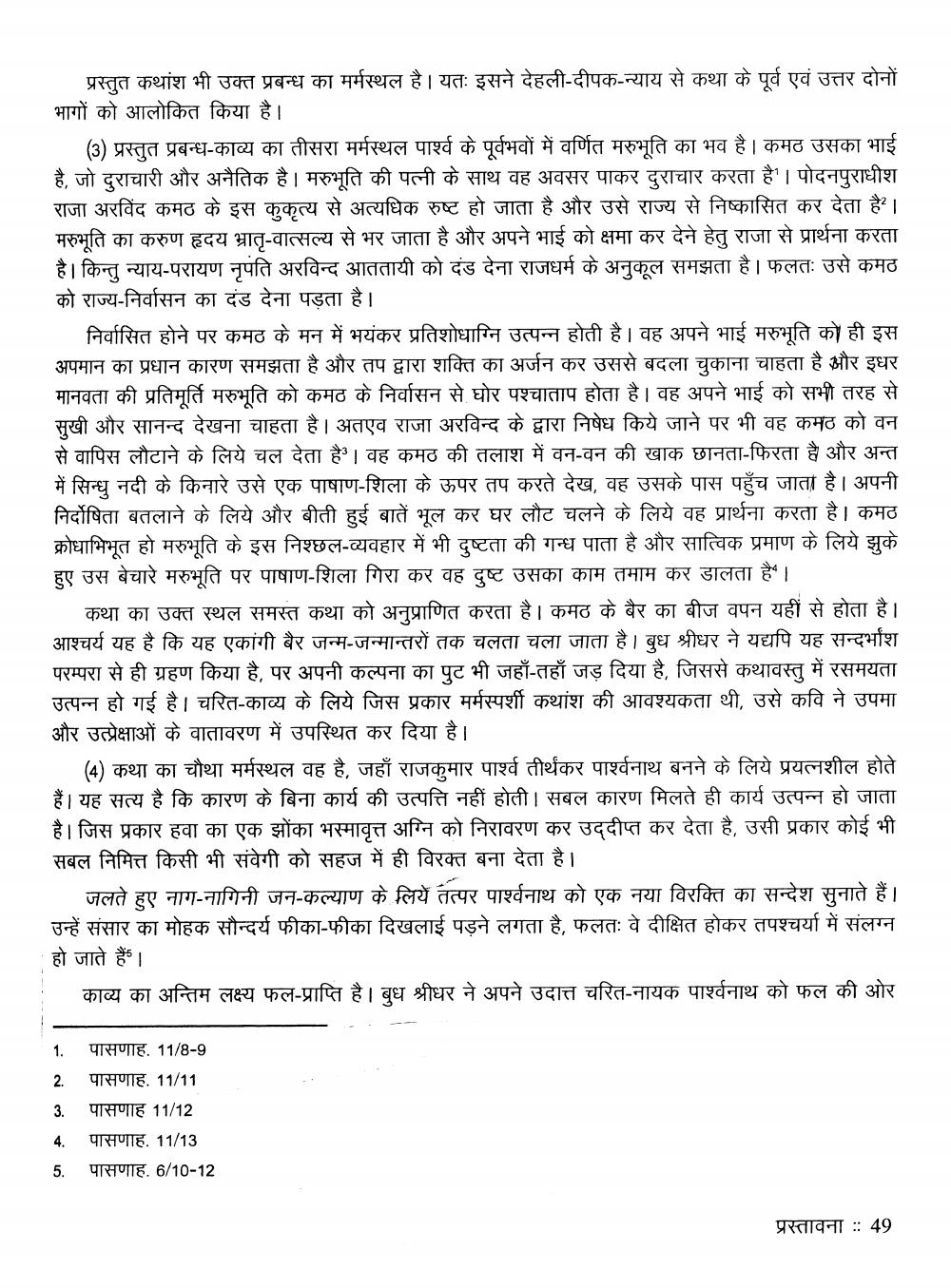________________
प्रस्तुत कथांश भी उक्त प्रबन्ध का मर्मस्थल है । यतः इसने देहली- दीपक न्याय से कथा के पूर्व एवं उत्तर दोनों भागों को आलोकित किया है।
(3) प्रस्तुत प्रबन्ध-काव्य का तीसरा मर्मस्थल पार्श्व के पूर्वभवों में वर्णित मरुभूति का भव है । कमठ उसका भाई है, जो दुराचारी और अनैतिक है । मरुभूति की पत्नी के साथ वह अवसर पाकर दुराचार करता है। पोदनपुराधीश राजा अरविंद कमठ के इस कुकृत्य से अत्यधिक रुष्ट हो जाता है और उसे राज्य से निष्कासित कर देता है' । मरुभूति का करुण हृदय भ्रातृ-वात्सल्य से भर जाता और अपने भाई को क्षमा कर देने हेतु राजा से प्रार्थना करता है । किन्तु न्याय-परायण नृपति अरविन्द आततायी को दंड देना राजधर्म के अनुकूल समझता है। फलतः उसे कमठ को राज्य निर्वासन का दंड देना पड़ता I
निर्वासित होने पर कमठ के मन में भयंकर प्रतिशोधाग्नि उत्पन्न होती है। वह अपने भाई मरुभूति को ही इस अपमान का प्रधान कारण समझता है और तप द्वारा शक्ति का अर्जन कर उससे बदला चुकाना चाहता है और इधर मानवता की प्रतिमूर्ति मरुभूति को कमठ के निर्वासन से घोर पश्चाताप होता है। वह अपने भाई को सभी तरह से सुखी और सानन्द देखना चाहता है। अतएव राजा अरविन्द के द्वारा निषेध किये जाने पर भी वह कमठ को वन से वापिस लौटाने के लिये चल देता है । वह कमठ की तलाश में वन-वन की खाक छानता-फिरता है और अन्त में सिन्धु नदी के किनारे उसे एक पाषाण शिला के ऊपर तप करते देख वह उसके पास पहुँच जाता है। अपनी निर्दोषिता बतलाने के लिये और बीती हुई बातें भूल कर घर लौट चलने के लिये वह प्रार्थना करता है । कमठ क्रोधाभिभूत हो मरुभूति के इस निश्छल व्यवहार में भी दुष्टता की गन्ध पाता है और सात्विक प्रमाण के लिये झुके हुए उस बेचारे मरुभूति पर पाषाण शिला गिरा कर वह दुष्ट उसका काम तमाम कर डालता है' ।
कथा का उक्त स्थल समस्त कथा को अनुप्राणित करता है । कमठ के बैर का बीज वपन यहीं से होता है । आश्चर्य यह है कि यह एकांगी बैर जन्म-जन्मान्तरों तक चलता चला जाता है। बुध श्रीधर ने यद्यपि यह सन्दर्भांश परम्परा से ही ग्रहण किया है, पर अपनी कल्पना का पुट भी जहाँ-तहाँ जड़ दिया है, जिससे कथावस्तु में रसमयता उत्पन्न हो गई है । चरित-काव्य के लिये जिस प्रकार मर्मस्पर्शी कथांश की आवश्यकता थी, उसे कवि ने उपमा और उत्प्रेक्षाओं के वातावरण में उपस्थित कर दिया है ।
(4) कथा का चौथा मर्मस्थल वह है, जहाँ राजकुमार पार्श्व तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनने के लिये प्रयत्नशील होते हैं। यह सत्य है कि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। सबल कारण मिलते ही कार्य उत्पन्न हो जाता है । जिस प्रकार हवा का एक झोंका भस्मावृत्त अग्नि को निरावरण कर उद्दीप्त कर देता है, उसी प्रकार कोई भी सबल निमित्त किसी भी संवेगी को सहज में ही विरक्त बना देता है।
जलते हुए नाग-नागिनी जन-कल्याण के लिये तत्पर पार्श्वनाथ को एक नया विरक्ति का सन्देश सुनाते हैं। उन्हें संसार का मोहक सौन्दर्य फीका-फीका दिखलाई पड़ने लगता है, फलतः वे दीक्षित होकर तपश्चर्या में संलग्न हो जाते हैं ।
काव्य का अन्तिम लक्ष्य फल प्राप्ति है। बुध श्रीधर ने अपने उदात्त चरित-नायक पार्श्वनाथ को फल की ओर
1.
2.
3.
4.
5.
पासणाह. 11/8-9
पासणाह. 11/11
पासणाह 11/12
पासणाह. 11/13
पासणाह. 6/10-12
प्रस्तावना :: 49