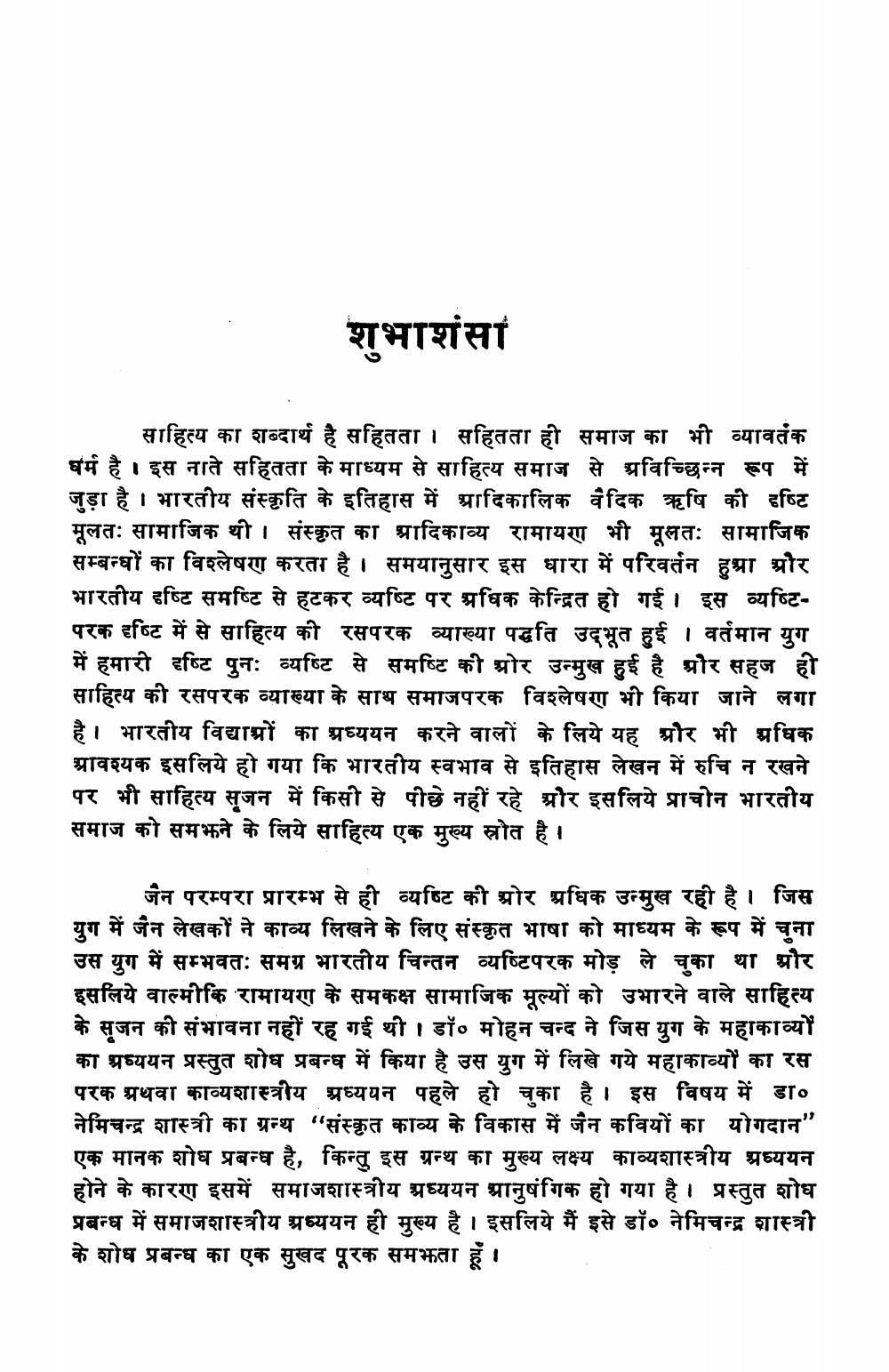________________
शुभाशंसा
साहित्य का शब्दार्थ है सहितता। सहितता ही समाज का भी व्यावतंक धर्म है । इस नाते सहितता के माध्यम से साहित्य समाज से अविच्छिन्न रूप में जुड़ा है । भारतीय संस्कृति के इतिहास में आदिकालिक वैदिक ऋषि की दृष्टि मूलतः सामाजिक थी। संस्कृत का प्रादिकाव्य रामायण भी मूलतः सामाजिक सम्बन्धों का विश्लेषण करता है। समयानुसार इस धारा में परिवर्तन हुआ और भारतीय दृष्टि समष्टि से हटकर व्यष्टि पर अधिक केन्द्रित हो गई। इस व्यष्टिपरक दृष्टि में से साहित्य की रसपरक व्याख्या पद्धति उद्भूत हुई । वर्तमान युग में हमारी दृष्टि पुनः व्यष्टि से समष्टि की ओर उन्मुख हुई है और सहज ही साहित्य की रसपरक व्याख्या के साथ समाजपरक विश्लेषण भी किया जाने लगा है। भारतीय विद्यानों का अध्ययन करने वालों के लिये यह और भी अधिक आवश्यक इसलिये हो गया कि भारतीय स्वभाव से इतिहास लेखन में रुचि न रखने पर भी साहित्य सृजन में किसी से पीछे नहीं रहे और इसलिये प्राचीन भारतीय समाज को समझने के लिये साहित्य एक मुख्य स्रोत है।
जैन परम्परा प्रारम्भ से ही व्यष्टि की ओर अधिक उन्मुख रही है। जिस युग में जैन लेखकों ने काव्य लिखने के लिए संस्कृत भाषा को माध्यम के रूप में चुना उस युग में सम्भवतः समग्र भारतीय चिन्तन व्यष्टिपरक मोड़ ले चुका था और इसलिये वाल्मीकि रामायण के समकक्ष सामाजिक मूल्यों को उभारने वाले साहित्य के सृजन की संभावना नहीं रह गई थी। डॉ० मोहन चन्द ने जिस युग के महाकाव्यों का अध्ययन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में किया है उस युग में लिखे गये महाकाव्यों का रस परक अथवा काव्यशास्त्रीय अध्ययन पहले हो चुका है। इस विषय में डा० नेमिचन्द्र शास्त्री का ग्रन्थ "संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान" एक मानक शोध प्रबन्ध है, किन्तु इस ग्रन्थ का मुख्य लक्ष्य काव्यशास्त्रीय अध्ययन होने के कारण इसमें समाजशास्त्रीय अध्ययन आनुषंगिक हो गया है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में समाजशास्त्रीय अध्ययन ही मुख्य है । इसलिये मैं इसे डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री के शोध प्रबन्ध का एक सुखद पूरक समझता हूँ।