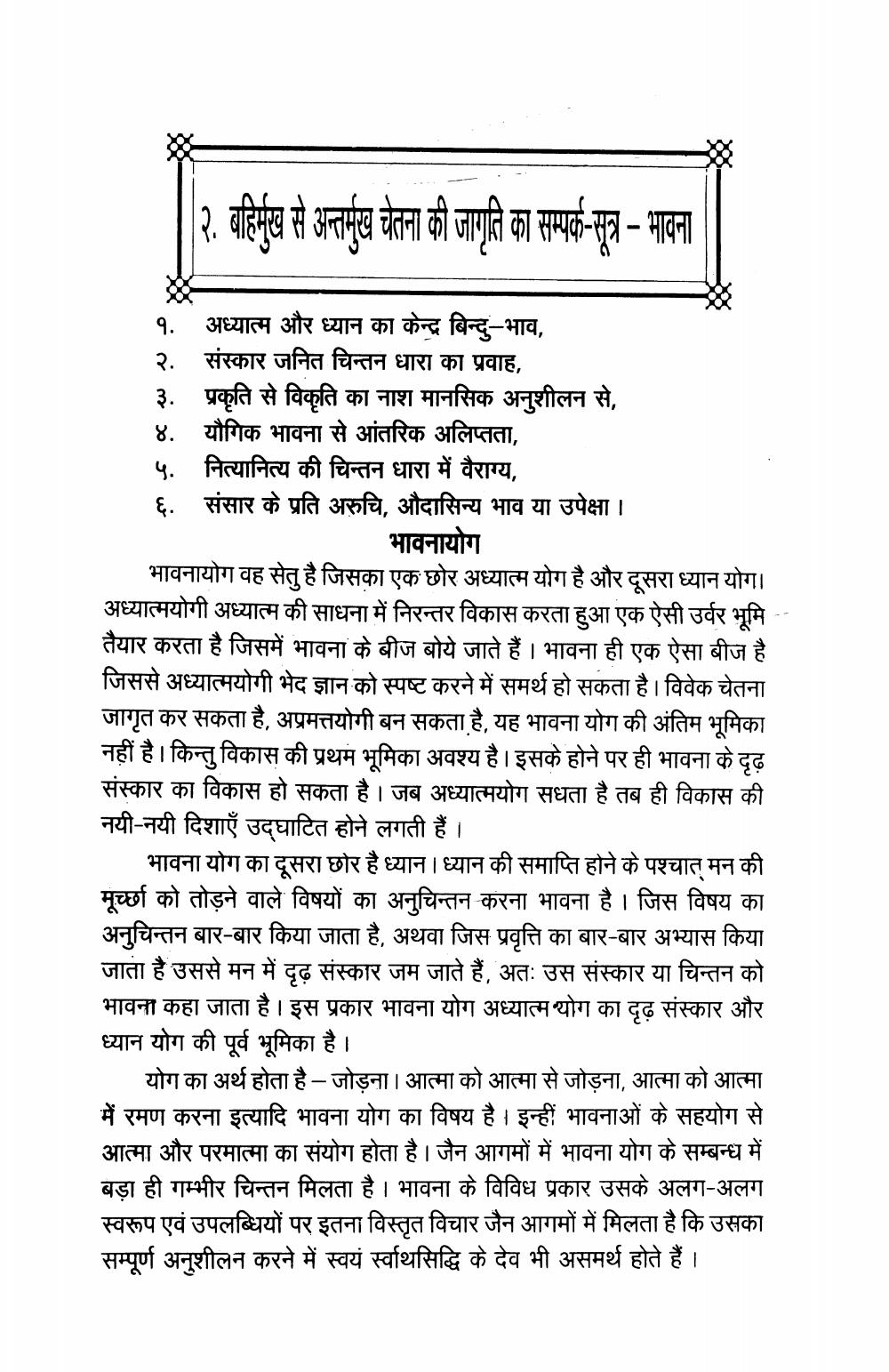________________
| २. बहिर्मुख से अन्तर्मुख चेतना की जागृति का सम्पर्क सूत्र - भावना
१. अध्यात्म और ध्यान का केन्द्र बिन्दु-भाव, २. संस्कार जनित चिन्तन धारा का प्रवाह, ३. प्रकृति से विकृति का नाश मानसिक अनुशीलन से, ४. यौगिक भावना से आंतरिक अलिप्तता, ५. नित्यानित्य की चिन्तन धारा में वैराग्य, ६. संसार के प्रति अरुचि, औदासिन्य भाव या उपेक्षा ।
भावनायोग भावनायोग वह सेतु है जिसका एक छोर अध्यात्म योग है और दूसरा ध्यान योग। अध्यात्मयोगी अध्यात्म की साधना में निरन्तर विकास करता हुआ एक ऐसी उर्वर भूमि तैयार करता है जिसमें भावना के बीज बोये जाते हैं । भावना ही एक ऐसा बीज है जिससे अध्यात्मयोगी भेद ज्ञान को स्पष्ट करने में समर्थ हो सकता है। विवेक चेतना जागृत कर सकता है, अप्रमत्तयोगी बन सकता है, यह भावना योग की अंतिम भूमिका नहीं है। किन्तु विकास की प्रथम भूमिका अवश्य है। इसके होने पर ही भावना के दृढ़ संस्कार का विकास हो सकता है। जब अध्यात्मयोग सधता है तब ही विकास की नयी-नयी दिशाएँ उद्घाटित होने लगती हैं ।
भावना योग का दूसरा छोर है ध्यान । ध्यान की समाप्ति होने के पश्चात् मन की मूर्छा को तोड़ने वाले विषयों का अनुचिन्तन करना भावना है। जिस विषय का अनुचिन्तन बार-बार किया जाता है, अथवा जिस प्रवृत्ति का बार-बार अभ्यास किया जाता है उससे मन में दृढ़ संस्कार जम जाते हैं, अतः उस संस्कार या चिन्तन को भावना कहा जाता है। इस प्रकार भावना योग अध्यात्म योग का दृढ़ संस्कार और ध्यान योग की पूर्व भूमिका है।
योग का अर्थ होता है-जोड़ना। आत्मा को आत्मा से जोड़ना, आत्मा को आत्मा में रमण करना इत्यादि भावना योग का विषय है। इन्हीं भावनाओं के सहयोग से आत्मा और परमात्मा का संयोग होता है। जैन आगमों में भावना योग के सम्बन्ध में बड़ा ही गम्भीर चिन्तन मिलता है। भावना के विविध प्रकार उसके अलग-अलग स्वरूप एवं उपलब्धियों पर इतना विस्तृत विचार जैन आगमों में मिलता है कि उसका सम्पूर्ण अनुशीलन करने में स्वयं थिसिद्धि के देव भी असमर्थ होते हैं ।