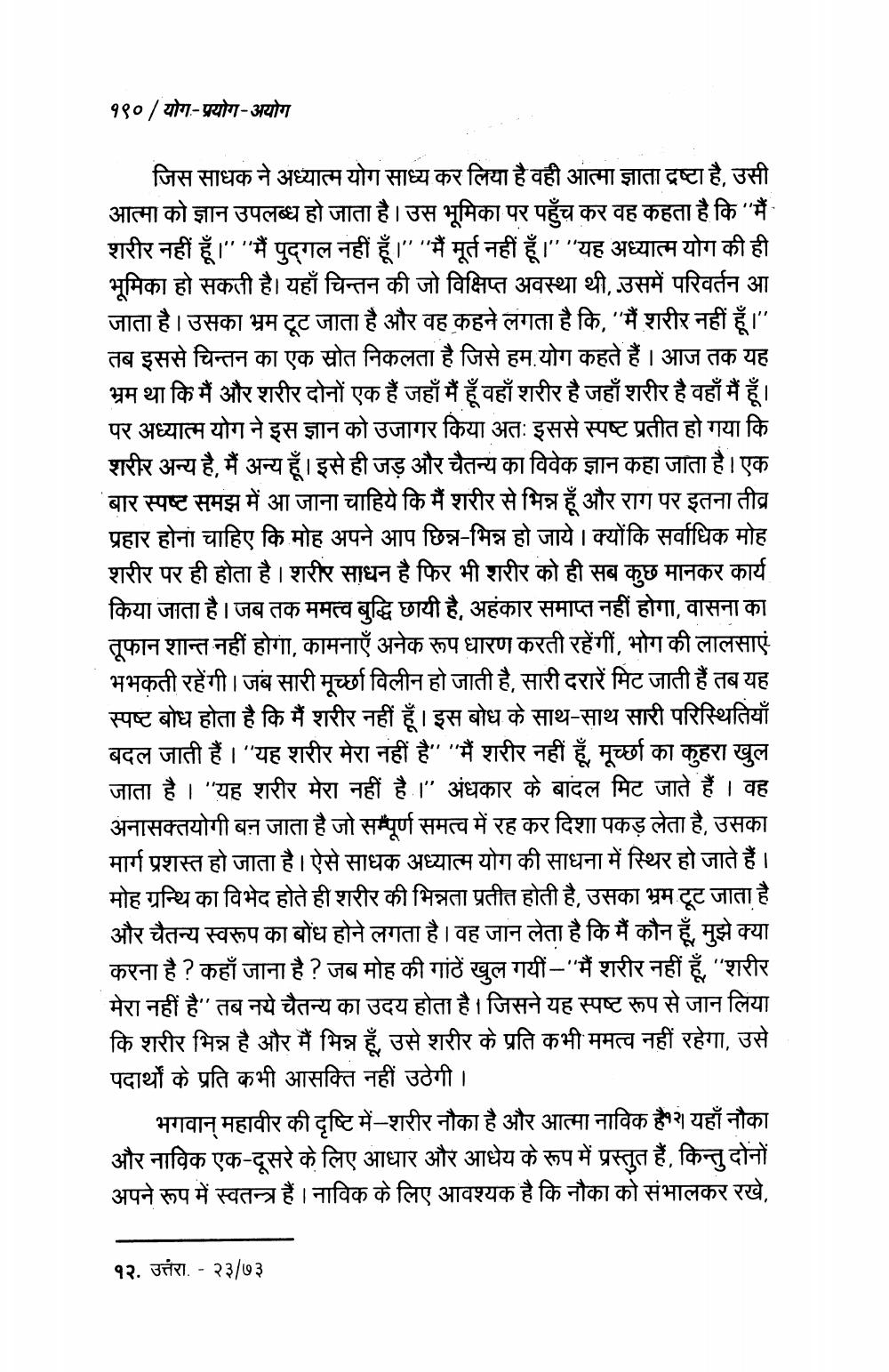________________
१९० / योग-प्रयोग-अयोग
जिस साधक ने अध्यात्म योग साध्य कर लिया है वही आत्मा ज्ञाता द्रष्टा है, उसी आत्मा को ज्ञान उपलब्ध हो जाता है। उस भूमिका पर पहुँच कर वह कहता है कि "मैं शरीर नहीं हूँ।" "मैं पुदगल नहीं हूँ।'' "मैं मूर्त नहीं हूँ।" "यह अध्यात्म योग की ही भूमिका हो सकती है। यहाँ चिन्तन की जो विक्षिप्त अवस्था थी, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसका भ्रम टूट जाता है और वह कहने लगता है कि, "मैं शरीर नहीं हैं।" तब इससे चिन्तन का एक स्रोत निकलता है जिसे हम.योग कहते हैं । आज तक यह भ्रम था कि मैं और शरीर दोनों एक हैं जहाँ मैं हूँ वहाँ शरीर है जहाँ शरीर है वहाँ मैं हूँ। पर अध्यात्म योग ने इस ज्ञान को उजागर किया अतः इससे स्पष्ट प्रतीत हो गया कि शरीर अन्य है, मैं अन्य हूँ। इसे ही जड़ और चैतन्य का विवेक ज्ञान कहा जाता है। एक बार स्पष्ट समझ में आ जाना चाहिये कि मैं शरीर से भिन्न हूँ और राग पर इतना तीव्र प्रहार होना चाहिए कि मोह अपने आप छिन्न-भिन्न हो जाये। क्योंकि सर्वाधिक मोह शरीर पर ही होता है। शरीर साधन है फिर भी शरीर को ही सब कुछ मानकर कार्य किया जाता है। जब तक ममत्व बुद्धि छायी है, अहंकार समाप्त नहीं होगा, वासना का तूफान शान्त नहीं होगा, कामनाएँ अनेक रूप धारण करती रहेंगी, भोग की लालसाएं भभकती रहेंगी। जब सारी मूर्छा विलीन हो जाती है, सारी दरारें मिट जाती हैं तब यह स्पष्ट बोध होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इस बोध के साथ-साथ सारी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं । "यह शरीर मेरा नहीं है" "मैं शरीर नहीं हूँ, मूर्छा का कुहरा खुल जाता है । "यह शरीर मेरा नहीं है ।" अंधकार के बादल मिट जाते हैं । वह अनासक्तयोगी बन जाता है जो सम्पूर्ण समत्व में रह कर दिशा पकड़ लेता है, उसका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ऐसे साधक अध्यात्म योग की साधना में स्थिर हो जाते हैं। मोह ग्रन्थि का विभेद होते ही शरीर की भिन्नता प्रतीत होती है, उसका भ्रम टूट जाता है और चैतन्य स्वरूप का बोध होने लगता है। वह जान लेता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है ? कहाँ जाना है? जब मोह की गांठें खुल गयीं- "मैं शरीर नहीं हूँ, "शरीर मेरा नहीं है" तब नये चैतन्य का उदय होता है। जिसने यह स्पष्ट रूप से जान लिया कि शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, उसे शरीर के प्रति कभी ममत्व नहीं रहेगा, उसे पदार्थों के प्रति कभी आसक्ति नहीं उठेगी।
भगवान महावीर की दृष्टि में शरीर नौका है और आत्मा नाविक है। यहाँ नौका और नाविक एक-दूसरे के लिए आधार और आधेय के रूप में प्रस्तुत हैं, किन्तु दोनों अपने रूप में स्वतन्त्र हैं । नाविक के लिए आवश्यक है कि नौका को संभालकर रखे,
१२. उत्तरा. - २३/७३