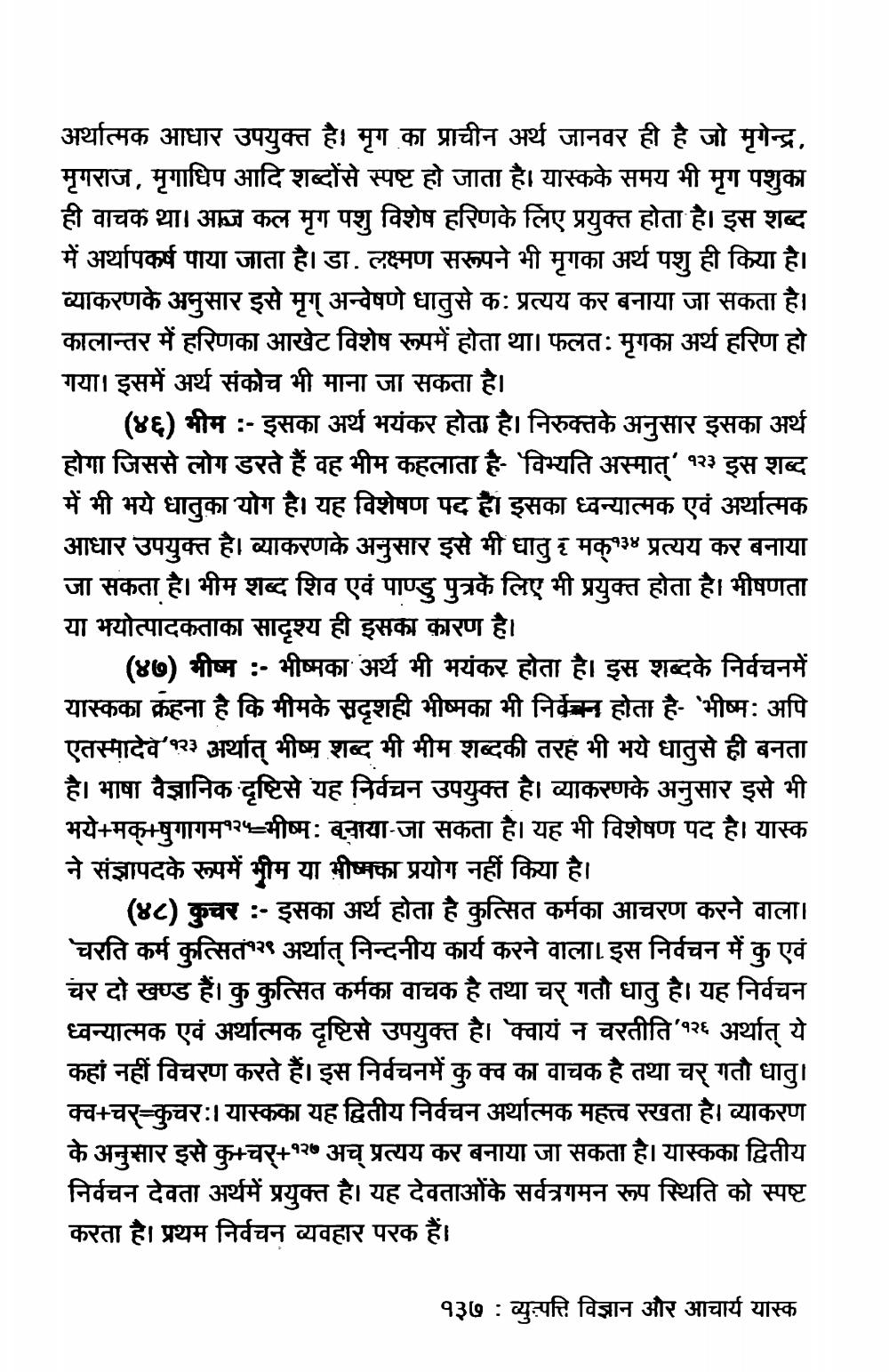________________
अर्थात्मक आधार उपयुक्त है। मृग का प्राचीन अर्थ जानवर ही है जो मृगेन्द्र, मृगराज, मृगाधिप आदि शब्दोंसे स्पष्ट हो जाता है। यास्कके समय भी मृग पशुका ही वाचक था। आज कल मृग पशु विशेष हरिणके लिए प्रयुक्त होता है। इस शब्द में अर्थापकर्ष पाया जाता है। डा. लक्ष्मण सरूपने भी मृगका अर्थ पशु ही किया है। व्याकरणके अनुसार इसे मृग् अन्वेषणे धातुसे कः प्रत्यय कर बनाया जा सकता है। कालान्तर में हरिणका आखेट विशेष रूपमें होता था। फलतः मृगका अर्थ हरिण हो गया। इसमें अर्थ संकोच भी माना जा सकता है।
(४६) भीम :- इसका अर्थ भयंकर होता है। निरुक्तके अनुसार इसका अर्थ होगा जिससे लोग डरते हैं वह भीम कहलाता है- 'विभ्यति अस्मात् १२३ इस शब्द में भी भये धातका योग है। यह विशेषण पद है। इसका ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक आधार उपयुक्त है। व्याकरणके अनुसार इसे मी धातु र मक्३४ प्रत्यय कर बनाया जा सकता है। भीम शब्द शिव एवं पाण्डु पुत्रके लिए भी प्रयुक्त होता है। भीषणता या भयोत्पादकताका सादृश्य ही इसका कारण है।
(४७) भीष्म :- भीष्मका अर्थ भी भयंकर होता है। इस शब्दके निर्वचनमें यास्कका कहना है कि भीमके सदृशही भीष्मका भी निर्वचन होता है- 'भीष्मः अपि एतस्मादेव'१२३ अर्थात् भीष्म शब्द भी भीम शब्दकी तरह भी भये धातुसे ही बनता है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टिसे यह निर्वचन उपयुक्त है। व्याकरणके अनुसार इसे भी भये+मक्षुगागम१२५=भीष्मः बनाया जा सकता है। यह भी विशेषण पद है। यास्क ने संज्ञापदके रूपमें भीम या भीष्मका प्रयोग नहीं किया है।
(४८) कुचर :- इसका अर्थ होता है कुत्सित कर्मका आचरण करने वाला। चरति कर्म कुत्सितं.२९ अर्थात् निन्दनीय कार्य करने वाला। इस निर्वचन में कु एवं चर दो खण्ड हैं। कु कुत्सित कर्मका वाचक है तथा चर् गतौ धातु है। यह निर्वचन ध्वन्यात्मक एवं अर्थात्मक दृष्टिसे उपयुक्त है। 'क्वायं न चरतीति'१२६ अर्थात् ये कहां नहीं विचरण करते हैं। इस निर्वचनमें कु क्व का वाचक है तथा चर् गतौ धातु। क्व+चर-कुचरः। यास्कका यह द्वितीय निर्वचन अर्थात्मक महत्व रखता है। व्याकरण के अनुसार इसे कु+च+१२७ अच् प्रत्यय कर बनाया जा सकता है। यास्कका द्वितीय निर्वचन देवता अर्थमें प्रयुक्त है। यह देवताओंके सर्वत्रगमन रूप स्थिति को स्पष्ट करता है। प्रथम निर्वचन व्यवहार परक हैं।
१३७ : व्युत्पत्ति विज्ञान और आचार्य यास्क