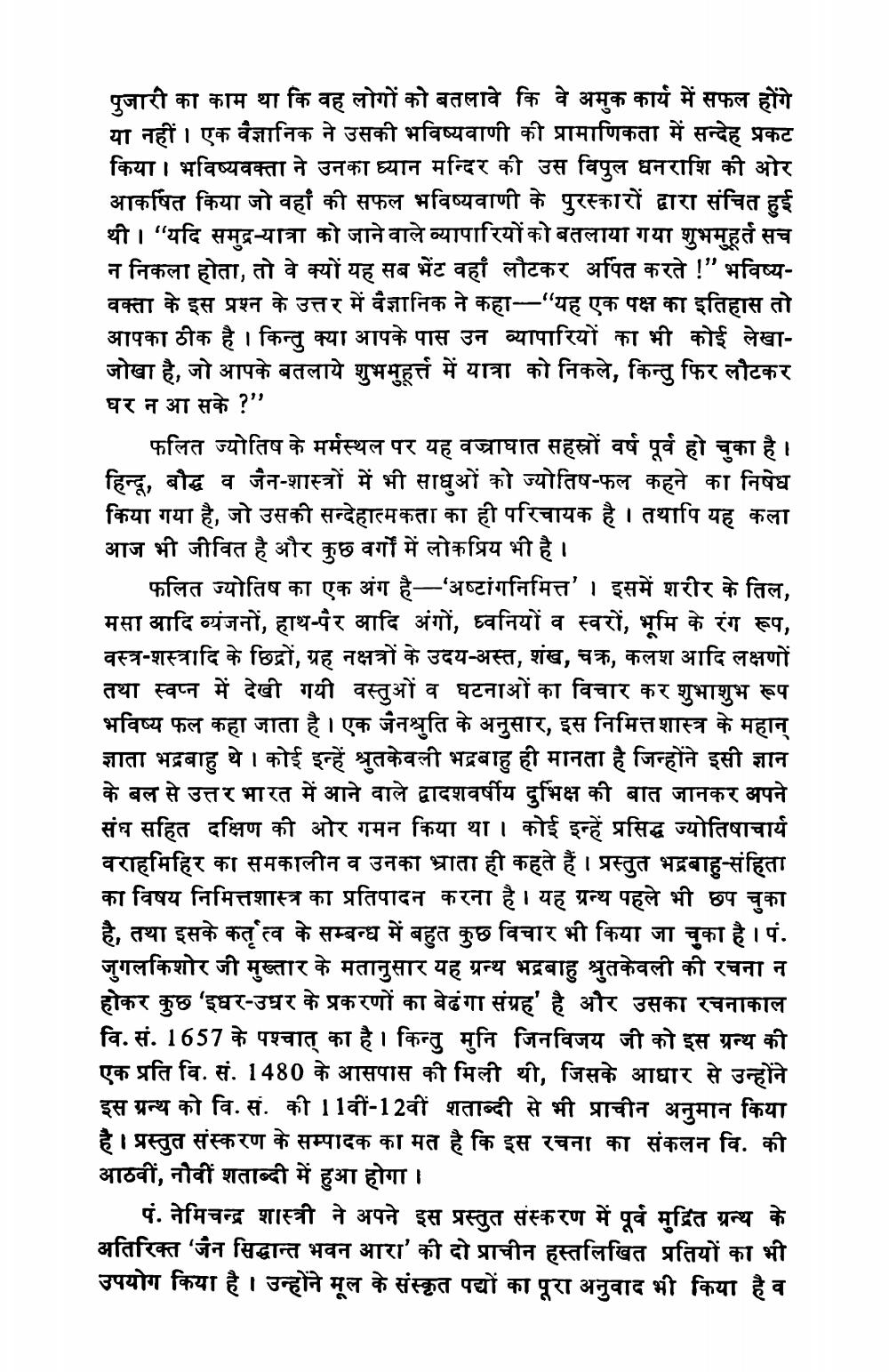________________
पुजारी का काम था कि वह लोगों को बतलावे कि वे अमुक कार्य में सफल होंगे या नहीं। एक वैज्ञानिक ने उसकी भविष्यवाणी की प्रामाणिकता में सन्देह प्रकट किया। भविष्यवक्ता ने उनका ध्यान मन्दिर की उस विपुल धनराशि की ओर आकर्षित किया जो वहां की सफल भविष्यवाणी के पुरस्कारों द्वारा संचित हुई थी। "यदि समुद्र-यात्रा को जाने वाले व्यापारियों को बतलाया गया शुभमुहुर्त सच न निकला होता, तो वे क्यों यह सब भेंट वहाँ लौटकर अर्पित करते !" भविष्यवक्ता के इस प्रश्न के उत्तर में वैज्ञानिक ने कहा-"यह एक पक्ष का इतिहास तो आपका ठीक है। किन्तु क्या आपके पास उन व्यापारियों का भी कोई लेखाजोखा है, जो आपके बतलाये शुभमुहूर्त में यात्रा को निकले, किन्तु फिर लौटकर घर न आ सके ?"
फलित ज्योतिष के मर्मस्थल पर यह वज्राघात सहस्रों वर्ष पूर्व हो चुका है। हिन्दू, बौद्ध व जैन-शास्त्रों में भी साधुओं को ज्योतिष-फल कहने का निषेध किया गया है, जो उसकी सन्देहात्मकता का ही परिचायक है । तथापि यह कला आज भी जीवित है और कुछ वर्गों में लोकप्रिय भी है।
फलित ज्योतिष का एक अंग है—'अष्टांगनिमित्त' । इसमें शरीर के तिल, मसा आदि व्यंजनों, हाथ-पैर आदि अंगों, ध्वनियों व स्वरों, भूमि के रंग रूप, वस्त्र-शस्त्रादि के छिद्रों, ग्रह नक्षत्रों के उदय-अस्त, शंख, चक्र, कलश आदि लक्षणों तथा स्वप्न में देखी गयी वस्तुओं व घटनाओं का विचार कर शुभाशुभ रूप भविष्य फल कहा जाता है । एक जनश्रुति के अनुसार, इस निमित्त शास्त्र के महान् ज्ञाता भद्रबाहु थे। कोई इन्हें श्रुतकेवली भद्रबाहु ही मानता है जिन्होंने इसी ज्ञान के बल से उत्तर भारत में आने वाले द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष की बात जानकर अपने संघ सहित दक्षिण की ओर गमन किया था। कोई इन्हें प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य वराहमिहिर का समकालीन व उनका भ्राता ही कहते हैं । प्रस्तुत भद्रबाहु-संहिता का विषय निमित्तशास्त्र का प्रतिपादन करना है। यह ग्रन्थ पहले भी छप चुका है, तथा इसके कर्तृत्व के सम्बन्ध में बहुत कुछ विचार भी किया जा चुका है । पं. जुगलकिशोर जी मुख्तार के मतानुसार यह ग्रन्थ भद्रबाहु श्रुतकेवली की रचना न होकर कुछ 'इधर-उधर के प्रकरणों का बेढंगा संग्रह' है और उसका रचनाकाल वि. सं. 1657 के पश्चात् का है। किन्तु मुनि जिनविजय जी को इस ग्रन्थ की एक प्रति वि. सं. 1480 के आसपास की मिली थी, जिसके आधार से उन्होंने इस ग्रन्थ को वि. सं. की 11वीं-12वीं शताब्दी से भी प्राचीन अनुमान किया है। प्रस्तुत संस्करण के सम्पादक का मत है कि इस रचना का संकलन वि. की आठवीं, नौवीं शताब्दी में हुआ होगा।
पं. नेमिचन्द्र शास्त्री ने अपने इस प्रस्तुत संस्करण में पूर्व मुद्रित ग्रन्थ के अतिरिक्त 'जैन सिद्धान्त भवन आरा' की दो प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों का भी उपयोग किया है। उन्होंने मूल के संस्कृत पद्यों का पूरा अनुवाद भी किया है व