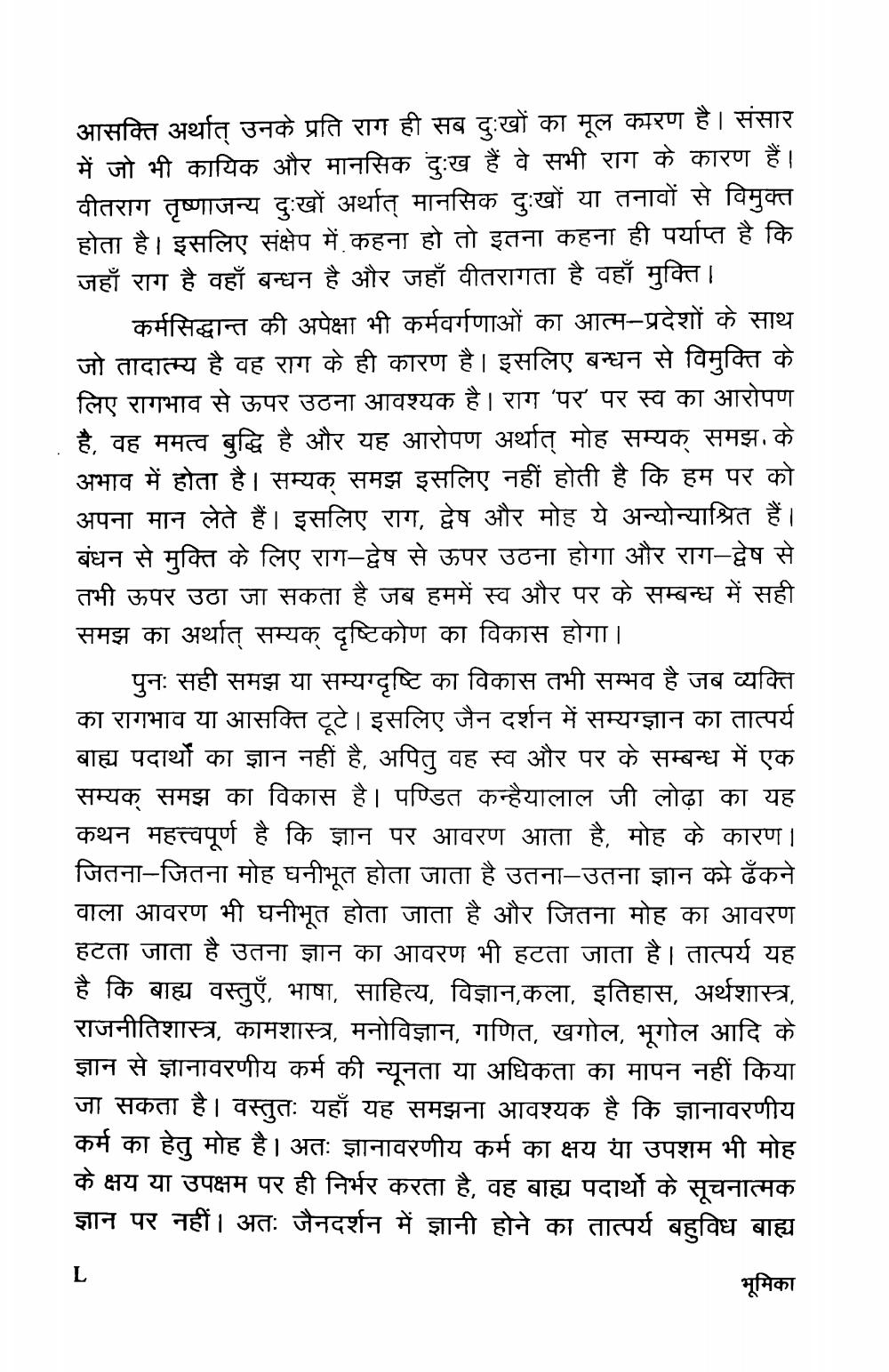________________
आसक्ति अर्थात् उनके प्रति राग ही सब दुःखों का मूल कारण है। संसार में जो भी कायिक और मानसिक दुःख हैं वे सभी राग के कारण हैं। वीतराग तृष्णाजन्य दुःखों अर्थात् मानसिक दुःखों या तनावों से विमुक्त होता है। इसलिए संक्षेप में कहना हो तो इतना कहना ही पर्याप्त है कि जहाँ राग है वहाँ बन्धन है और जहाँ वीतरागता है वहाँ मुक्ति।
कर्मसिद्धान्त की अपेक्षा भी कर्मवर्गणाओं का आत्म-प्रदेशों के साथ जो तादात्म्य है वह राग के ही कारण है। इसलिए बन्धन से विमुक्ति के लिए रागभाव से ऊपर उठना आवश्यक है। राग 'पर' पर स्व का आरोपण है, वह ममत्व बुद्धि है और यह आरोपण अर्थात् मोह सम्यक् समझ. के अभाव में होता है। सम्यक समझ इसलिए नहीं होती है कि हम पर को अपना मान लेते हैं। इसलिए राग, द्वेष और मोह ये अन्योन्याश्रित हैं। बंधन से मुक्ति के लिए राग-द्वेष से ऊपर उठना होगा और राग-द्वेष से तभी ऊपर उठा जा सकता है जब हममें स्व और पर के सम्बन्ध में सही समझ का अर्थात् सम्यक् दृष्टिकोण का विकास होगा।
पुनः सही समझ या सम्यग्दृष्टि का विकास तभी सम्भव है जब व्यक्ति का रागभाव या आसक्ति टूटे। इसलिए जैन दर्शन में सम्यग्ज्ञान का तात्पर्य बाह्य पदार्थों का ज्ञान नहीं है, अपितु वह स्व और पर के सम्बन्ध में एक सम्यक समझ का विकास है। पण्डित कन्हैयालाल जी लोढ़ा का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि ज्ञान पर आवरण आता है, मोह के कारण। जितना-जितना मोह घनीभूत होता जाता है उतना-उतना ज्ञान को ढंकने वाला आवरण भी घनीभूत होता जाता है और जितना मोह का आवरण हटता जाता है उतना ज्ञान का आवरण भी हटता जाता है। तात्पर्य यह है कि बाह्य वस्तुएँ, भाषा, साहित्य, विज्ञान,कला, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कामशास्त्र, मनोविज्ञान, गणित, खगोल, भूगोल आदि के ज्ञान से ज्ञानावरणीय कर्म की न्यूनता या अधिकता का मापन नहीं किया जा सकता है। वस्तुतः यहाँ यह समझना आवश्यक है कि ज्ञानावरणीय कर्म का हेतु मोह है। अतः ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय या उपशम भी मोह के क्षय या उपक्षम पर ही निर्भर करता है, वह बाह्य पदार्थो के सूचनात्मक ज्ञान पर नहीं। अतः जैनदर्शन में ज्ञानी होने का तात्पर्य बहुविध बाह्य
भूमिका