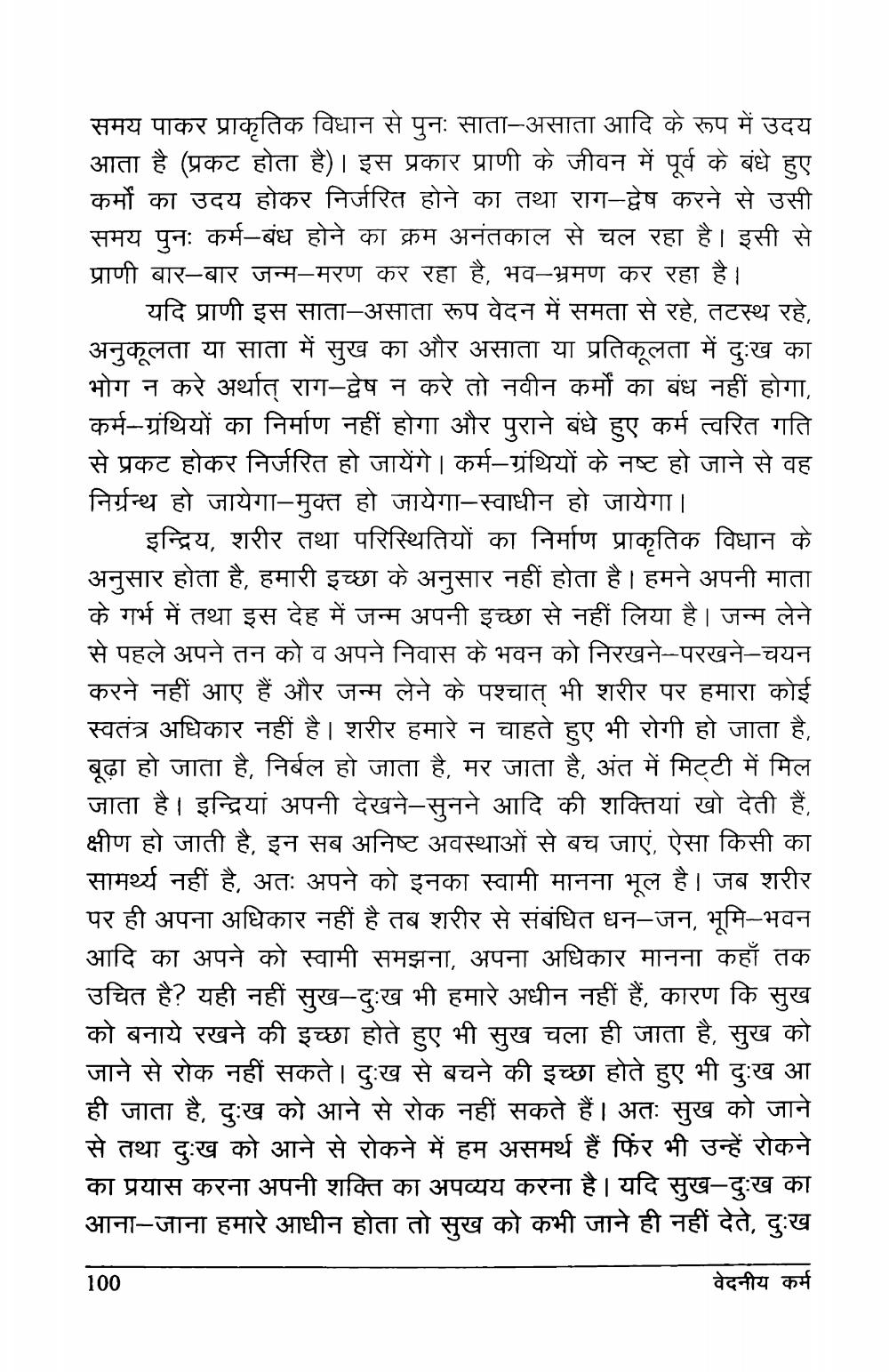________________
समय पाकर प्राकृतिक विधान से पुनः साता - असाता आदि के रूप में उदय आता है (प्रकट होता है)। इस प्रकार प्राणी के जीवन में पूर्व के बंधे हुए कर्मों का उदय होकर निर्जरित होने का तथा राग-द्वेष करने से उसी समय पुनः कर्म-बंध होने का क्रम अनंतकाल से चल रहा है। इसी से प्राणी बार-बार जन्म-मरण कर रहा है, भव-भ्रमण कर रहा है।
यदि प्राणी इस साता - असाता रूप वेदन में समता से रहे, तटस्थ रहे, अनुकूलता या साता में सुख का और असाता या प्रतिकूलता में दुःख का भोग न करे अर्थात् राग-द्वेष न करे तो नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा, कर्म-ग्रंथियों का निर्माण नहीं होगा और पुराने बंधे हुए कर्म त्वरित गति से प्रकट होकर निर्जरित हो जायेंगे । कर्म-ग्रंथियों के नष्ट हो जाने से वह निर्ग्रन्थ हो जायेगा - मुक्त हो जायेगा - स्वाधीन हो जायेगा ।
इन्द्रिय, शरीर तथा परिस्थितियों का निर्माण प्राकृतिक विधान के अनुसार होता है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है । हमने अपनी माता के गर्भ में तथा इस देह में जन्म अपनी इच्छा से नहीं लिया है। जन्म लेने से पहले अपने तन को व अपने निवास के भवन को निरखने-परखने - चयन करने नहीं आए हैं और जन्म लेने के पश्चात् भी शरीर पर हमारा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है । शरीर हमारे न चाहते हुए भी रोगी हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, निर्बल हो जाता है, मर जाता है, अंत में मिट्टी में मिल जाता है। इन्द्रियां अपनी देखने-सुनने आदि की शक्तियां खो देती हैं, क्षीण हो जाती है, इन सब अनिष्ट अवस्थाओं से बच जाएं, ऐसा किसी का सामर्थ्य नहीं है, अतः अपने को इनका स्वामी मानना भूल है। जब शरीर पर ही अपना अधिकार नहीं है तब शरीर से संबंधित धन-जन, भूमि-भवन आदि का अपने को स्वामी समझना, अपना अधिकार मानना कहाँ तक उचित है? यही नहीं सुख - दुःख भी हमारे अधीन नहीं हैं, कारण कि सुख को बनाये रखने की इच्छा होते हुए भी सुख चला ही जाता है, सुख को जाने से रोक नहीं सकते । दुःख से बचने की इच्छा होते हुए भी दुःख आ ही जाता है, दुःख को आने से रोक नहीं सकते हैं। अतः सुख को जाने से तथा दुःख को आने से रोकने में हम असमर्थ हैं फिर भी उन्हें रोकने का प्रयास करना अपनी शक्ति का अपव्यय करना है । यदि सुख-दुःख का आना-जाना हमारे आधीन होता तो सुख को कभी जाने ही नहीं देते, दुःख
वेदनीय कर्म
100