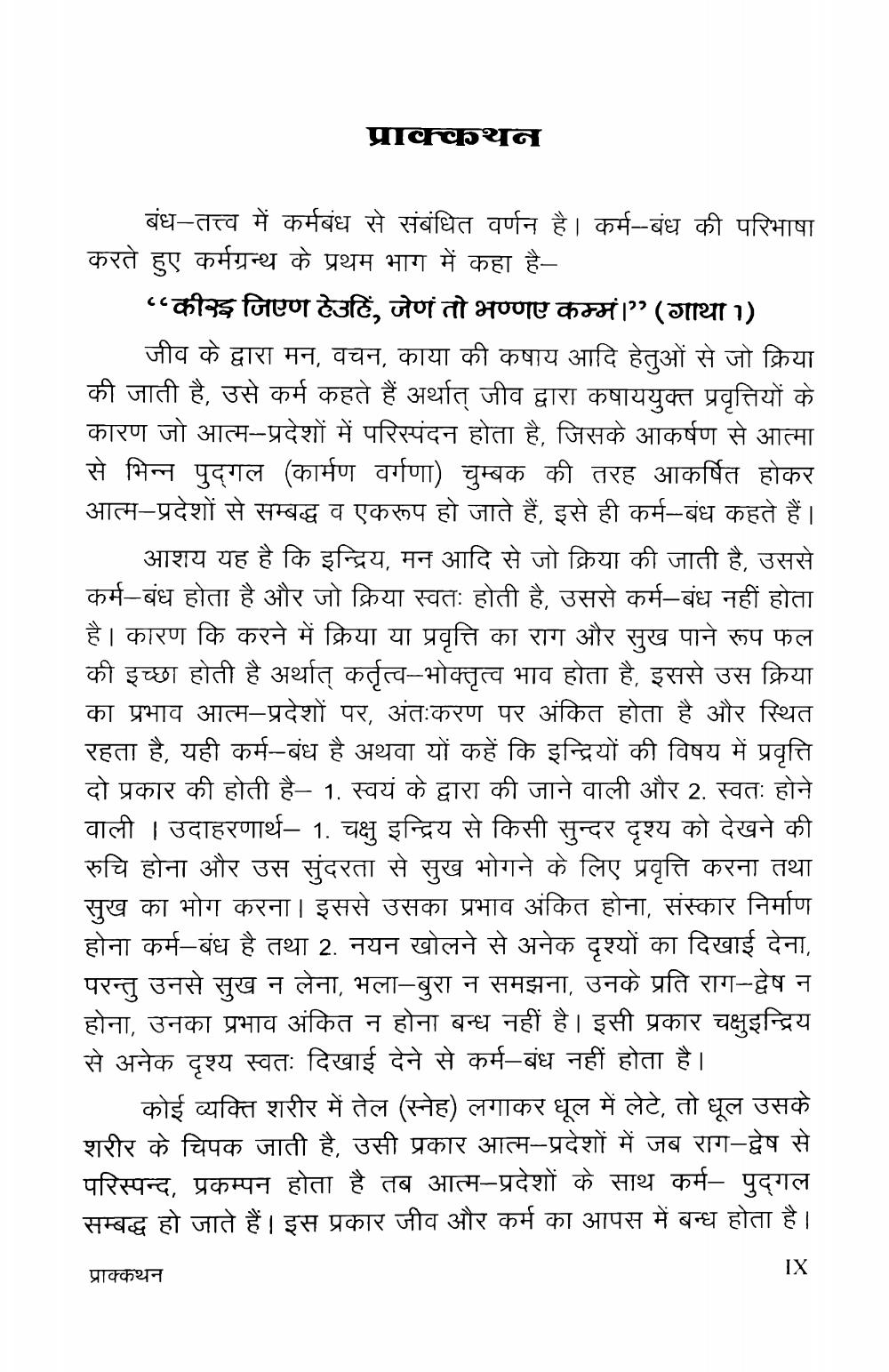________________
प्राक्कथन
बंध-तत्त्व में कर्मबंध से संबंधित वर्णन है। कर्म-बंध की परिभाषा करते हुए कर्मग्रन्थ के प्रथम भाग में कहा है
"कीरइ जिएण ठेउठिं, जेणं तो भण्णए कम्म।” (गाथा 1)
जीव के द्वारा मन, वचन, काया की कषाय आदि हेतुओं से जो क्रिया की जाती है, उसे कर्म कहते हैं अर्थात् जीव द्वारा कषाययुक्त प्रवृत्तियों के कारण जो आत्म-प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जिसके आकर्षण से आत्मा से भिन्न पुदगल (कार्मण वर्गणा) चुम्बक की तरह आकर्षित होकर आत्म-प्रदेशों से सम्बद्ध व एकरूप हो जाते हैं, इसे ही कर्म-बंध कहते हैं।
आशय यह है कि इन्द्रिय, मन आदि से जो क्रिया की जाती है, उससे कर्म-बंध होता है और जो क्रिया स्वतः होती है, उससे कर्म-बंध नहीं होता है। कारण कि करने में क्रिया या प्रवृत्ति का राग और सुख पाने रूप फल की इच्छा होती है अर्थात् कर्तृत्व-भोक्तृत्व भाव होता है, इससे उस क्रिया का प्रभाव आत्म-प्रदेशों पर, अंतःकरण पर अंकित होता है और स्थित रहता है, यही कर्म-बंध है अथवा यों कहें कि इन्द्रियों की विषय में प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है- 1. स्वयं के द्वारा की जाने वाली और 2. स्वतः होने वाली । उदाहरणार्थ- 1. चक्षु इन्द्रिय से किसी सुन्दर दृश्य को देखने की रुचि होना और उस सुंदरता से सुख भोगने के लिए प्रवृत्ति करना तथा सुख का भोग करना। इससे उसका प्रभाव अंकित होना, संस्कार निर्माण होना कर्म-बंध है तथा 2. नयन खोलने से अनेक दृश्यों का दिखाई देना, परन्तु उनसे सुख न लेना, भला-बुरा न समझना, उनके प्रति राग-द्वेष न होना, उनका प्रभाव अंकित न होना बन्ध नहीं है। इसी प्रकार चक्षुइन्द्रिय से अनेक दृश्य स्वतः दिखाई देने से कर्म-बंध नहीं होता है।
कोई व्यक्ति शरीर में तेल (स्नेह) लगाकर धूल में लेटे, तो धूल उसके शरीर के चिपक जाती है, उसी प्रकार आत्म-प्रदेशों में जब राग-द्वेष से परिस्पन्द, प्रकम्पन होता है तब आत्म-प्रदेशों के साथ कर्म- पुदगल सम्बद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार जीव और कर्म का आपस में बन्ध होता है।
IX
प्राक्कथन