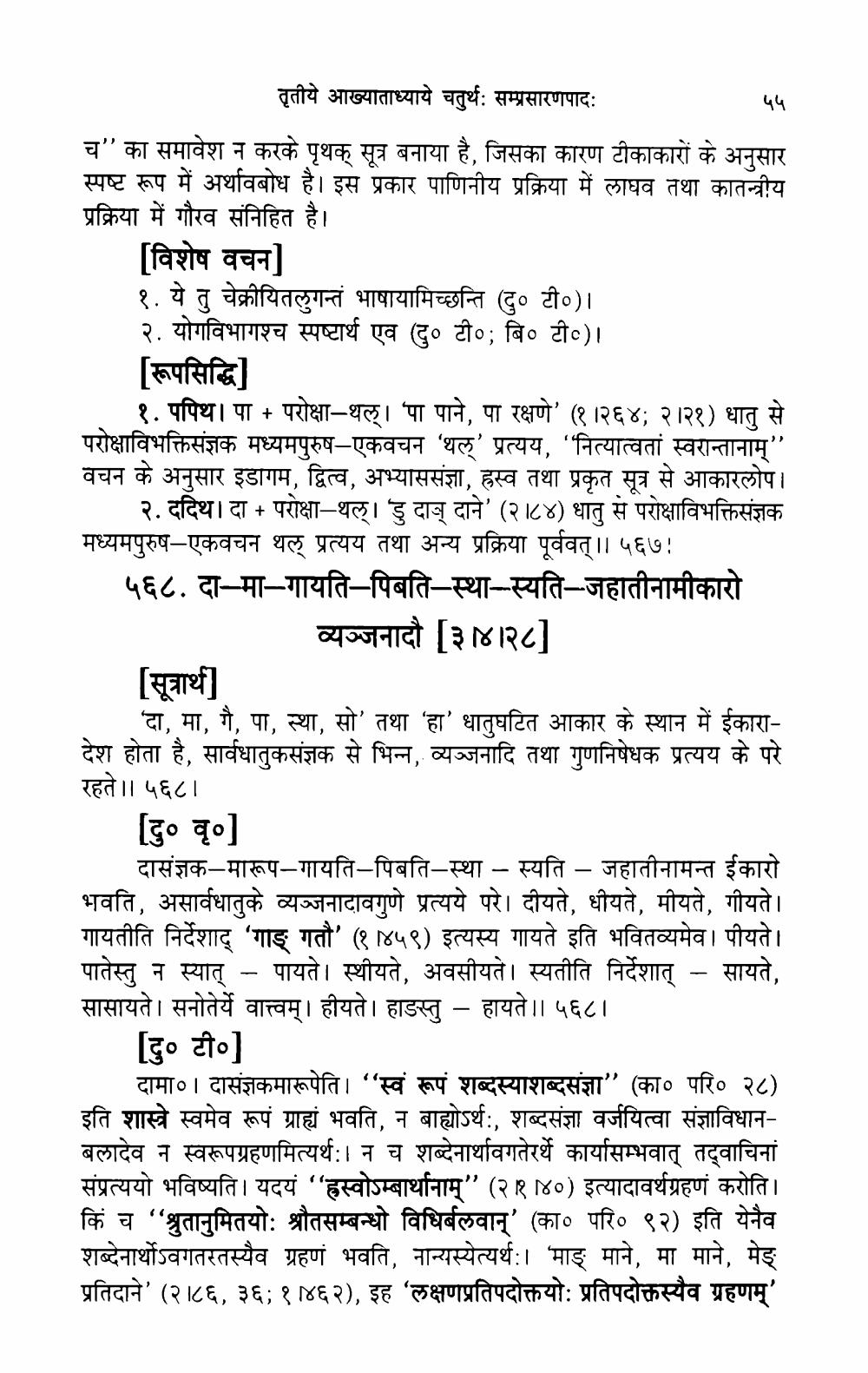________________
५५
तृतीये आख्याताध्याये चतुर्थः सम्प्रसारणपाद: च' का समावेश न करके पृथक् सूत्र बनाया है, जिसका कारण टीकाकारों के अनुसार स्पष्ट रूप में अर्थावबोध है। इस प्रकार पाणिनीय प्रक्रिया में लाघव तथा कातन्त्रीय प्रक्रिया में गौरव संनिहित है।
[विशेष वचन] १. ये तु चेक्रीयितलगन्तं भाषायामिच्छन्ति (द० टी०)। २. योगविभागश्च स्पष्टार्थ एव (दु० टी०; बि० टी०)। [रूपसिद्धि]
१. पपिथ। पा + परोक्षा-थल्। 'पा पाने, पा रक्षणे' (१।२६४; २।२१) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक मध्यमपुरुष–एकवचन 'थल्' प्रत्यय, “नित्यात्वतां स्वरान्तानाम्" वचन के अनुसार इडागम, द्वित्व, अभ्याससंज्ञा, ह्रस्व तथा प्रकृत सूत्र से आकारलोप।
२. ददिथ। दा + परोक्षा-थल्। 'डु दाञ् दाने' (२।८४) धातु से परोक्षाविभक्तिसंज्ञक मध्यमपुरुष–एकवचन थल् प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ।। ५६७ ५६८. दा–मा-गायति-पिबति-स्था-स्यति-जहातीनामीकारो
व्यञ्जनादौ [३।४।२८] [सूत्रार्थ]
'दा, मा, गै, पा, स्था, सो' तथा 'हा' धातुघटित आकार के स्थान में ईकारादेश होता है, सार्वधातकसंज्ञक से भिन्न, व्यञ्जनादि तथा गुणनिषेधक प्रत्यय के परे रहते।। ५६८।
[दु० वृ०]
दासंज्ञक-मारूप-गायति-पिबति-स्था – स्यति – जहातीनामन्त ईकारो भवति, असार्वधातुके व्यञ्जनादावगुणे प्रत्यये परे। दीयते, धीयते, मीयते, गीयते। गायतीति निर्देशाद् 'गाङ् गतौ' (१४५९) इत्यस्य गायते इति भवितव्यमेव। पीयते। पातेस्तु न स्यात् – पायते। स्थीयते, अवसीयते। स्यतीति निर्देशात् – सायते, सासायते। सनोतेर्ये वात्त्वम्। हीयते। हाङस्तु – हायते।। ५६८।
[दु० टी०]
दामा० । दासंज्ञकमारूपेति। "स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा" (का० परि० २८) इति शास्त्रे स्वमेव रूपं ग्राह्यं भवति, न बाह्योऽर्थः, शब्दसंज्ञा वर्जयित्वा संज्ञाविधानबलादेव न स्वरूपग्रहणमित्यर्थः। न च शब्देनार्थावगतेरर्थे कार्यासम्भवात् तद्वाचिनां संप्रत्ययो भविष्यति। यदयं "हस्वोऽम्बार्थानाम्" (२१४०) इत्यादावर्थग्रहणं करोति। किं च "श्रुतानुमितयोः श्रौतसम्बन्धी विधिर्बलवान्' (का० परि० ९२) इति येनैव शब्देनार्थोऽवगतस्तस्यैव ग्रहणं भवति, नान्यस्येत्यर्थः। 'माङ् माने, मा माने, मेङ् प्रतिदाने' (२।८६, ३६; १४६२), इह 'लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणम्'