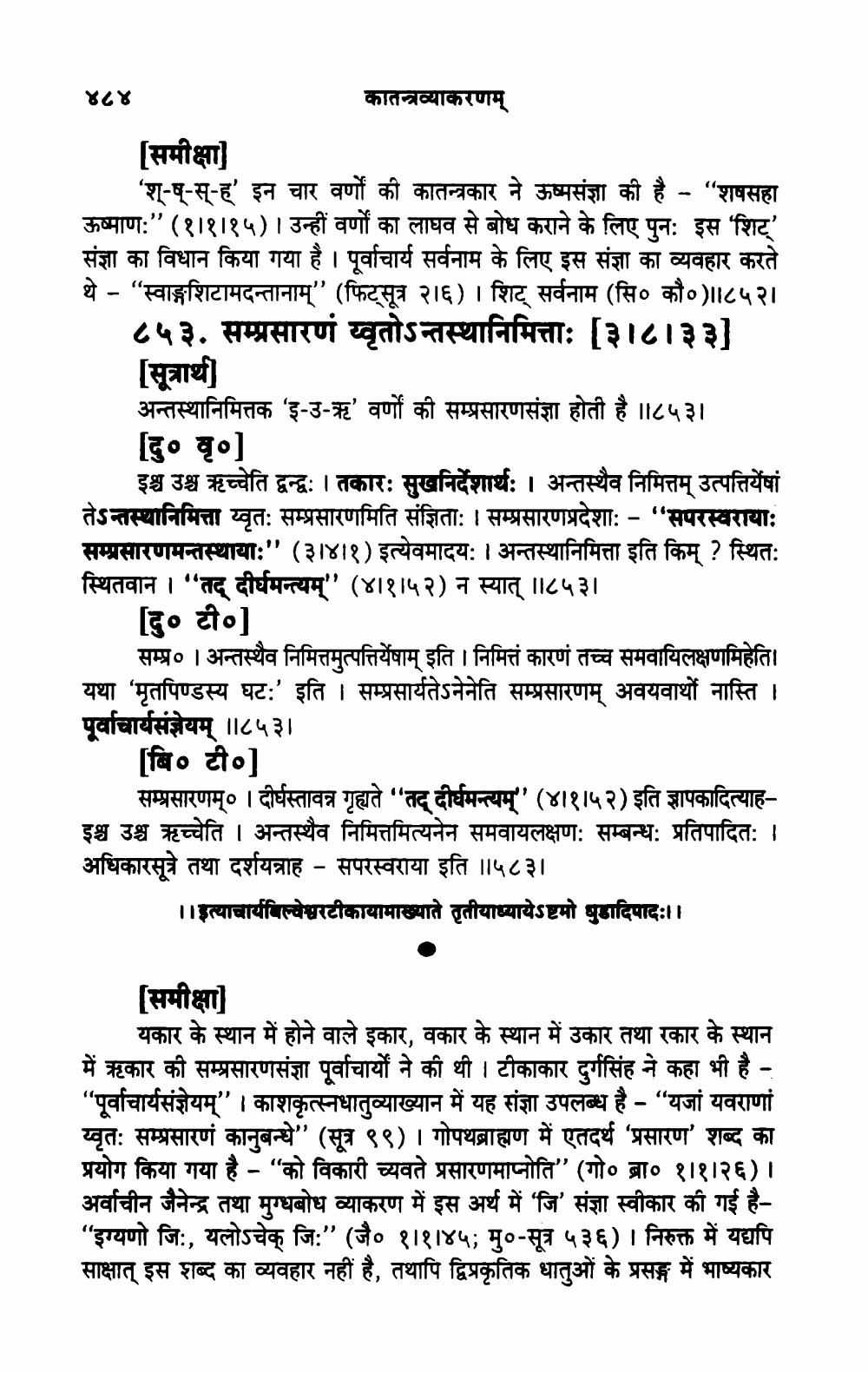________________
४८४
कातन्त्रव्याकरणम्
[समीक्षा
'श-प-स-ह' इन चार वर्णों की कातन्त्रकार ने ऊष्मसंज्ञा की है - "शषसहा ऊष्माणः” (१।१।१५)। उन्हीं वर्णों का लाघव से बोध कराने के लिए पुन: इस 'शिट्' संज्ञा का विधान किया गया है । पूर्वाचार्य सर्वनाम के लिए इस संज्ञा का व्यवहार करते थे - “स्वाङ्गशिटामदन्तानाम्' (फिट्सूत्र २।६) । शिट् सर्वनाम (सि० को०)।८५२।
८५३. सम्प्रसारणं वृतोऽन्तस्थानिमित्ताः [३।८।३३] [सूत्रार्थ अन्तस्थानिमित्तक 'इ-उ-ऋ' वर्गों की सम्प्रसारणसंज्ञा होती है ।।८५३। [दु० वृ०]
इश्च उश्च ऋच्चेति द्वन्द्वः । तकारः सुखनिर्देशार्थः । अन्तस्थैव निमित्तम् उत्पत्तिर्येषां तेऽन्तस्थानिमित्ता य्वृतः सम्प्रसारणमिति संज्ञिताः । सम्प्रसारणप्रदेशाः - "सपरस्वरायाः सम्प्रसारणमन्तस्थायाः" (३।४।१) इत्येवमादयः । अन्तस्थानिमित्ता इति किम् ? स्थितः स्थितवान । "तद् दीर्घमन्त्यम्" (४।१।५२) न स्यात् ।।८५३।
[दु० टी०]
सम्प्र० । अन्तस्यैव निमित्तमुत्पत्तिर्येषाम् इति । निमित्तं कारणं तच्च समवायिलक्षणमिहेति। यथा 'मृतपिण्डस्य घटः' इति । सम्प्रसार्यतेऽनेनेति सम्प्रसारणम् अवयवार्थो नास्ति । पूर्वाचार्यसंज्ञेयम् ।।८५३।
[बि० टी०]
सम्प्रसारणम् । दीर्घस्तावन्न गृह्यते "तद् दीर्घमन्त्यम्' (४।१।५२) इति ज्ञापकादित्याहइश्च उश्च ऋच्चेति । अन्तस्थैव निमित्तमित्यनेन समवायलक्षण: सम्बन्ध: प्रतिपादितः । अधिकारसूत्रे तथा दर्शयन्नाह - सपरस्वराया इति ।।५८३।
।इत्याचार्यविल्वेश्वरटीकायामाख्याते तृतीयाध्यायेऽष्टमो घुडादिपादः।।
[समीक्षा
यकार के स्थान में होने वाले इकार, वकार के स्थान में उकार तथा रकार के स्थान में ऋकार की सम्प्रसारणसंज्ञा पूर्वाचार्यों ने की थी । टीकाकार दुर्गसिंह ने कहा भी है - "पूर्वाचार्यसंज्ञेयम्" । काशकृत्स्नधातुव्याख्यान में यह संज्ञा उपलब्ध है - "यजां यवराणां वृतः सम्प्रसारणं कानुबन्धे" (सूत्र ९९) । गोपथब्राह्मण में एतदर्थ 'प्रसारण' शब्द का प्रयोग किया गया है - “को विकारी च्यवते प्रसारणमाप्नोति” (गो० ब्रा० १।१।२६)। अर्वाचीन जैनेन्द्र तथा मुग्धबोध व्याकरण में इस अर्थ में 'जि' संज्ञा स्वीकार की गई है"इग्यणो जि:, यलोऽचेक् जि:" (जै० १।१।४५; मु०-सूत्र ५३६) । निरुक्त में यद्यपि साक्षात् इस शब्द का व्यवहार नहीं है, तथापि द्विप्रकृतिक धातुओं के प्रसङ्ग में भाष्यकार