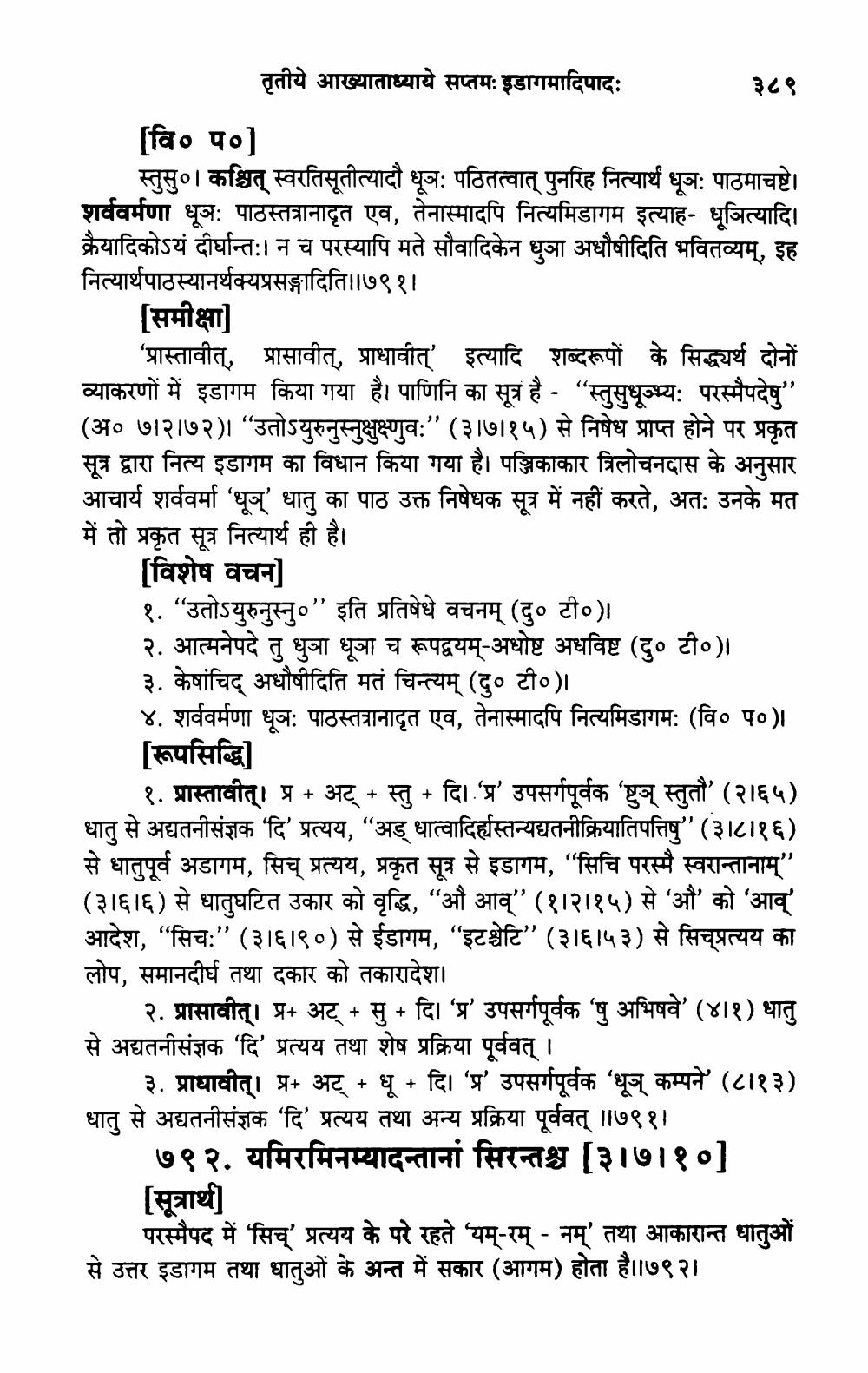________________
तृतीये आख्याताध्याये सप्तमः इडागमादिपादः
३८९
[वि० प० ]
स्तुसु०। कश्चित् स्वरतिसूतीत्यादौ धूञः पठितत्वात् पुनरिह नित्यार्थं धूञः पाठमाचष्टे। शर्ववर्मणा धूञः पाठस्तत्रानादृत एव तेनास्मादपि नित्यमिडागम इत्याह- धूञित्यादि । क्रैयादिकोऽयं दीर्घान्तः । न च परस्यापि मते सौवादिकेन धुञा अधौषीदिति भवितव्यम्, इह नित्यार्थपाठस्यानर्थक्यप्रसङ्गादिति ।। ७९१ । [समीक्षा]
'प्रास्तावीत्, प्रासावीत्, प्राधावीत्' इत्यादि शब्दरूपों के सिद्ध्यर्थ दोनों व्याकरणों में इडागम किया गया है। पाणिनि का सूत्र है- "स्तुसुधूञ्भ्यः परस्मैपदेषु” (अ० ७।२।७२)। “उतोऽयुरुनुस्नुक्षुक्ष्णुवः” (३।७।१५) से निषेध प्राप्त होने पर प्रकृत सूत्र द्वारा नित्य इडागम का विधान किया गया है। पञ्जिकाकार त्रिलोचनदास के अनुसार आचार्य शर्ववर्मा 'धूञ्' धातु का पाठ उक्त निषेधक सूत्र में नहीं करते, अतः उनके मत में तो प्रकृत सूत्र नित्यार्थ ही है ।
[विशेष वचन ]
१. “उतोऽयुरुनुस्नु०” इति प्रतिषेधे वचनम् (दु० टी०)।
२. आत्मनेपदे तु धुञ धूञा च रूपद्वयम् - अधोष्ट अधविष्ट (दु० टी०)।
३. केषांचिद् अधौषीदिति मतं चिन्त्यम् (दु० टी०)।
४. शर्ववर्मणा धूञः पाठस्तत्रानादृत एव तेनास्मादपि नित्यमिडागमः (वि० प० ) । [रूपसिद्धि]
+
१. प्रास्तावीत्। प्र + अट् + स्तु दि। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'ष्टुञ् स्तुतौ' (२।६५ ) धातु से अद्यतनीसंज्ञक ‘दि’ प्रत्यय, “अड् धात्वादिर्ह्यस्तन्यद्यतनीक्रियातिपत्तिषु” (३।८।१६) से धातुपूर्व अडागम, सिच् प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से इडागम, “सिचि परस्मै स्वरान्तानाम्” (३।६।६ ) से धातुघटित उकार को वृद्धि, " औ आव्' (१।२।१५) से 'औ' को 'आव्' आदेश, “सिचः” (३।६।९०) से ईडागम, “इटश्चेटि" (३।६।५३) से सिच्प्रत्यय का लोप, समानदीर्घ तथा दकार को तकारादेश ।
२. प्रासावीत् । प्र + अट् + सु + दि। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'षु अभिषवे' (४।१ ) धातु से अद्यतनीसंज्ञक 'दि' प्रत्यय तथा शेष प्रक्रिया पूर्ववत् ।
३. प्राधावीत् । प्र + अट् + धू + दि। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'धूञ् कम्पने' (८।१३) धातु से अद्यतनीसंज्ञक 'दि' प्रत्यय तथा अन्य प्रक्रिया पूर्ववत् ॥७९१ । ७९२. यमिरमिनम्यादन्तानां सिरन्तश्च [ ३।७।१०] [सूत्रार्थ]
परस्मैपद में 'सिच्' प्रत्यय के परे रहते 'यम् - रम् - नम्' तथा आकारान्त धातुओं से उत्तर इडागम तथा धातुओं के अन्त में सकार ( आगम) होता है ।।७९२ ।