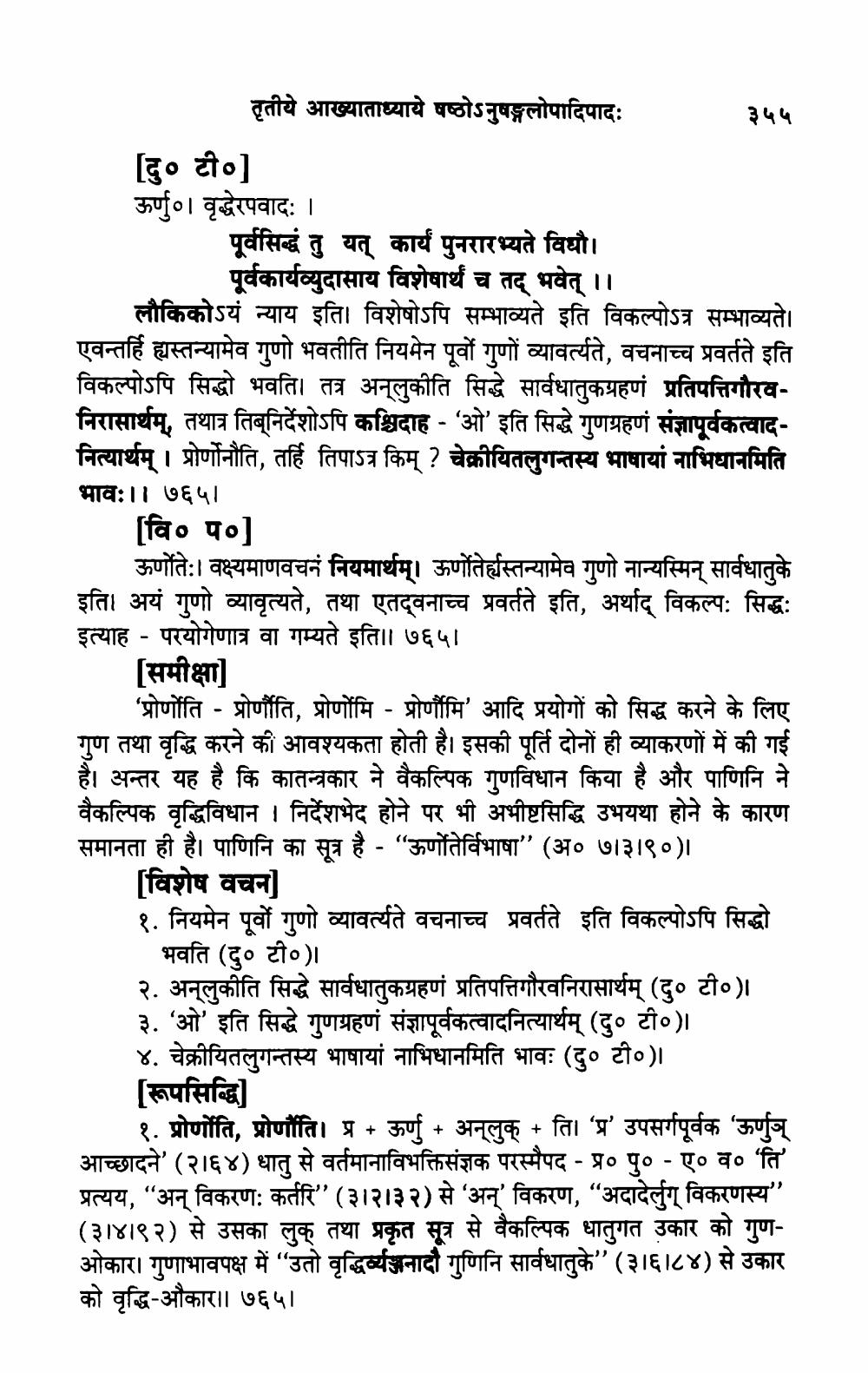________________
तृतीये आख्याताध्याये षष्ठोऽनुषङ्गलोपादिपादः
३५५ [दु० टी०] ऊर्गु०। वृद्धेरपवादः ।
पूर्वसिद्धं तु यत् कार्यं पुनरारभ्यते विधौ।
पूर्वकार्यव्युदासाय विशेषार्थं च तद् भवेत् ।। लौकिकोऽयं न्याय इति। विशेषोऽपि सम्भाव्यते इति विकल्पोऽत्र सम्भाव्यते। एवन्तर्हि ह्यस्तन्यामेव गुणो भवतीति नियमेन पूर्वो गुणों व्यावय॑ते, वचनाच्च प्रवर्तते इति विकल्पोऽपि सिद्धो भवति। तत्र अन्लुकीति सिद्धे सार्वधातुकग्रहणं प्रतिपत्तिगौरवनिरासार्थम्, तथात्र तिग्निर्देशोऽपि कश्चिदाह - 'ओ' इति सिद्धे गुणग्रहणं संज्ञापूर्वकत्वादनित्यार्थम् । प्रोर्णोनौति, तर्हि तिपाऽत्र किम् ? चेक्रीयितलुगन्तस्य भाषायां नाभिधानमिति भावः।। ७६५।
[वि० प०]
ऊणोंतेः। वक्ष्यमाणवचनं नियमार्थम्। ऊणोंतेीस्तन्यामेव गुणो नान्यस्मिन् सार्वधातुके इति। अयं गुणो व्यावृत्यते, तथा एतद्वनाच्च प्रवर्तते इति, अर्थाद् विकल्प: सिद्धः इत्याह - परयोगेणात्र वा गम्यते इति।। ७६५।
[समीक्षा]
'प्रोणोंति - प्रोणीति, प्रोणोमि - प्रो#मि' आदि प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए गुण तथा वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। इसकी पूर्ति दोनों ही व्याकरणों में की गई है। अन्तर यह है कि कातन्त्रकार ने वैकल्पिक गुणविधान किया है और पाणिनि ने वैकल्पिक वृद्धिविधान । निर्देशभेद होने पर भी अभीष्टसिद्धि उभयथा होने के कारण समानता ही है। पाणिनि का सूत्र है - "ऊर्णोतेर्विभाषा" (अ० ७।३।९०)।
[विशेष वचन) १. नियमेन पूर्वो गुणो व्यावय॑ते वचनाच्च प्रवर्तते इति विकल्पोऽपि सिद्धो
भवति (दु० टी०)। २. अन्लुकीति सिद्धे सार्वधातुकग्रहणं प्रतिपत्तिगौरवनिरासार्थम् (दु० टी०)। ३. 'ओ' इति सिद्धे गुणग्रहणं संज्ञापूर्वकत्वादनित्यार्थम् (दु० टी०)। ४. चेक्रीयितलुगन्तस्य भाषायां नाभिधानमिति भावः (दु० टी०)। [रूपसिद्धि
१. प्रोर्णोति, प्रोणौति। प्र + ऊर्गु + अन्लुक् + ति। 'प्र' उपसर्गपूर्वक 'ऊर्गुब् आच्छादने' (२१६४) धातु से वर्तमानाविभक्तिसंज्ञक परस्मैपद - प्र० पु० - ए० व० 'ति' प्रत्यय, “अन् विकरणः कर्तरि" (३।२।३२) से 'अन्' विकरण, “अदादेलुंग विकरणस्य" (३।४।९२) से उसका लुक् तथा प्रकृत सूत्र से वैकल्पिक धातुगत उकार को गुण
ओकार। गुणाभावपक्ष में "उतो वृद्धिर्व्यञ्जनादौ गुणिनि सार्वधातुके” (३।६।८४) से उकार को वृद्धि-औकार।। ७६५।