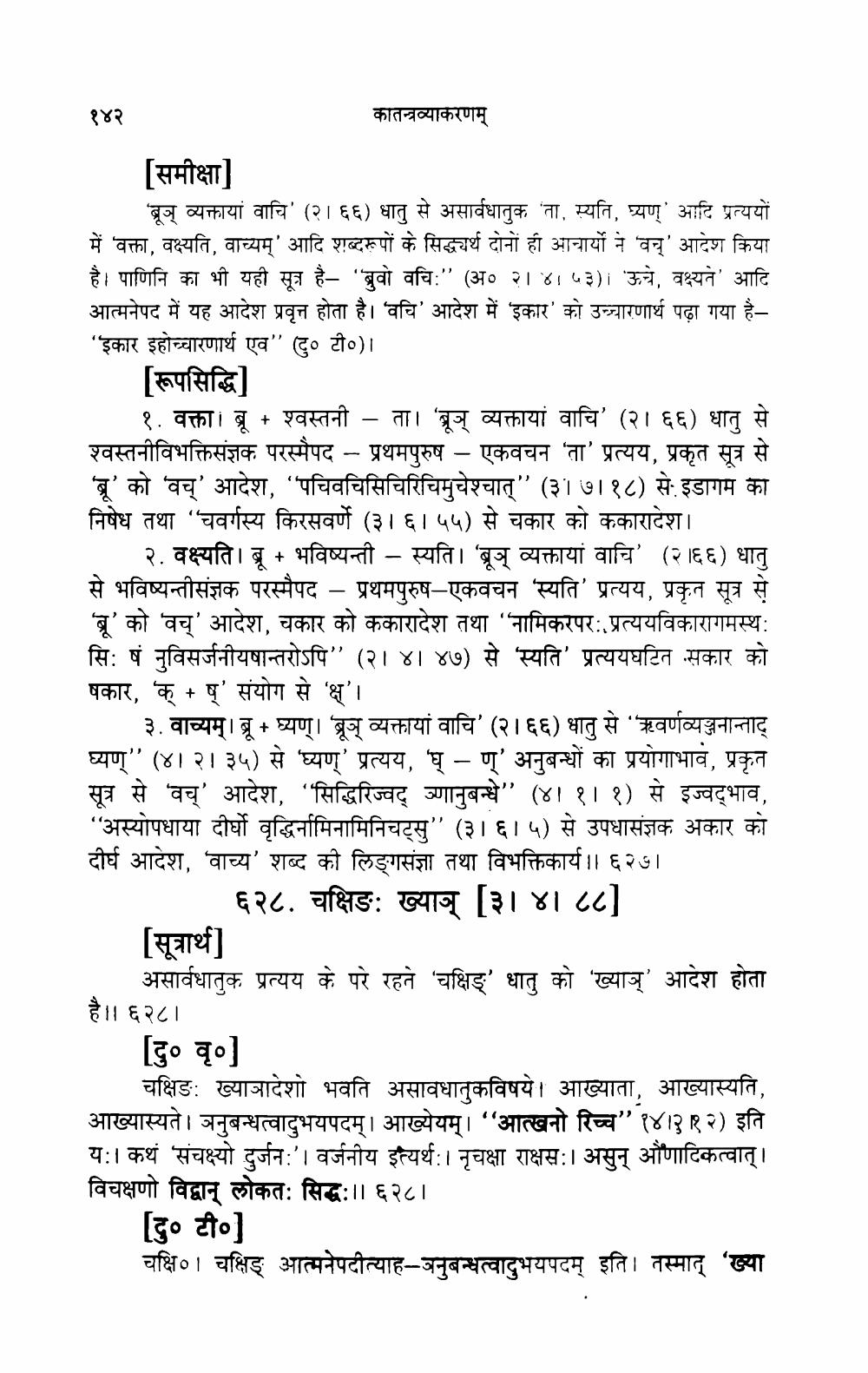________________
१४२
कातन्त्रव्याकरणम्
[समीक्षा
'ब्रू व्यक्तायां वाचि' (२ । ६६) धातु से असार्वधातुक 'ता. स्यति, घ्यण' आदि प्रत्ययों में वक्ता, वक्ष्यति, वाच्यम्' आदि शब्दरूपों के सिद्धयर्थ दोनों ही आचार्यों ने 'वच्' आदेश किया है। पाणिनि का भी यही सूत्र है- "ब्रुवो वचिः'' (अ० २। ४। ५३)। ऊचे, वक्ष्यते' आदि आत्मनेपद में यह आदेश प्रवृत्त होता है। 'वचि' आदेश में 'इकार' को उच्चारणार्थ पढ़ा गया है"इकार इहोच्चारणार्थ एव'' (टु० टी०)।
[रूपसिद्धि]
१. वक्ता। ब्रू + श्वस्तनी – ता। ‘ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि' (२। ६६) धातु से श्वस्तनीविभक्तिसंज्ञक परस्मैपद - प्रथमपुरुष – एकवचन 'ता' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से 'ब्रू' को 'वच्' आदेश, “पचिवचिसिचिरिचिमुचेश्चात्'' (३। ७। १८) से: इडागम का निषेध तथा “चवर्गस्य किरसवर्णे (३।६। ५५) से चकार को ककारादेश।
२. वक्ष्यति। ब्रू + भविष्यन्ती – स्यति। 'ब्रूञ् व्यक्तायां वाचि' (२६६) धातु से भविष्यन्तीसंज्ञक परस्मैपद – प्रथमपुरुष–एकवचन ‘स्यति' प्रत्यय, प्रकृत सूत्र से 'ब्रू' को 'वच्' आदेश, चकार को ककारादेश तथा “नामिकरपरः प्रत्ययविकारागमस्थ: सि: षं नुविसर्जनीयषान्तरोऽपि' (२। ४। ४७) से 'स्यति' प्रत्ययघटित सकार को षकार, 'क् + प्' संयोग से 'क्ष'।
३. वाच्यम्। ब्रू + घ्यण। 'ब्रू व्यक्तायां वाचि' (२। ६६) धातु से "ऋवर्णव्यञ्जनान्ताद् घ्यण्' (४। २। ३५) से 'घ्यण' प्रत्यय, 'घ – ण' अनुबन्धों का प्रयोगाभाव, प्रकृत सूत्र से 'वच्' आदेश, “सिद्धिरिज्वद् ज्णानुबन्धे" (४। १। १) से इज्वद्भाव, "अस्योपधाया दीर्घो वृद्धि मिनामिनिचट्सु' (३।६। ५) से उपधासंज्ञक अकार को दीर्घ आदेश, 'वाच्य' शब्द की लिङ्गसंज्ञा तथा विभक्तिकार्य।। ६२७ ।
६२८. चक्षिङः ख्याञ् [३। ४। ८८] [सूत्रार्थ] असार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते 'चक्षिङ्' धातु को 'ख्याञ्' आदेश होता
है।। ६२८।
[दु० वृ०]
चक्षिङः ख्याादेशो भवति असावधातकविषये। आख्याता, आख्यास्यति, आख्यास्यते। अनुबन्धत्वादुभयपदम्। आख्येयम्। “आत्खनो रिच्च" १४।२ १२) इति यः। कथं संचक्ष्यो दुर्जन:'। वर्जनीय इत्यर्थः। नृचक्षा राक्षसः। असुन औणादिकत्वात्। विचक्षणो विद्वान् लोकत: सिद्धः।। ६२८ ।
[दु० टी०] चक्षि०। चक्षिङ् आत्मनेपदीत्याह-अनुबन्धत्वादुभयपदम् इति। तस्मात् ‘ख्या