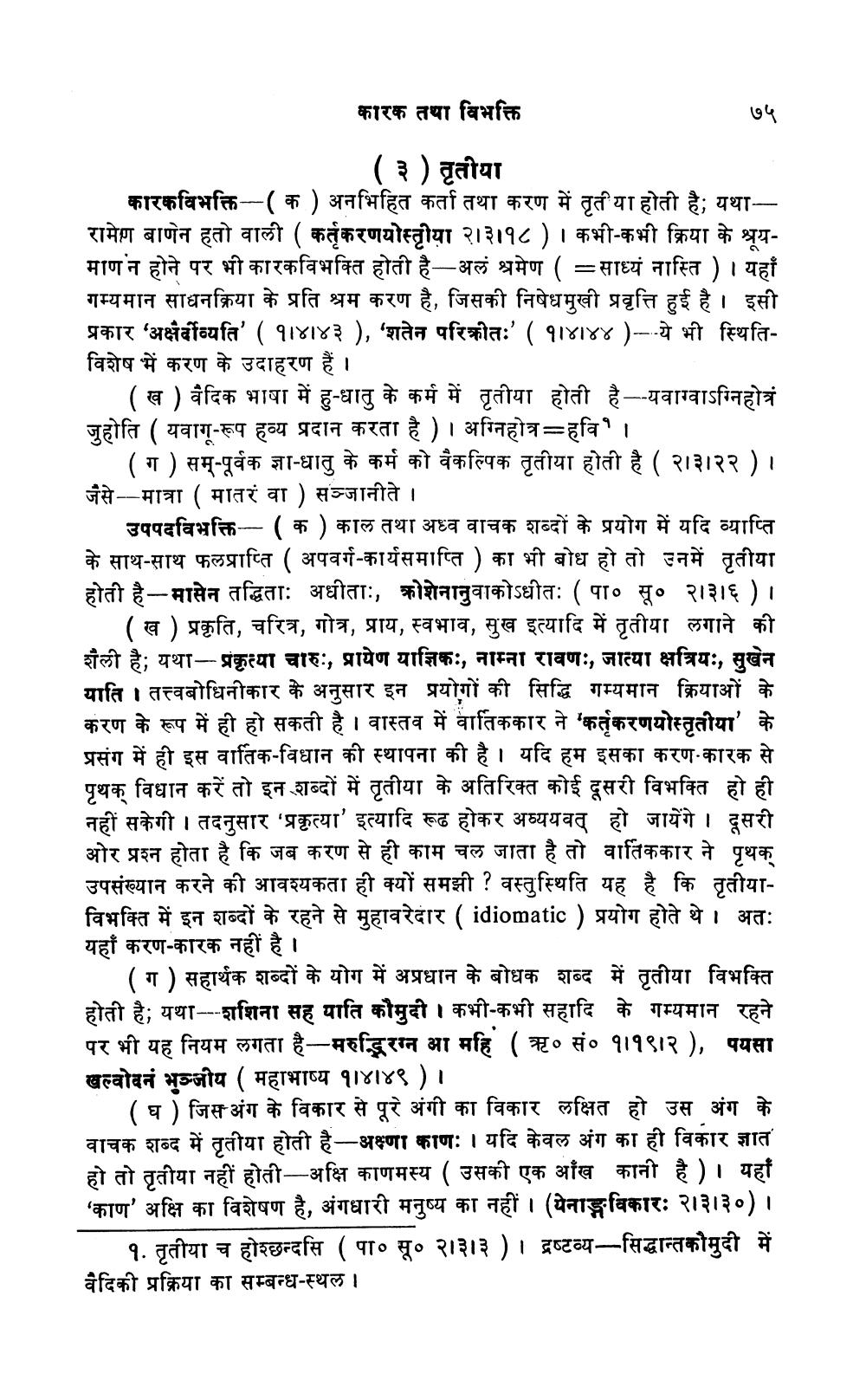________________
कारक तथा विभक्ति
(३) तृतीया कारकविभक्ति-( क ) अनभिहित कर्ता तथा करण में तृतीया होती है; यथारामेण बाणेन हतो वाली ( कर्तृकरणयोस्तृीया २।३।१८ ) । कभी-कभी क्रिया के श्रूयमाण न होने पर भी कारकविभक्ति होती है-अलं श्रमेण ( = साध्यं नास्ति ) । यहाँ गम्यमान साधनक्रिया के प्रति श्रम करण है, जिसकी निषेधमुखी प्रवृत्ति हुई है। इसी प्रकार 'अक्षर्दीव्यति' ( १।४।४३ ), 'शतेन परिक्रीतः' ( १।४।४४ )-.ये भी स्थितिविशेष में करण के उदाहरण हैं ।
(ख ) वैदिक भाषा में हु-धातु के कर्म में तृतीया होती है--यवाग्वाऽग्निहोत्रं जुहोति ( यवागू-रूप हव्य प्रदान करता है ) । अग्निहोत्र=हवि ।।
(ग ) सम्-पूर्वक ज्ञा-धातु के कर्म को वैकल्पिक तृतीया होती है ( २।३।२२ )। जैसे--मात्रा ( मातरं वा ) सञ्जानीते ।
उपपदविभक्ति- ( क ) काल तथा अध्व वाचक शब्दों के प्रयोग में यदि व्याप्ति के साथ-साथ फलप्राप्ति ( अपवर्ग-कार्यसमाप्ति ) का भी बोध हो तो उनमें तृतीया होती है-मासेन तद्धिताः अधीताः, क्रोशेनानुवाकोऽधीतः ( पा० सू० २।३।६ ) ।
(ख ) प्रकृति, चरित्र, गोत्र, प्राय, स्वभाव, सुख इत्यादि में तृतीया लगाने की शैली है; यथा-प्रकृत्या चारुः, प्रायेण याज्ञिकः, नाम्ना रावणः, जात्या क्षत्रियः, सुखेन याति । तत्त्वबोधिनीकार के अनुसार इन प्रयोगों की सिद्धि गम्यमान क्रियाओं के करण के रूप में ही हो सकती है । वास्तव में वार्तिककार ने 'कर्तृकरणयोस्तृतीया' के प्रसंग में ही इस वार्तिक-विधान की स्थापना की है। यदि हम इसका करण कारक से पृथक् विधान करें तो इन शब्दों में तृतीया के अतिरिक्त कोई दूसरी विभक्ति हो ही नहीं सकेगी। तदनुसार 'प्रकृत्या' इत्यादि रूढ होकर अव्ययवत् हो जायेंगे। दूसरी ओर प्रश्न होता है कि जब करण से ही काम चल जाता है तो वार्तिककार ने पृथक उपसंख्यान करने की आवश्यकता ही क्यों समझी ? वस्तुस्थिति यह है कि तृतीयाविभक्ति में इन शब्दों के रहने से मुहावरेदार ( idiomatic ) प्रयोग होते थे। अतः यहाँ करण-कारक नहीं है।
(ग ) सहार्थक शब्दों के योग में अप्रधान के बोधक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है; यथा---शशिना सह याति कौमुदी। कभी-कभी सहादि के गम्यमान रहने पर भी यह नियम लगता है-मरुद्भिरग्न आ महि ( ऋ० सं० १।१९।२ ), पयसा खल्वोवनं भुजीय ( महाभाष्य १।४।४९ )।
(घ) जिस अंग के विकार से पूरे अंगी का विकार लक्षित हो उस अंग के वाचक शब्द में तृतीया होती है-अक्षणा काणः । यदि केवल अंग का ही विकार ज्ञात हो तो तृतीया नहीं होती–अक्षि काणमस्य ( उसकी एक आँख कानी है)। यहाँ 'काण' अक्षि का विशेषण है, अंगधारी मनुष्य का नहीं । (येनाङ्गविकारः २।३।३०) ।
१. तृतीया च होश्छन्दसि ( पा० सू० २।३।३ )। द्रष्टव्य-सिद्धान्तकौमुदी में वैदिकी प्रक्रिया का सम्बन्ध-स्थल ।