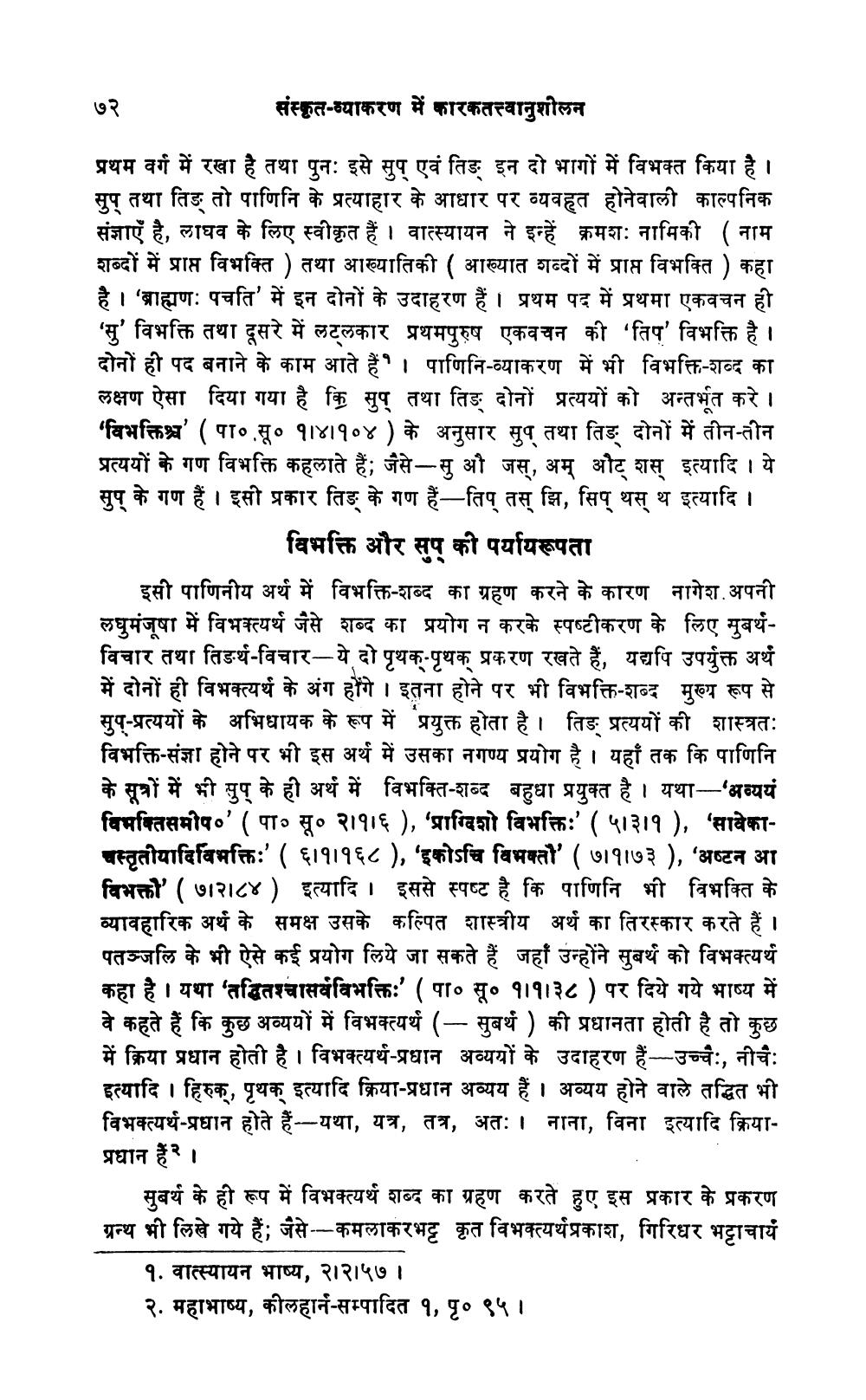________________
संस्कृत - व्याकरण में कारकतत्वानुशीलन
प्रथम वर्ग में रखा है तथा पुनः इसे सुप् एवं तिङ् इन दो भागों में विभक्त किया है । सुप् तथा तिङ् तो पाणिनि के प्रत्याहार के आधार पर व्यवहृत होनेवाली काल्पनिक संज्ञाएँ है, लाघव के लिए स्वीकृत हैं । वात्स्यायन ने इन्हें क्रमशः नामिकी ( नाम शब्दों में प्राप्त विभक्ति ) तथा आख्यातिकी ( आख्यात शब्दों में प्राप्त विभक्ति ) कहा है । 'ब्राह्मणः पचति' में इन दोनों के उदाहरण हैं । प्रथम पद में प्रथमा एकवचन ही 'सु' विभक्ति तथा दूसरे में लट्लकार प्रथमपुरुष एकवचन की 'तिप' विभक्ति है । दोनों ही पद बनाने के काम आते हैं । पाणिनि व्याकरण में भी विभक्ति-शब्द का लक्षण ऐसा दिया गया है कि सुप् तथा तिङ् दोनों प्रत्ययों को अन्तर्भूत करे । 'विभक्तिश्च' ( पा० सू० १|४|१०४ ) के अनुसार सुप् तथा तिङ् दोनों में तीन-तीन प्रत्ययों के गण विभक्ति कहलाते हैं; जैसे- सु औ जस्, अम् औट् शस् इत्यादि । ये सुप् के गण हैं । इसी प्रकार तिङ् के गण हैं - तिप् तस् झि, सिप् थस् थ इत्यादि । विभक्ति और सुप् की पर्यायरूपता
७२
इस पाणिनीय अर्थ में विभक्ति-शब्द का ग्रहण करने के कारण नागेश अपनी लघुमंजूषा में विभक्त्यर्थ जैसे शब्द का प्रयोग न करके स्पष्टीकरण के लिए सुबर्थविचार तथा तिङर्थ- विचार - ये दो पृथक्-पृथक् प्रकरण रखते हैं, यद्यपि उपर्युक्त अर्थ में दोनों ही विभक्त्यर्थ के अंग होंगे। इतना होने पर भी विभक्ति-शब्द मुख्य रूप से सुप्-प्रत्ययों के अभिधायक के रूप में प्रयुक्त होता है । तिङ् प्रत्ययों की शास्त्रतः विभक्ति -संज्ञा होने पर भी इस अर्थ में उसका नगण्य प्रयोग है । यहाँ तक कि पाणिनि सूत्रों में भी सुप् केही अर्थ में विभक्ति-शब्द बहुधा प्रयुक्त है । यथा - ' अव्ययं विभक्तिसमीप ० ' ( पा० सू० २।१।६), 'प्राग्दिशो विभक्ति:' ( ५1३1१ ), 'सावेकाचस्तृतीयादिविभक्ति:' ( ६।१।१६८), 'इकोऽचि विभक्तौ ' ( ७।१1७३), 'अष्टन आ विभक्तौ' ( ७|२|८४ ) इत्यादि । इससे स्पष्ट है कि पाणिनि भी विभक्ति के व्यावहारिक अर्थ के समक्ष उसके कल्पित शास्त्रीय अर्थ का तिरस्कार करते हैं । पतञ्जलि के भी ऐसे कई प्रयोग लिये जा सकते हैं जहाँ उन्होंने सुबर्थ को विभक्त्यर्थ कहा है । यथा 'तद्धितश्चासर्वविभक्तिः' ( पा० सू० १।१।३८ ) पर दिये गये भाष्य में वे कहते हैं कि कुछ अव्ययों में विभक्त्यर्थ ( - सुबर्थ ) की प्रधानता होती है तो कुछ में क्रिया प्रधान होती है । विभक्त्यर्थ प्रधान अव्ययों के उदाहरण हैं --- उच्चैः, नीचः इत्यादि । हिरुक् पृथक् इत्यादि क्रिया-प्रधान अव्यय हैं । अव्यय होने वाले तद्धित भी विभक्त्यर्थ प्रधान होते हैं - यथा, यत्र, तत्र, अत: । नाना, विना इत्यादि क्रियाप्रधान हैं ।
सुबर्थ के ही रूप में विभक्त्यर्थ शब्द का ग्रहण करते हुए इस प्रकार के प्रकरण ग्रन्थ भी लिखे गये हैं; जैसे - कमलाकरभट्ट कृत विभक्त्यर्थ प्रकाश, गिरिधर भट्टाचार्य
१. वात्स्यायन भाष्य, २।२।५७ ।
२. महाभाष्य, कीलहान-सम्पादित १, पृ० ९५ ।