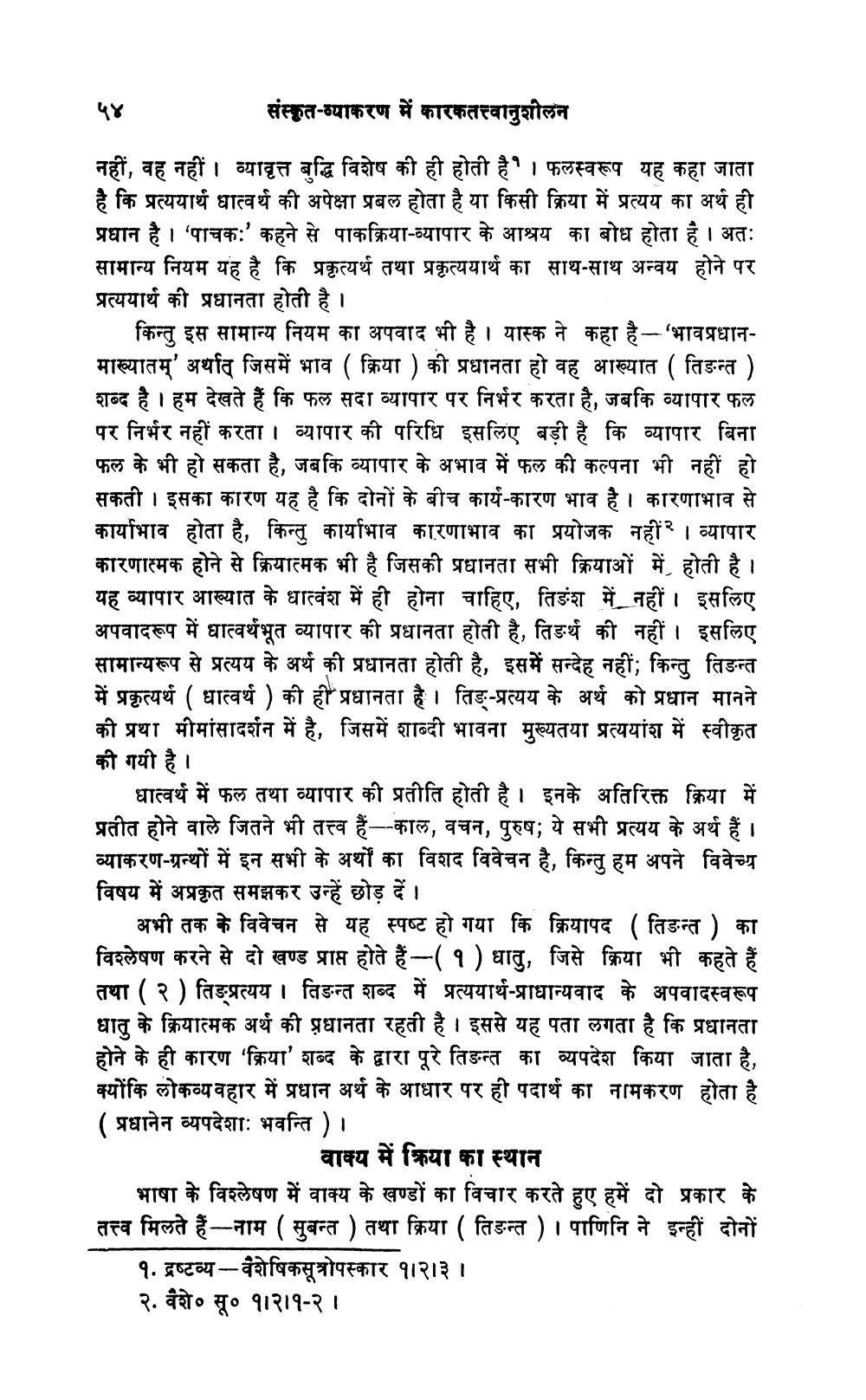________________
५४
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन
नहीं, वह नहीं। व्यावृत्त बुद्धि विशेष की ही होती है । फलस्वरूप यह कहा जाता है कि प्रत्ययार्थ धात्वर्थ की अपेक्षा प्रबल होता है या किसी क्रिया में प्रत्यय का अर्थ ही प्रधान है । 'पाचकः' कहने से पाकक्रिया-व्यापार के आश्रय का बोध होता है । अतः सामान्य नियम यह है कि प्रकृत्यर्थ तथा प्रकृत्ययार्थ का साथ-साथ अन्वय होने पर प्रत्ययार्थ की प्रधानता होती है ।
किन्तु इस सामान्य नियम का अपवाद भी है। यास्क ने कहा है- 'भावप्रधानमाख्यातम्' अर्थात् जिसमें भाव ( क्रिया ) की प्रधानता हो वह आख्यात ( तिङन्त ) शब्द है। हम देखते हैं कि फल सदा व्यापार पर निर्भर करता है, जबकि व्यापार फल पर निर्भर नहीं करता। व्यापार की परिधि इसलिए बड़ी है कि व्यापार बिना फल के भी हो सकता है, जबकि व्यापार के अभाव में फल की कल्पना भी नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि दोनों के बीच कार्य-कारण भाव है। कारणाभाव से कार्याभाव होता है, किन्तु कार्याभाव कारणाभाव का प्रयोजक नहीं२ । व्यापार कारणात्मक होने से क्रियात्मक भी है जिसकी प्रधानता सभी क्रियाओं में होती है। यह व्यापार आख्यात के धात्वंश में ही होना चाहिए, तिडंश में नहीं। इसलिए अपवादरूप में धात्वर्थभूत व्यापार की प्रधानता होती है, तिङर्थ की नहीं। इसलिए सामान्यरूप से प्रत्यय के अर्थ की प्रधानता होती है, इसमें सन्देह नहीं; किन्तु तिङन्त में प्रकृत्यर्थ ( धात्वर्थ ) की ही प्रधानता है। तिङ्-प्रत्यय के अर्थ को प्रधान मानने की प्रथा मीमांसादर्शन में है, जिसमें शाब्दी भावना मुख्यतया प्रत्ययांश में स्वीकृत की गयी है।
धात्वर्थ में फल तथा व्यापार की प्रतीति होती है। इनके अतिरिक्त क्रिया में प्रतीत होने वाले जितने भी तत्त्व हैं--काल, वचन, पुरुष; ये सभी प्रत्यय के अर्थ हैं। व्याकरण-ग्रन्थों में इन सभी के अर्थों का विशद विवेचन है, किन्तु हम अपने विवेच्य विषय में अप्रकृत समझकर उन्हें छोड़ दें।
अभी तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि क्रियापद (तिङन्त ) का विश्लेषण करने से दो खण्ड प्राप्त होते हैं-(१) धातु, जिसे क्रिया भी कहते हैं तथा ( २ ) तिप्रत्यय । तिङन्त शब्द में प्रत्ययार्थ-प्राधान्यवाद के अपवादस्वरूप धातु के क्रियात्मक अर्थ की प्रधानता रहती है। इससे यह पता लगता है कि प्रधानता होने के ही कारण 'क्रिया' शब्द के द्वारा पूरे तिङन्त का व्यपदेश किया जाता है, क्योंकि लोकव्यवहार में प्रधान अर्थ के आधार पर ही पदार्थ का नामकरण होता है (प्रधानेन व्यपदेशाः भवन्ति )।
वाक्य में क्रिया का स्थान भाषा के विश्लेषण में वाक्य के खण्डों का विचार करते हुए हमें दो प्रकार के तत्त्व मिलते हैं-नाम ( सुबन्त ) तथा क्रिया ( तिङन्त ) । पाणिनि ने इन्हीं दोनों
१. द्रष्टव्य-वैशेषिकसूत्रोपस्कार १।२।३ । २. वैशे० सू० १।२।१-२ ।