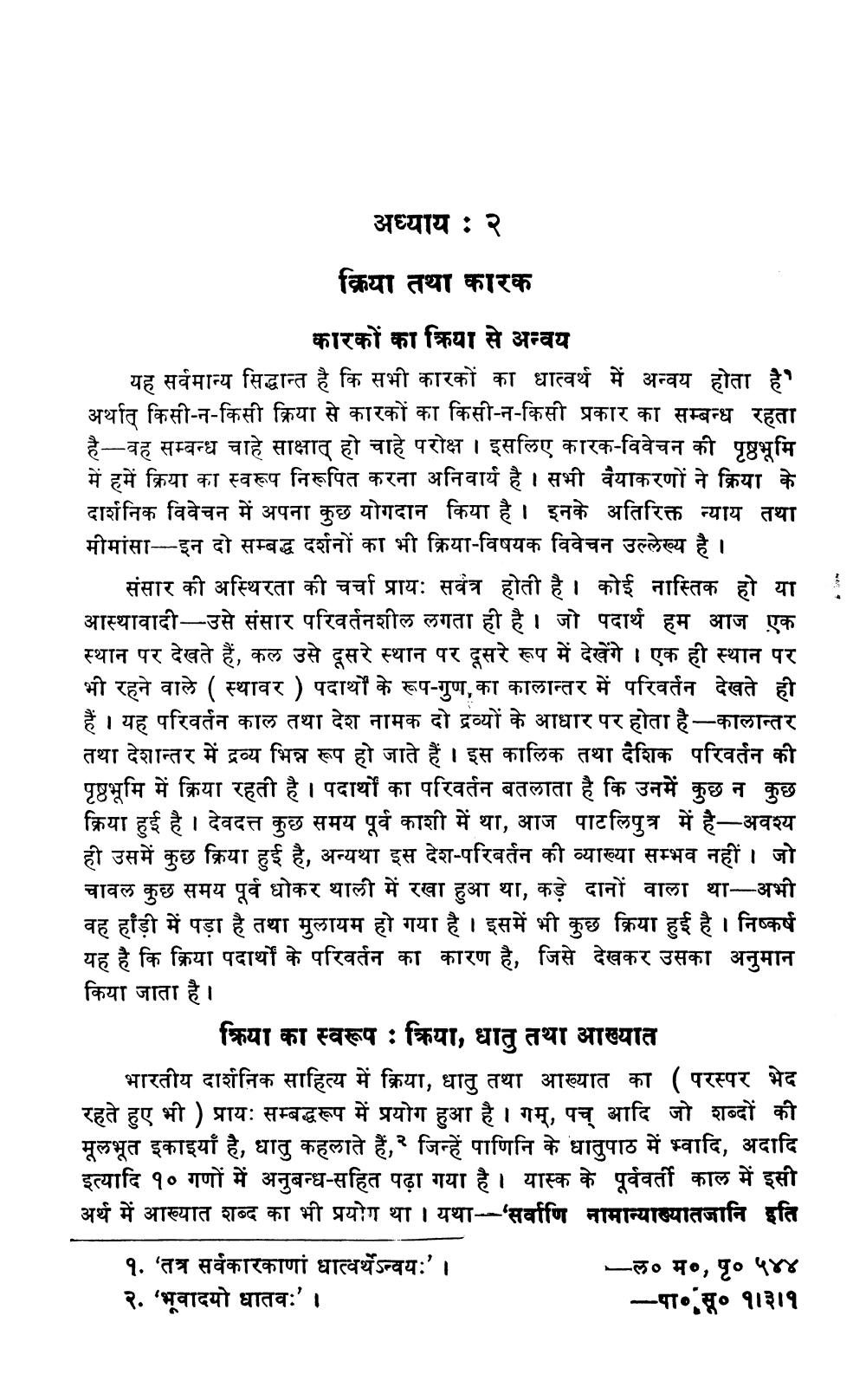________________
अध्याय : २
किया तथा कारक
कारकों का क्रिया से अन्वय यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि सभी कारकों का धात्वर्थ में अन्वय होता है। अर्थात् किसी-न-किसी क्रिया से कारकों का किसी-न-किसी प्रकार का सम्बन्ध रहता है-वह सम्बन्ध चाहे साक्षात् हो चाहे परोक्ष । इसलिए कारक-विवेचन की पृष्ठभूमि में हमें क्रिया का स्वरूप निरूपित करना अनिवार्य है। सभी वैयाकरणों ने क्रिया के दार्शनिक विवेचन में अपना कुछ योगदान किया है। इनके अतिरिक्त न्याय तथा मीमांसा-इन दो सम्बद्ध दर्शनों का भी क्रिया-विषयक विवेचन उल्लेख्य है।
संसार की अस्थिरता की चर्चा प्रायः सर्वत्र होती है। कोई नास्तिक हो या आस्थावादी-उसे संसार परिवर्तनशील लगता ही है। जो पदार्थ हम आज एक स्थान पर देखते हैं, कल उसे दूसरे स्थान पर दूसरे रूप में देखेंगे । एक ही स्थान पर भी रहने वाले ( स्थावर ) पदार्थों के रूप-गुण,का कालान्तर में परिवर्तन देखते ही हैं । यह परिवर्तन काल तथा देश नामक दो द्रव्यों के आधार पर होता है-कालान्तर तथा देशान्तर में द्रव्य भिन्न रूप हो जाते हैं । इस कालिक तथा दैशिक परिवर्तन की पृष्ठभूमि में क्रिया रहती है । पदार्थों का परिवर्तन बतलाता है कि उनमें कुछ न कुछ क्रिया हुई है । देवदत्त कुछ समय पूर्व काशी में था, आज पाटलिपुत्र में है-अवश्य ही उसमें कुछ क्रिया हुई है, अन्यथा इस देश-परिबर्तन की व्याख्या सम्भव नहीं। जो चावल कुछ समय पूर्व धोकर थाली में रखा हुआ था, कड़े दानों वाला था-अभी वह हांड़ी में पड़ा है तथा मुलायम हो गया है । इसमें भी कुछ क्रिया हुई है। निष्कर्ष यह है कि क्रिया पदार्थों के परिवर्तन का कारण है, जिसे देखकर उसका अनुमान किया जाता है।
क्रिया का स्वरूप : क्रिया, धातु तथा आख्यात भारतीय दार्शनिक साहित्य में क्रिया, धातु तथा आख्यात का ( परस्पर भेद रहते हुए भी ) प्रायः सम्बद्धरूप में प्रयोग हुआ है । गम्, पच् आदि जो शब्दों की मूलभूत इकाइयाँ है, धातु कहलाते हैं, जिन्हें पाणिनि के धातुपाठ में भ्वादि, अदादि इत्यादि १० गणों में अनुबन्ध-सहित पढ़ा गया है। यास्क के पूर्ववर्ती काल में इसी अर्थ में आख्यात शब्द का भी प्रयोग था । यथा--'सर्वाणि नामान्याख्यातजानि इति १. 'तत्र सर्वकारकाणां धात्वर्थेऽन्वयः' ।
-ल० म०, पृ० ५४४ २. 'भूवादयो धातवः' ।
-पासू० १।३।१