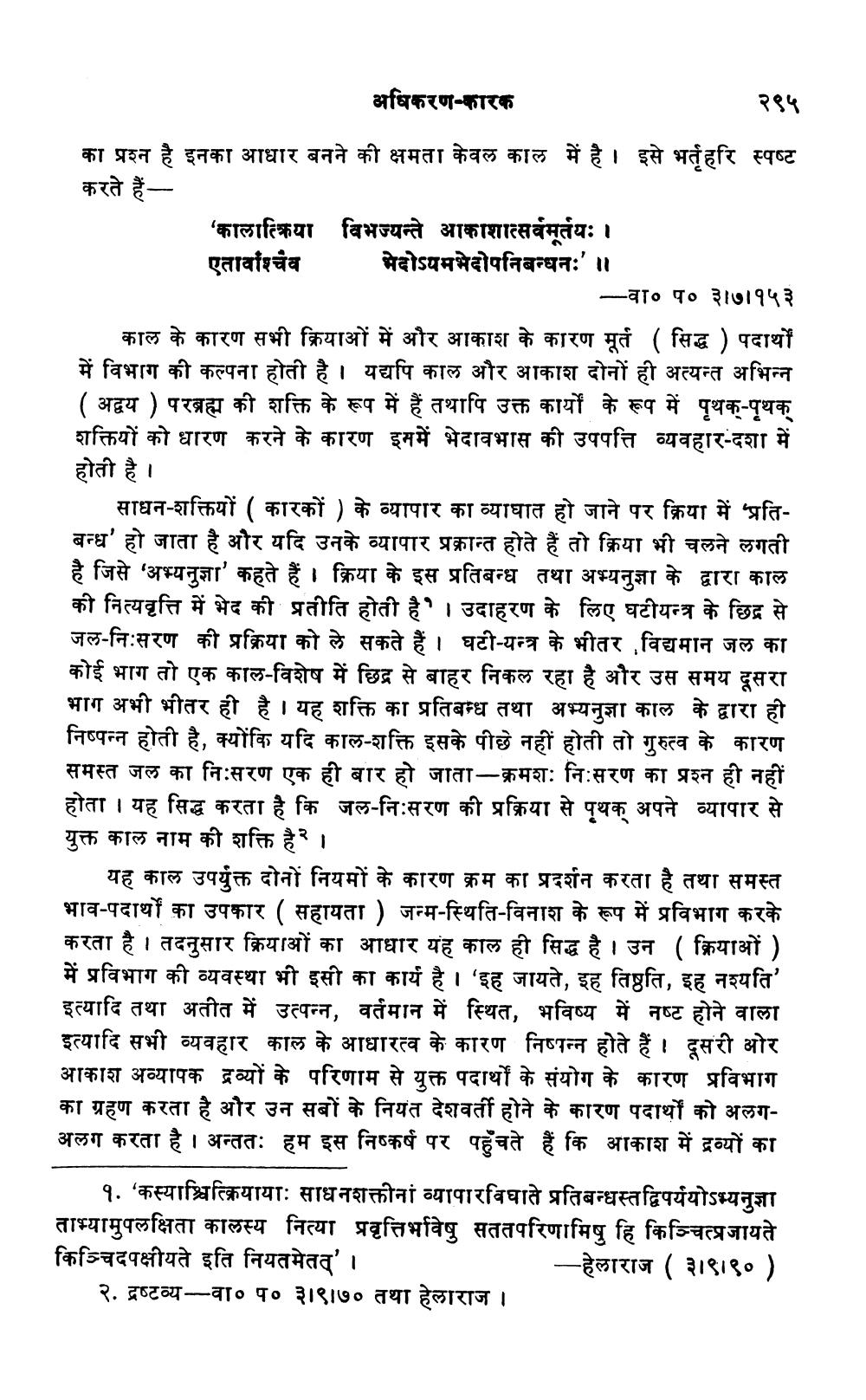________________
अधिकरण-कारक
२९५ का प्रश्न है इनका आधार बनने की क्षमता केवल काल में है। इसे भर्तृहरि स्पष्ट करते हैं
'कालाक्रिया विभज्यन्ते आकाशात्सर्वमूर्तयः । एतावांश्चैव भेदोऽयमभेदोपनिबन्धनः ॥
-वा० प० ३।७।१५३ काल के कारण सभी क्रियाओं में और आकाश के कारण मूर्त ( सिद्ध ) पदार्थों में विभाग की कल्पना होती है। यद्यपि काल और आकाश दोनों ही अत्यन्त अभिन्न ( अद्वय ) परब्रह्म की शक्ति के रूप में हैं तथापि उक्त कार्यों के रूप में पृथक्-पृथक शक्तियों को धारण करने के कारण इममें भेदावभास की उपपत्ति व्यवहार-दशा में होती है।
__ साधन-शक्तियों ( कारकों ) के व्यापार का व्याघात हो जाने पर क्रिया में 'प्रतिबन्ध' हो जाता है और यदि उनके व्यापार प्रक्रान्त होते हैं तो क्रिया भी चलने लगती है जिसे 'अभ्यनुज्ञा' कहते हैं। क्रिया के इस प्रतिबन्ध तथा अभ्यनुज्ञा के द्वारा काल की नित्यवृत्ति में भेद की प्रतीति होती है । उदाहरण के लिए घटीयन्त्र के छिद्र से जल-निःसरण की प्रक्रिया को ले सकते हैं। घटी-यन्त्र के भीतर विद्यमान जल का कोई भाग तो एक काल-विशेष में छिद्र से बाहर निकल रहा है और उस समय दूसरा भाग अभी भीतर ही है । यह शक्ति का प्रतिबन्ध तथा अभ्यनुज्ञा काल के द्वारा ही निष्पन्न होती है, क्योंकि यदि काल-शक्ति इसके पीछे नहीं होती तो गुरुत्व के कारण समस्त जल का निःसरण एक ही बार हो जाता-क्रमशः निःसरण का प्रश्न ही नहीं होता । यह सिद्ध करता है कि जल-निःसरण की प्रक्रिया से पृथक् अपने व्यापार से युक्त काल नाम की शक्ति है । __ यह काल उपर्युक्त दोनों नियमों के कारण क्रम का प्रदर्शन करता है तथा समस्त भाव-पदार्थों का उपकार ( सहायता ) जन्म-स्थिति-विनाश के रूप में प्रविभाग करके करता है । तदनुसार क्रियाओं का आधार यह काल ही सिद्ध है । उन ( क्रियाओं) में प्रविभाग की व्यवस्था भी इसी का कार्य है। 'इह जायते, इह तिष्ठति, इह नश्यति' इत्यादि तथा अतीत में उत्पन्न, वर्तमान में स्थित, भविष्य में नष्ट होने वाला इत्यादि सभी व्यवहार काल के आधारत्व के कारण निष्पन्न होते हैं। दूसरी ओर आकाश अव्यापक द्रव्यों के परिणाम से युक्त पदार्थों के संयोग के कारण प्रविभाग का ग्रहण करता है और उन सबों के नियत देशवर्ती होने के कारण पदार्थों को अलगअलग करता है । अन्ततः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आकाश में द्रव्यों का
१. 'कस्याश्चिक्रियायाः साधनशक्तीनां व्यापारविघाते प्रतिबन्धस्तद्विपर्ययोऽभ्यनुज्ञा ताभ्यामुपलक्षिता कालस्य नित्या प्रवृत्तिर्भावेषु सततपरिणामिषु हि किञ्चित्प्रजायते किञ्चिदपक्षीयते इति नियतमेतत्' ।
–हेलाराज ( ३।९।९०) २. द्रष्टव्य-वा०प० ३।९।७० तथा हेलाराज।