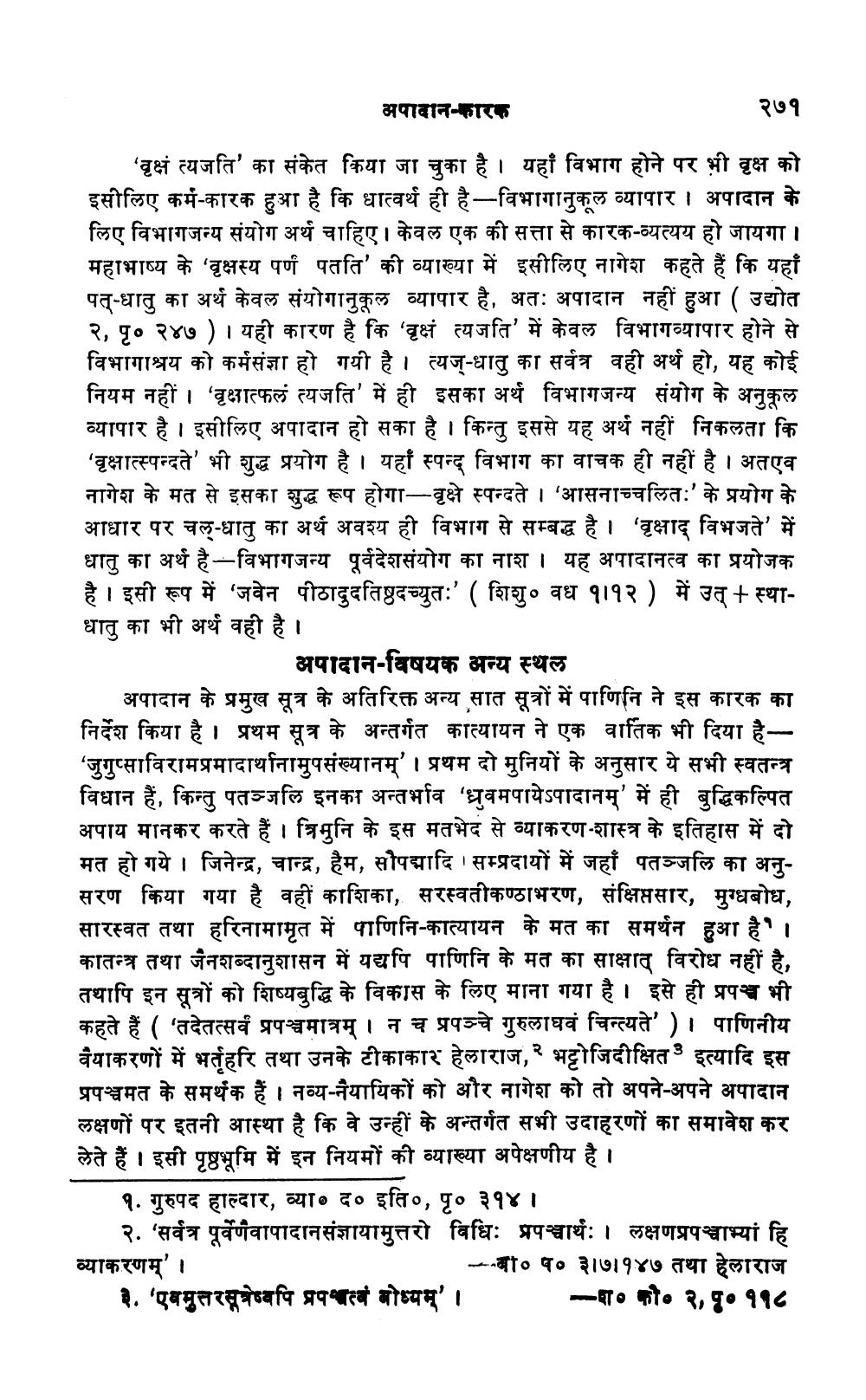________________
अपादान-कारक
२७१
'वृक्षं त्यजति' का संकेत किया जा चुका है। यहाँ विभाग होने पर भी वृक्ष को इसीलिए कर्म-कारक हुआ है कि धात्वर्थ ही है-विभागानुकूल व्यापार । अपादान के लिए विभागजन्य संयोग अर्थ चाहिए। केवल एक की सत्ता से कारक-व्यत्यय हो जायगा। महाभाष्य के 'वृक्षस्य पर्ण पतति' की व्याख्या में इसीलिए नागेश कहते हैं कि यहाँ पत्-धातु का अर्थ केवल संयोगानुकूल व्यापार है, अतः अपादान नहीं हुआ ( उद्योत २, पृ० २४७ ) । यही कारण है कि 'वृक्षं त्यजति' में केवल विभागव्यापार होने से विभागाश्रय को कर्मसंज्ञा हो गयी है। त्यज्-धातु का सर्वत्र वही अर्थ हो, यह कोई नियम नहीं। 'वृक्षात्फलं त्यजति' में ही इसका अर्थ विभागजन्य संयोग के अनुकूल व्यापार है । इसीलिए अपादान हो सका है। किन्तु इससे यह अर्थ नहीं निकलता कि 'वृक्षात्स्पन्दते' भी शुद्ध प्रयोग है। यहाँ स्पन्द विभाग का वाचक ही नहीं है । अतएव नागेश के मत से इसका शुद्ध रूप होगा-वृक्षे स्पन्दते । 'आसनाच्चलितः' के प्रयोग के आधार पर चल्-धातु का अर्थ अवश्य ही विभाग से सम्बद्ध है। 'वृक्षाद् विभजते' में धातु का अर्थ है-विभागजन्य पूर्वदेशसंयोग का नाश । यह अपादानत्व का प्रयोजक है । इसी रूप में 'जवेन पीठादुदतिष्ठदच्युतः' ( शिशु० वध १।१२) में उत् + स्थाधातु का भी अर्थ वही है।
अपादान-विषयक अन्य स्थल अपादान के प्रमुख सूत्र के अतिरिक्त अन्य सात सूत्रों में पाणिनि ने इस कारक का निर्देश किया है। प्रथम सूत्र के अन्तर्गत कात्यायन ने एक वार्तिक भी दिया है'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्' । प्रथम दो मुनियों के अनुसार ये सभी स्वतन्त्र विधान हैं, किन्तु पतञ्जलि इनका अन्तर्भाव 'ध्रुवमपायेऽपादानम्' में ही बुद्धिकल्पित अपाय मानकर करते हैं । त्रिमुनि के इस मतभेद से व्याकरण-शास्त्र के इतिहास में दो मत हो गये। जिनेन्द्र, चान्द्र, हैम, सौपद्मादि । सम्प्रदायों में जहाँ पतञ्जलि का अनुसरण किया गया है वहीं काशिका, सरस्वतीकण्ठाभरण, संक्षिप्तसार, मुग्धबोध, सारस्वत तथा हरिनामामृत में पाणिनि-कात्यायन के मत का समर्थन हुआ है। कातन्त्र तथा जैनशब्दानुशासन में यद्यपि पाणिनि के मत का साक्षात् विरोध नहीं है, तथापि इन सूत्रों को शिष्यबुद्धि के विकास के लिए माना गया है। इसे ही प्रपञ्च भी कहते हैं ( 'तदेतत्सर्वं प्रपञ्चमात्रम् । न च प्रपञ्चे गुरुलाघवं चिन्त्यते' )। पाणिनीय वैयाकरणों में भर्तृहरि तथा उनके टीकाकार हेलाराज,२ भट्टोजिदीक्षित' इत्यादि इस प्रपञ्चमत के समर्थक हैं। नव्य-नैयायिकों को और नागेश को तो अपने-अपने अपादान लक्षणों पर इतनी आस्था है कि वे उन्हीं के अन्तर्गत सभी उदाहरणों का समावेश कर लेते हैं। इसी पृष्ठभूमि में इन नियमों की व्याख्या अपेक्षणीय है।
१. गुरुपद हाल्दार, व्या० द० इति०, पृ० ३१४ ।
२. 'सर्वत्र पूर्वेणैवापादानसंज्ञायामुत्तरो विधिः प्रपञ्चार्थः । लक्षणप्रपञ्चाभ्यां हि व्याकरणम्'।
बा०प० ३१७११४७ तथा हेलाराज ३. 'एवमुत्तरसूत्रेष्वपि प्रपत्य बोध्यम्' । -पा० को. २, पृ० ११८