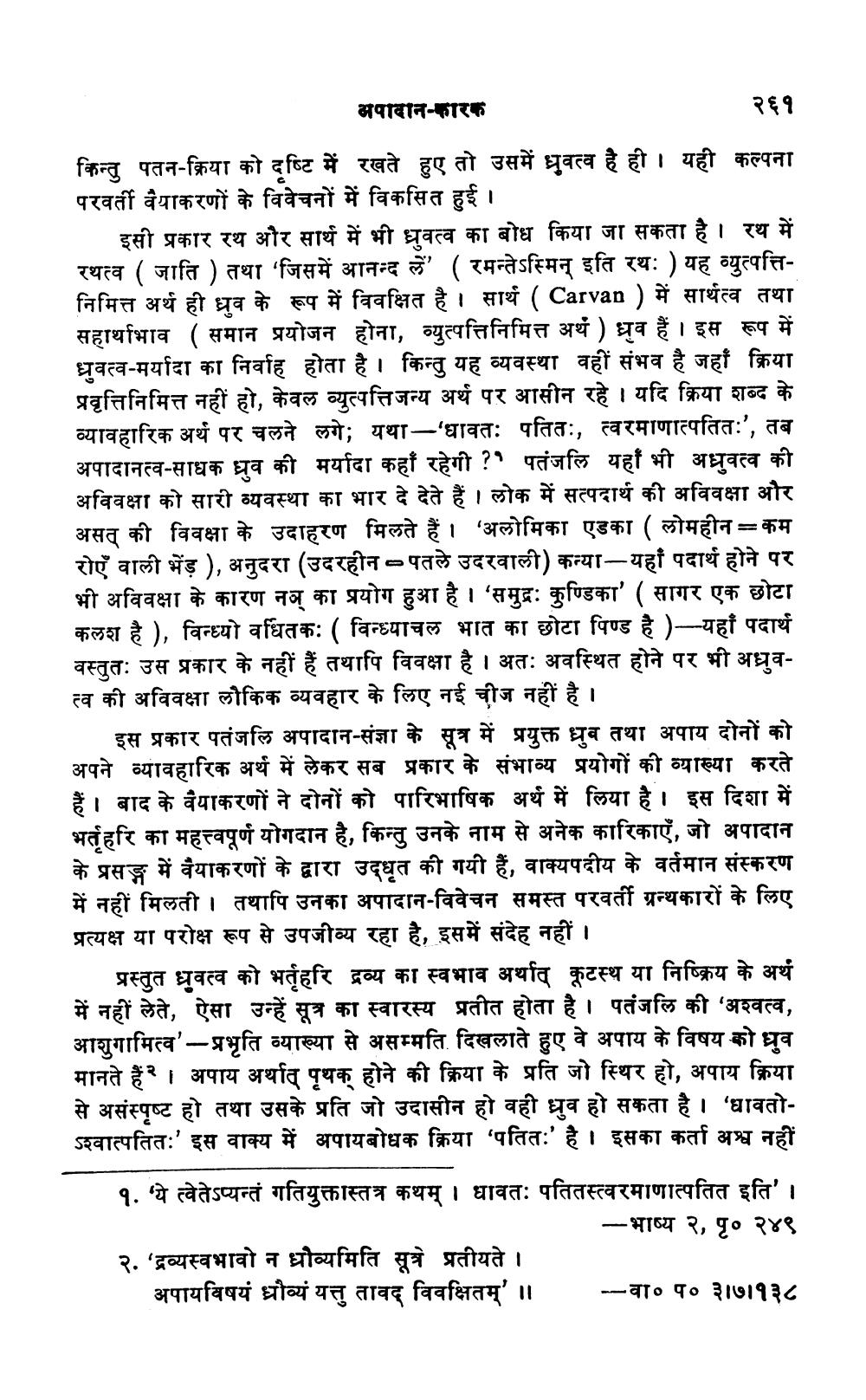________________
अपादान-कारक
२६१
किन्तु पतन-क्रिया को दष्टि में रखते हुए तो उसमें ध्रुवत्व है ही। यही कल्पना परवर्ती वैयाकरणों के विवेचनों में विकसित हुई।
इसी प्रकार रथ और सार्थ में भी ध्रुवत्व का बोध किया जा सकता है। रथ में रथत्व ( जाति ) तथा 'जिसमें आनन्द लें' ( रमन्तेऽस्मिन् इति रथः ) यह व्युत्पत्तिनिमित्त अर्थ ही ध्रुव के रूप में विवक्षित है। सार्थ ( Carvan ) में सार्थत्व तथा सहार्थाभाव ( समान प्रयोजन होना, व्युत्पत्तिनिमित्त अर्थ ) ध्रुव हैं । इस रूप में ध्रुवत्व-मर्यादा का निर्वाह होता है। किन्तु यह व्यवस्था वहीं संभव है जहाँ क्रिया प्रवृत्तिनिमित्त नहीं हो, केवल व्युत्पत्तिजन्य अर्थ पर आसीन रहे । यदि क्रिया शब्द के व्यावहारिक अर्थ पर चलने लगे; यथा-'धावतः पतितः, त्वरमाणात्पतितः', तब अपादानत्व-साधक ध्रुव की मर्यादा कहाँ रहेगी ?' पतंजलि यहाँ भी अध्रुवत्व की अविवक्षा को सारी व्यवस्था का भार दे देते हैं । लोक में सत्पदार्थ की अविवक्षा और असत् की विवक्षा के उदाहरण मिलते हैं। 'अलोमिका एडका ( लोमहीन = कम रोएँ वाली भेंड़ ), अनुदरा (उदरहीन-पतले उदरवाली) कन्या-यहां पदार्थ होने पर भी अविवक्षा के कारण नञ् का प्रयोग हुआ है । 'समुद्रः कुण्डिका' ( सागर एक छोटा कलश है ), विन्ध्यो वधितकः ( विन्ध्याचल भात का छोटा पिण्ड है )-यहाँ पदार्थ वस्तुतः उस प्रकार के नहीं हैं तथापि विवक्षा है । अतः अवस्थित होने पर भी अध्रुवत्व की अविवक्षा लौकिक व्यवहार के लिए नई चीज नहीं है। ___ इस प्रकार पतंजलि अपादान-संज्ञा के सूत्र में प्रयुक्त ध्रुव तथा अपाय दोनों को अपने व्यावहारिक अर्थ में लेकर सब प्रकार के संभाव्य प्रयोगों की व्याख्या करते हैं। बाद के वैयाकरणों ने दोनों को पारिभाषिक अर्थ में लिया है। इस दिशा में भर्तृहरि का महत्त्वपूर्ण योगदान है, किन्तु उनके नाम से अनेक कारिकाएँ, जो अपादान के प्रसङ्ग में वैयाकरणों के द्वारा उद्धृत की गयी हैं, वाक्यपदीय के वर्तमान संस्करण में नहीं मिलती। तथापि उनका अपादान-विवेचन समस्त परवर्ती ग्रन्थकारों के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपजीव्य रहा है, इसमें संदेह नहीं।
प्रस्तुत ध्रुवत्व को भर्तृहरि द्रव्य का स्वभाव अर्थात् कूटस्थ या निष्क्रिय के अर्थ में नहीं लेते, ऐसा उन्हें सूत्र का स्वारस्य प्रतीत होता है। पतंजलि की 'अश्वत्व, आशुगामित्व'-प्रभृति व्याख्या से असम्मति. दिखलाते हुए वे अपाय के विषय को ध्रुव मानते हैं । अपाय अर्थात् पृथक् होने की क्रिया के प्रति जो स्थिर हो, अपाय क्रिया से असंस्पृष्ट हो तथा उसके प्रति जो उदासीन हो वही ध्रुव हो सकता है। 'धावतोऽश्वात्पतितः' इस वाक्य में अपायबोधक क्रिया 'पतितः' है। इसका कर्ता अश्व नहीं १. 'ये त्वेतेऽप्यन्तं गतियुक्तास्तत्र कथम् । धावतः पतितस्त्वरमाणात्पतित इति' ।
-भाष्य २, पृ० २४९ २. 'द्रव्यस्वभावो न ध्रौव्यमिति सूत्रे प्रतीयते ।
अपायविषयं ध्रौव्यं यत्तु तावद् विवक्षितम् ॥ -वा०प० ३।७।१३८