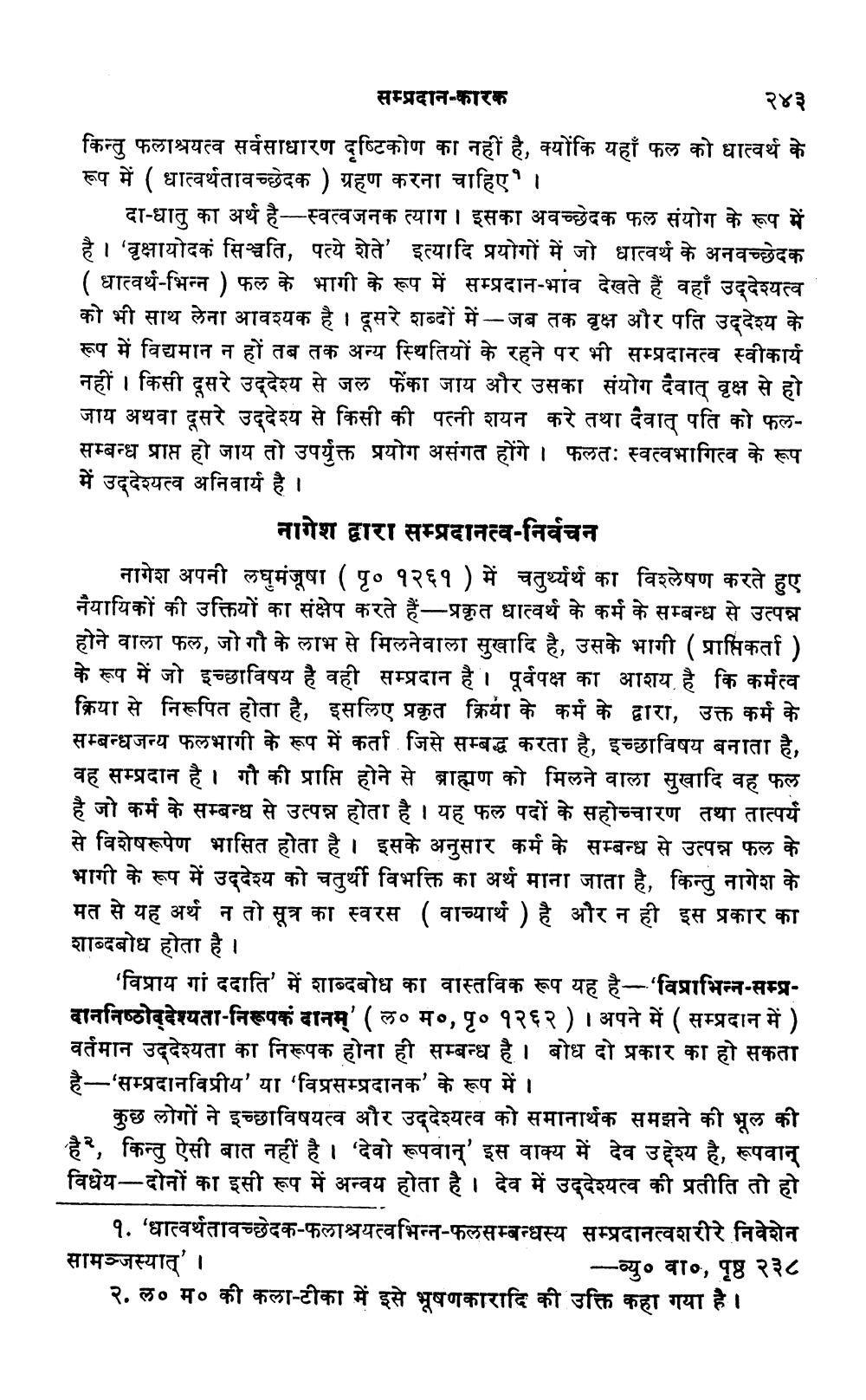________________
सम्प्रदान-कारक
२४३ किन्तु फलाश्रयत्व सर्वसाधारण दृष्टिकोण का नहीं है, क्योंकि यहाँ फल को धात्वर्थ के रूप में (धात्वर्थतावच्छेदक ) ग्रहण करना चाहिए। __दा-धातु का अर्थ है-स्वत्वजनक त्याग। इसका अवच्छेदक फल संयोग के रूप में है। 'वृक्षायोदकं सिञ्चति, पत्ये शेते' इत्यादि प्रयोगों में जो धात्वर्थ के अनवच्छेदक ( धात्वर्थ-भिन्न ) फल के भागी के रूप में सम्प्रदान-भाव देखते हैं वहाँ उद्देश्यत्व को भी साथ लेना आवश्यक है । दूसरे शब्दों में- जब तक वृक्ष और पति उद्देश्य के रूप में विद्यमान न हों तब तक अन्य स्थितियों के रहने पर भी सम्प्रदानत्व स्वीकार्य नहीं। किसी दूसरे उद्देश्य से जल फेंका जाय और उसका संयोग दैवात् वृक्ष से हो जाय अथवा दूसरे उद्देश्य से किसी की पत्नी शयन करे तथा दैवात् पति को फलसम्बन्ध प्राप्त हो जाय तो उपर्युक्त प्रयोग असंगत होंगे। फलतः स्वत्वभागित्व के रूप में उद्देश्यत्व अनिवार्य है।
नागेश द्वारा सम्प्रदानत्व-निर्वचन नागेश अपनी लघुमंजूषा ( पृ० १२६१ ) में चतुर्थ्यर्थ का विश्लेषण करते हुए नैयायिकों की उक्तियों का संक्षेप करते हैं-प्रकृत धात्वर्थ के कर्म के सम्बन्ध से उत्पन्न होने वाला फल, जो गौ के लाभ से मिलनेवाला सुखादि है, उसके भागी (प्राप्तिकर्ता ) के रूप में जो इच्छाविषय है वही सम्प्रदान है। पूर्वपक्ष का आशय है कि कर्मत्व क्रिया से निरूपित होता है, इसलिए प्रकृत क्रिया के कर्म के द्वारा, उक्त कर्म के सम्बन्धजन्य फलभागी के रूप में कर्ता जिसे सम्बद्ध करता है, इच्छाविषय बनाता है, वह सम्प्रदान है। गौ की प्राप्ति होने से ब्राह्मण को मिलने वाला सुखादि वह फल है जो कर्म के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है । यह फल पदों के सहोच्चारण तथा तात्पर्य से विशेषरूपेण भासित होता है। इसके अनुसार कर्म के सम्बन्ध से उत्पन्न फल के भागी के रूप में उद्देश्य को चतुर्थी विभक्ति का अर्थ माना जाता है, किन्तु नागेश के मत से यह अर्थ न तो सूत्र का स्वरस ( वाच्यार्थ) है और न ही इस प्रकार का शाब्दबोध होता है।
'विप्राय गां ददाति' में शाब्दबोध का वास्तविक रूप यह है- 'विप्राभिन्न-सम्प्र. दाननिष्ठोदेश्यता-निरूपकं दानम्' (ल० म०, पृ० १२६२) । अपने में ( सम्प्रदान में) वर्तमान उद्देश्यता का निरूपक होना ही सम्बन्ध है। बोध दो प्रकार का हो सकता है-'सम्प्रदानविप्रीय' या 'विप्रसम्प्रदानक' के रूप में।
कुछ लोगों ने इच्छाविषयत्व और उद्देश्यत्व को समानार्थक समझने की भूल की है, किन्तु ऐसी बात नहीं है । 'देवो रूपवान्' इस वाक्य में देव उद्देश्य है, रूपवान् विधेय-दोनों का इसी रूप में अन्वय होता है। देव में उद्देश्यत्व की प्रतीति तो हो
१. 'धात्वर्थतावच्छेदक-फलाश्रयत्वभिन्न-फलसम्बन्धस्य सम्प्रदानत्वशरीरे निवेशेन सामञ्जस्यात्'।
-व्यु० वा०, पृष्ठ २३८ २. ल० म० की कला-टीका में इसे भूषणकारादि की उक्ति कहा गया है।