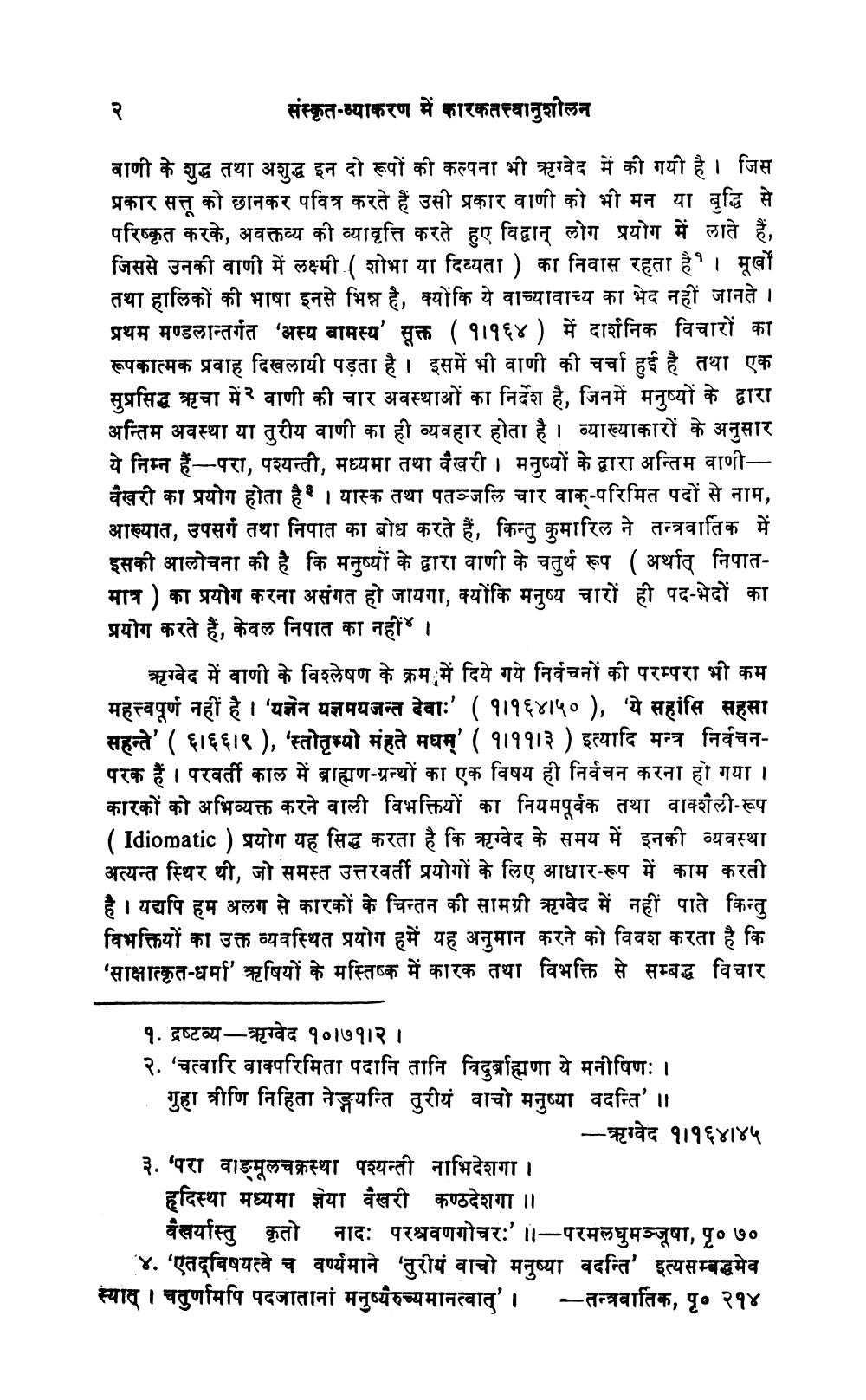________________
संस्कृत व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन
वाणी के शुद्ध तथा अशुद्ध इन दो रूपों की कल्पना भी ऋग्वेद में की गयी है । जिस प्रकार सत्तू को छानकर पवित्र करते हैं उसी प्रकार वाणी को भी मन या बुद्धि से परिष्कृत करके, अवक्तव्य की व्यावृत्ति करते हुए विद्वान् लोग प्रयोग में लाते हैं, जिससे उनकी वाणी में लक्ष्मी ( शोभा या दिव्यता ) का निवास रहता है । मूर्खो तथा हालिकों की भाषा इनसे भिन्न है, क्योंकि ये वाच्यावाच्य का भेद नहीं जानते । प्रथम मण्डलान्तर्गत 'अस्य वामस्य' सूक्त ( १1१६४ ) में दार्शनिक विचारों का रूपकात्मक प्रवाह दिखलायी पड़ता है। इसमें भी वाणी की चर्चा हुई है तथा एक सुप्रसिद्ध ऋचा में वाणी की चार अवस्थाओं का निर्देश है, जिनमें मनुष्यों के द्वारा अन्तिम अवस्था या तुरीय वाणी का ही व्यवहार होता है । व्याख्याकारों के अनुसार ये निम्न हैं- परा, पश्यन्ती, मध्यमा तथा वैखरी । मनुष्यों के द्वारा अन्तिम वाणीवैखरी का प्रयोग होता है । यास्क तथा पतञ्जलि चार वाक्-परिमित पदों से नाम, आख्यात, उपसर्ग तथा निपात का बोध करते हैं, किन्तु कुमारिल ने तन्त्रवार्तिक में इसकी आलोचना की है कि मनुष्यों के द्वारा वाणी के चतुर्थ रूप ( अर्थात् निपातमात्र ) का प्रयोग करना असंगत हो जायगा, क्योंकि मनुष्य चारों ही पद-भेदों का प्रयोग करते हैं, केवल निपात का नहीं ।
ऋग्वेद में वाणी के विश्लेषण के क्रम में दिये गये निर्वचनों की परम्परा भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' ( १।१६४|५०), 'ये सहांसि सहसा सहन्ते ' ( ६ । ६६ । ९ ), 'स्तोतृभ्यो मंहते मघम्' ( १।११।३ ) इत्यादि मन्त्र निर्वचनपरक हैं । परवर्ती काल में ब्राह्मण-ग्रन्थों का एक विषय ही निर्वचन करना हो गया । कारकों को अभिव्यक्त करने वाली विभक्तियों का नियमपूर्वक तथा वाक्शैली- रूप ( Idiomatic ) प्रयोग यह सिद्ध करता है कि ऋग्वेद के समय में इनकी व्यवस्था अत्यन्त स्थिर थी, जो समस्त उत्तरवर्ती प्रयोगों के लिए आधार रूप में काम करती है । यद्यपि हम अलग से कारकों के चिन्तन की सामग्री ऋग्वेद में नहीं पाते किन्तु विभक्तियों का उक्त व्यवस्थित प्रयोग हमें यह अनुमान करने को विवश करता है कि 'साक्षात्कृत-धर्मा' ऋषियों के मस्तिष्क में कारक तथा विभक्ति से सम्बद्ध विचार
१. द्रष्टव्य – ऋग्वेद १०।७१।२ ।
२. ' चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति' ॥
- ऋग्वेद १।१६४।४५
३. 'परा वाङ्मूलचक्रस्था पश्यन्ती नाभिदेशगा । हृदिस्था मध्यमा ज्ञेया वैखरी कण्ठदेशगा ॥
वैखर्यास्तु कृतो नादः परश्रवणगोचर: ' ॥ - परमलघुमञ्जूषा, पृ० ७० ४. 'एतद्विषयत्वे च वर्ण्यमाने 'तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति' इत्यसम्बद्धमेव स्यात् । चतुर्णामपि पदजातानां मनुष्यैरुच्यमानत्वात्' । - तन्त्रवार्तिक, पृ० २१४