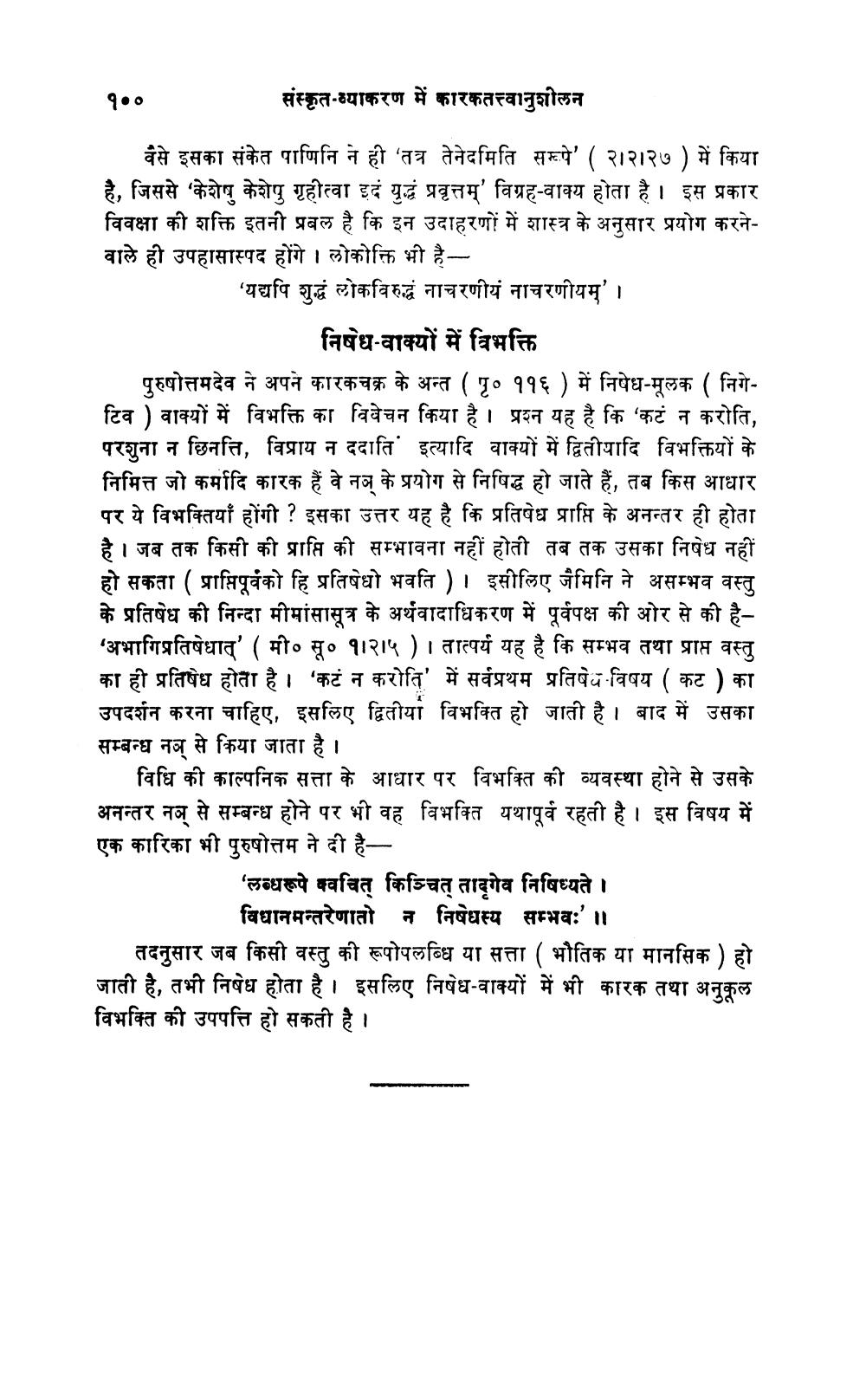________________
संस्कृत व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन
वैसे इसका संकेत पाणिनि ने ही 'तत्र तेनेदमिति सरूपे' ( २।२।२७ ) में किया है, जिससे 'केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्' विग्रह वाक्य होता है । इस प्रकार विवक्षा की शक्ति इतनी प्रबल है कि इन उदाहरणों में शास्त्र के अनुसार प्रयोग करनेवाले ही उपहासास्पद होंगे । लोकोक्ति भी है—
'यद्यपि शुद्धं लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाचरणीयम्' ।
निषेध वाक्यों में विभक्ति
पुरुषोत्तमदेव ने अपने कारकचक्र के अन्त ( पृ० ११६ ) में निषेध - मूलक ( निगेटिव) वाक्यों में विभक्ति का विवेचन किया है। प्रश्न यह है कि 'कटं न करोति, परशुना न छिनत्ति, विप्राय न ददाति इत्यादि वाक्यों में द्वितीयादि विभक्तियों के निमित्त जो कर्मादि कारक हैं वे नञ् के प्रयोग से निषिद्ध हो जाते हैं, तब किस आधार पर ये विभक्तियाँ होंगी ? इसका उत्तर यह है कि प्रतिषेध प्राप्ति के अनन्तर ही होता है । जब तक किसी की प्राप्ति की सम्भावना नहीं होती तब तक उसका निषेध नहीं हो सकता ( प्राप्तिपूर्वको हि प्रतिषेधो भवति ) । इसीलिए जैमिनि ने असम्भव वस्तु
प्रतिषेध की निन्दा मीमांसासूत्र के अर्थवादाधिकरण में पूर्वपक्ष की ओर से की है'अभागि प्रतिषेधात् ' ( मी० सू० १/२/५ ) । तात्पर्य यह है कि सम्भव तथा प्राप्त वस्तु काही प्रतिषेध होता है । 'कटं न करोति' में सर्वप्रथम प्रतिषेध विषय ( कट ) का उपदर्शन करना चाहिए, इसलिए द्वितीया विभक्ति हो जाती है । बाद में उसका सम्बन्ध नत्र से किया जाता है ।
१००
विधि की काल्पनिक सत्ता के आधार पर विभक्ति की व्यवस्था होने से उसके अनन्तर नत्र से सम्बन्ध होने पर भी वह विभक्ति यथापूर्व रहती है । इस विषय में एक कारिका भी पुरुषोत्तम ने दी है
'लन्धरूपे क्वचित् किञ्चित् तादृगेव निषिध्यते । विधानमन्तरेणातो न निषेधस्य सम्भवः ॥
तदनुसार जब किसी वस्तु की रूपोपलब्धि या सत्ता ( भौतिक या मानसिक ) हो जाती है, तभी निषेध होता है । इसलिए निषेध वाक्यों में भी कारक तथा अनुकूल विभक्ति की उपपत्ति हो सकती है ।