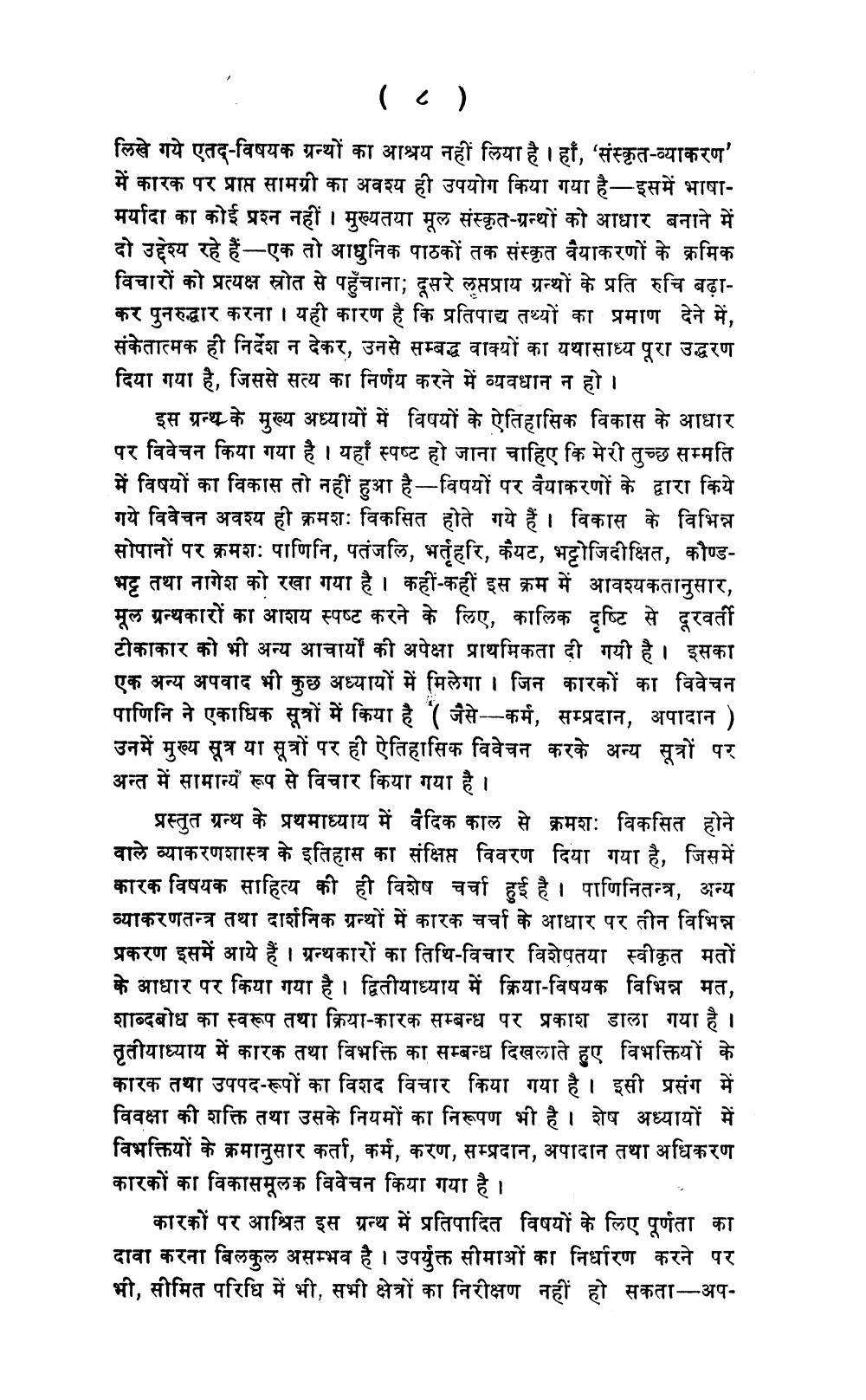________________
( ८ )
लिखे गये एतद् - विषयक ग्रन्थों का आश्रय नहीं लिया है। हाँ, 'संस्कृत - व्याकरण' में कारक पर प्राप्त सामग्री का अवश्य ही उपयोग किया गया है— इसमें भाषामर्यादा का कोई प्रश्न नहीं । मुख्यतया मूल संस्कृत-ग्रन्थों को आधार बनाने में दो उद्देश्य रहे हैं - एक तो आधुनिक पाठकों तक संस्कृत वैयाकरणों के क्रमिक विचारों को प्रत्यक्ष स्रोत से पहुँचाना; दूसरे लुप्तप्राय ग्रन्थों के प्रति रुचि बढ़ाकर पुनरुद्धार करना । यही कारण है कि प्रतिपाद्य तथ्यों का प्रमाण देने में, संकेतात्मक ही निर्देश न देकर, उनसे सम्बद्ध वाक्यों का यथासाध्य पूरा उद्धरण दिया गया है, जिससे सत्य का निर्णय करने में व्यवधान न हो ।
इस ग्रन्थ के मुख्य अध्यायों में विषयों के ऐतिहासिक विकास के आधार पर विवेचन किया गया है । यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मेरी तुच्छ सम्मति में विषयों का विकास तो नहीं हुआ है -विषयों पर वैयाकरणों के द्वारा किये गये विवेचन अवश्य ही क्रमशः विकसित होते गये हैं । विकास के विभिन्न सोपानों पर क्रमशः पाणिनि, पतंजलि, भर्तृहरि, कैयट भट्टोजिदीक्षित, कौण्डभट्ट तथा नागेश को रखा गया है । कहीं-कहीं इस क्रम में आवश्यकतानुसार, मूल ग्रन्थकारों का आशय स्पष्ट करने के लिए, कालिक दृष्टि से दूरवर्ती टीकाकार को भी अन्य आचार्यों की अपेक्षा प्राथमिकता दी गयी है । इसका एक अन्य अपवाद भी कुछ अध्यायों में मिलेगा । जिन कारकों का विवेचन पाणिनि ने एकाधिक सूत्रों में किया है ( जैसे --- कर्म, सम्प्रदान, अपादान ) उनमें मुख्य सूत्र या सूत्रों पर ही ऐतिहासिक विवेचन करके अन्य सूत्रों पर अन्त में सामान्य रूप से विचार किया गया है ।
प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रथमाध्याय में वैदिक काल से क्रमश: विकसित होने वाले व्याकरणशास्त्र के इतिहास का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, जिसमें कारक विषयक साहित्य की ही विशेष चर्चा हुई है । पाणिनितन्त्र, अन्य व्याकरणतन्त्र तथा दार्शनिक ग्रन्थों में कारक चर्चा के आधार पर तीन विभिन्न प्रकरण इसमें आये हैं । ग्रन्थकारों का तिथि - विचार विशेषतया स्वीकृत मतों के आधार पर किया गया है । द्वितीयाध्याय में क्रिया-विषयक विभिन्न मत, शाब्दबोध का स्वरूप तथा क्रिया-कारक सम्बन्ध पर प्रकाश डाला गया है । तृतीयाध्याय में कारक तथा विभक्ति का सम्बन्ध दिखलाते हुए विभक्तियों के कारक तथा उपपद-रूपों का विशद विचार किया गया है । इसी प्रसंग में विवक्षा की शक्ति तथा उसके नियमों का निरूपण भी है । शेष अध्यायों में विभक्तियों के क्रमानुसार कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण कारकों का विकासमूलक विवेचन किया गया है ।
कारकों पर आश्रित इस ग्रन्थ में प्रतिपादित विषयों के लिए पूर्णता का दावा करना बिलकुल असम्भव है । उपर्युक्त सीमाओं का निर्धारण करने पर भी, सीमित परिधि में भी, सभी क्षेत्रों का निरीक्षण नहीं हो सकता - अप