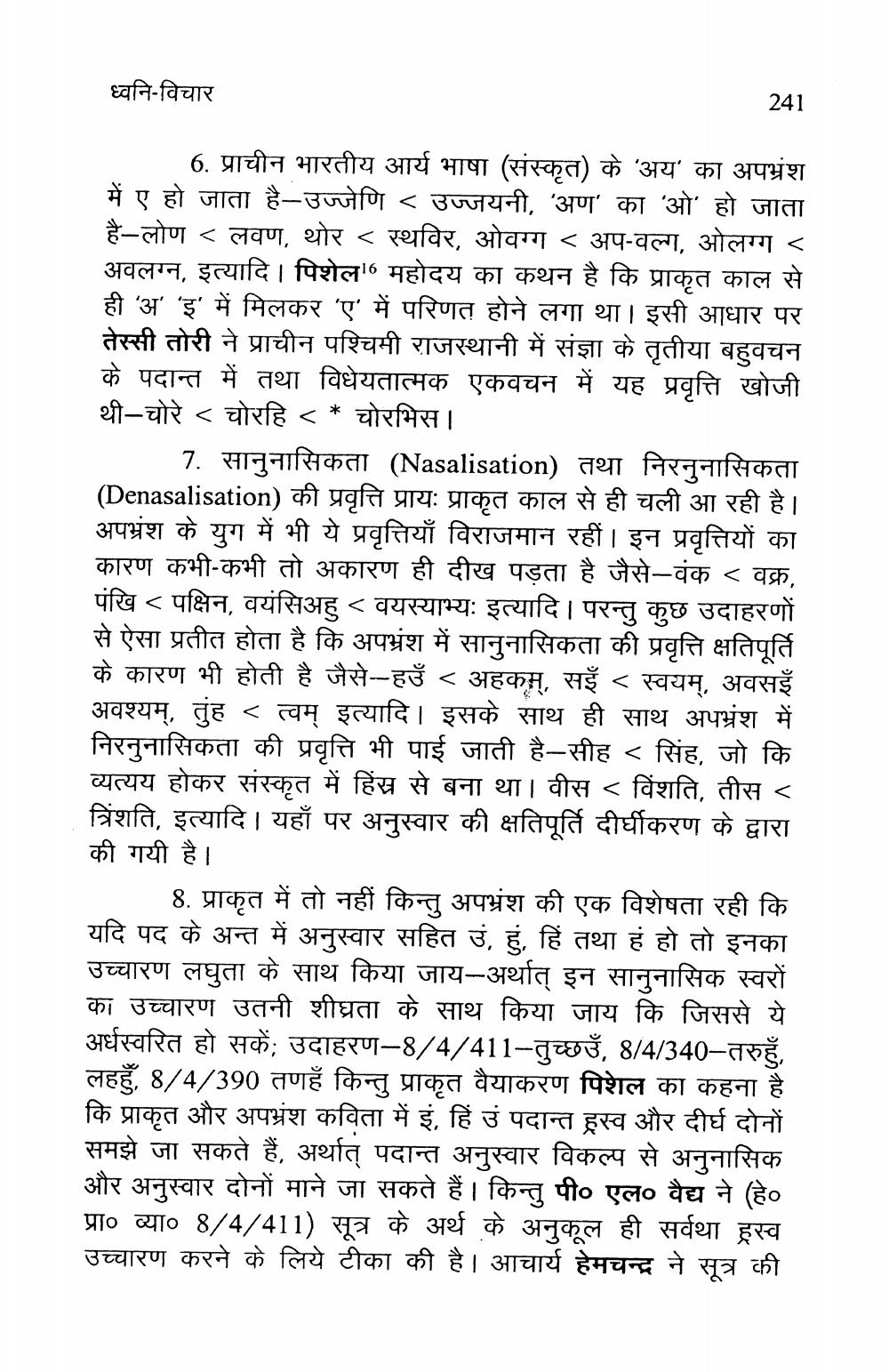________________
ध्वनि-विचार
241
6. प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (संस्कृत) के 'अय' का अपभ्रंश में ए हो जाता है-उज्जेणि < उज्जयनी, 'अण' का 'ओ' हो जाता है-लोण < लवण, थोर < स्थविर, ओवग्ग < अप-वल्ग, ओलग्ग < अवलग्न, इत्यादि। पिशेला6 महोदय का कथन है कि प्राकृत काल से ही 'अ' 'इ' में मिलकर 'ए' में परिणत होने लगा था। इसी आधार पर तेस्सी तोरी ने प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी में संज्ञा के तृतीया बहुवचन के पदान्त में तथा विधेयतात्मक एकवचन में यह प्रवृत्ति खोजी थी-चोरे < चोरहि < * चोरभिस ।
7. सानुनासिकता (Nasalisation) तथा निरनुनासिकता (Denasalisation) की प्रवृत्ति प्रायः प्राकृत काल से ही चली आ रही है। अपभ्रंश के युग में भी ये प्रवृत्तियाँ विराजमान रहीं। इन प्रवृत्तियों का कारण कभी-कभी तो अकारण ही दीख पड़ता है जैसे-वंक < वक्र, पंखि < पक्षिन, वयंसिअहु < वयस्याभ्यः इत्यादि। परन्तु कुछ उदाहरणों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपभ्रंश में सानुनासिकता की प्रवृत्ति क्षतिपूर्ति के कारण भी होती है जैसे-हउँ < अहकम्, सइँ < स्वयम्, अवस अवश्यम्, तुंह < त्वम् इत्यादि। इसके साथ ही साथ अपभ्रंश में निरनुनासिकता की प्रवृत्ति भी पाई जाती है-सीह < सिंह, जो कि व्यत्यय होकर संस्कृत में हिंस्र से बना था। वीस < विंशति, तीस < त्रिंशति, इत्यादि । यहाँ पर अनुस्वार की क्षतिपूर्ति दीर्धीकरण के द्वारा की गयी है।
8. प्राकृत में तो नहीं किन्तु अपभ्रंश की एक विशेषता रही कि यदि पद के अन्त में अनुस्वार सहित उं, हं, हिं तथा हं हो तो इनका उच्चारण लघुता के साथ किया जाय-अर्थात् इन सानुनासिक स्वरों का उच्चारण उतनी शीघ्रता के साथ किया जाय कि जिससे ये अर्धस्वरित हो सकें; उदाहरण-8/4/411-तुच्छउँ, 8/4/340-तरुहुँ, लहहुँ, 8/4/390 तणहँ किन्तु प्राकृत वैयाकरण पिशेल का कहना है कि प्राकृत और अपभ्रंश कविता में इं, हिं उं पदान्त हस्व और दीर्घ दोनों समझे जा सकते हैं, अर्थात् पदान्त अनुस्वार विकल्प से अनुनासिक
और अनुस्वार दोनों माने जा सकते हैं। किन्तु पी० एल० वैद्य ने (हे० प्रा० व्या० 8/4/411) सूत्र के अर्थ के अनुकूल ही सर्वथा हस्व उच्चारण करने के लिये टीका की है। आचार्य हेमचन्द्र ने सूत्र की