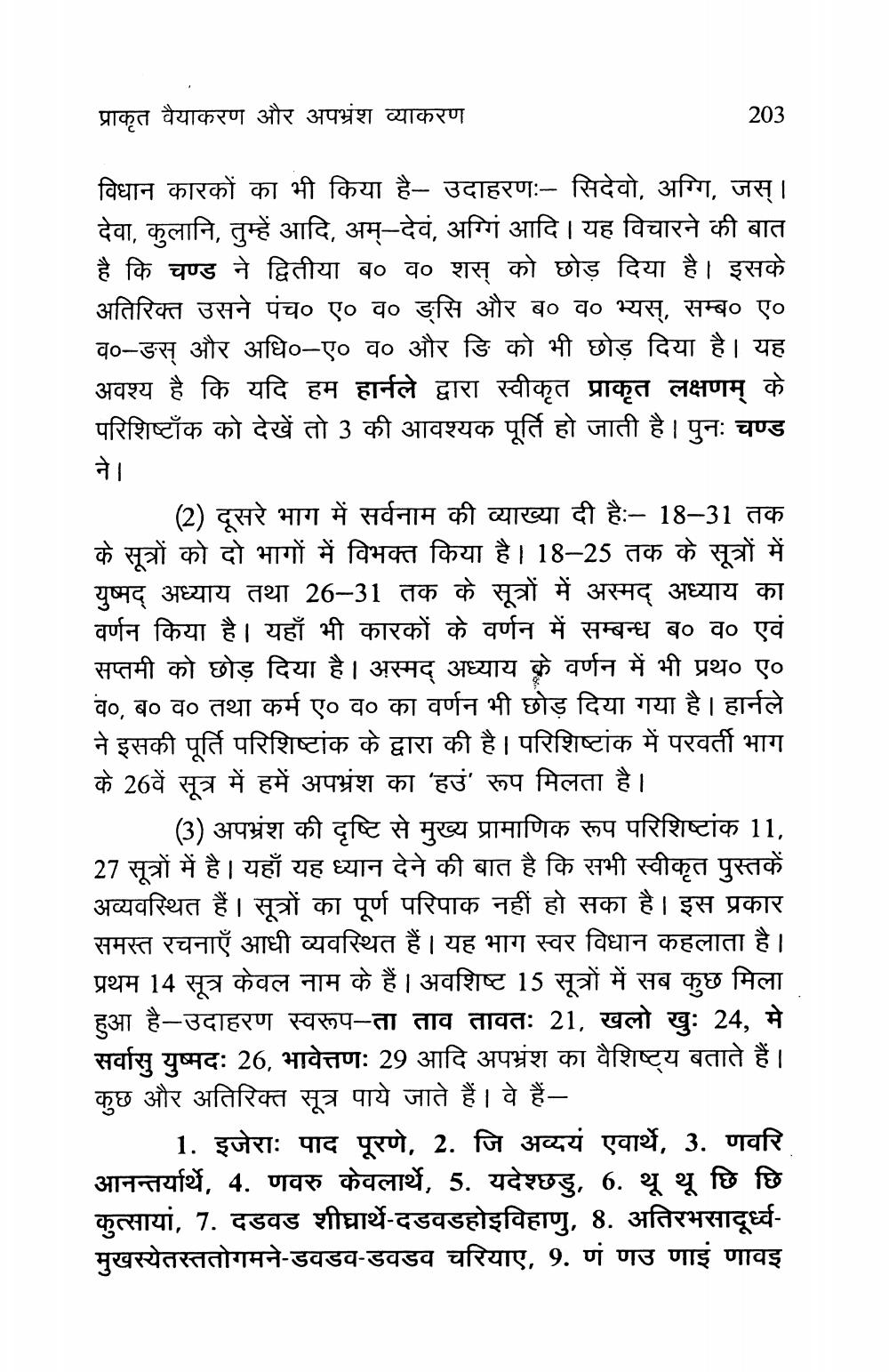________________
प्राकृत वैयाकरण और अपभ्रंश व्याकरण
203
विधान कारकों का भी किया है- उदाहरण:- सिदेवो, अग्गि, जस् । देवा, कुलानि, तुम्हें आदि, अम्-देवं, अग्गिं आदि । यह विचारने की बात है कि चण्ड ने द्वितीया ब० व० शस् को छोड़ दिया है। इसके अतिरिक्त उसने पंच० ए० व० सि और ब० व० भ्यस्, सम्ब० ए० व०-ङस और अधि०-ए० व० और ङि को भी छोड़ दिया है। यह अवश्य है कि यदि हम हार्नले द्वारा स्वीकृत प्राकृत लक्षणम् के परिशिष्टाँक को देखें तो 3 की आवश्यक पूर्ति हो जाती है। पुनः चण्ड ने।
(2) दूसरे भाग में सर्वनाम की व्याख्या दी है:- 18-31 तक के सूत्रों को दो भागों में विभक्त किया है। 18-25 तक के सूत्रों में युष्मद् अध्याय तथा 26-31 तक के सूत्रों में अस्मद् अध्याय का वर्णन किया है। यहाँ भी कारकों के वर्णन में सम्बन्ध ब० व० एवं सप्तमी को छोड़ दिया है। अस्मद् अध्याय के वर्णन में भी प्रथ० ए० व०, ब० व० तथा कर्म ए० व० का वर्णन भी छोड़ दिया गया है। हार्नले ने इसकी पूर्ति परिशिष्टांक के द्वारा की है। परिशिष्टांक में परवर्ती भाग के 26वें सूत्र में हमें अपभ्रंश का 'हउं' रूप मिलता है।
(3) अपभ्रंश की दृष्टि से मुख्य प्रामाणिक रूप परिशिष्टांक 11, 27 सूत्रों में है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि सभी स्वीकृत पुस्तकें अव्यवस्थित हैं। सूत्रों का पूर्ण परिपाक नहीं हो सका है। इस प्रकार समस्त रचनाएँ आधी व्यवस्थित हैं। यह भाग स्वर विधान कहलाता है। प्रथम 14 सूत्र केवल नाम के हैं । अवशिष्ट 15 सूत्रों में सब कुछ मिला हुआ है-उदाहरण स्वरूप-ता ताव तावतः 21, खलो खुः 24, मे सर्वासु युष्मदः 26, भावेत्तणः 29 आदि अपभ्रंश का वैशिष्ट्य बताते हैं। कुछ और अतिरिक्त सूत्र पाये जाते हैं। वे हैं
1. इजेराः पाद पूरणे, 2. जि अव्ययं एवार्थे, 3. णवरि आनन्तर्यार्थे, 4. णवरु केवलार्थे, 5. यदेश्छडु, 6. थू थू छि छि कुत्सायां, 7. दडवड शीघ्रार्थे-दडवडहोइविहाणु, 8. अतिरभसादूर्ध्वमुखस्येतस्ततोगमने-डवडव-डवडव चरियाए, 9. णं ण णाई णावइ