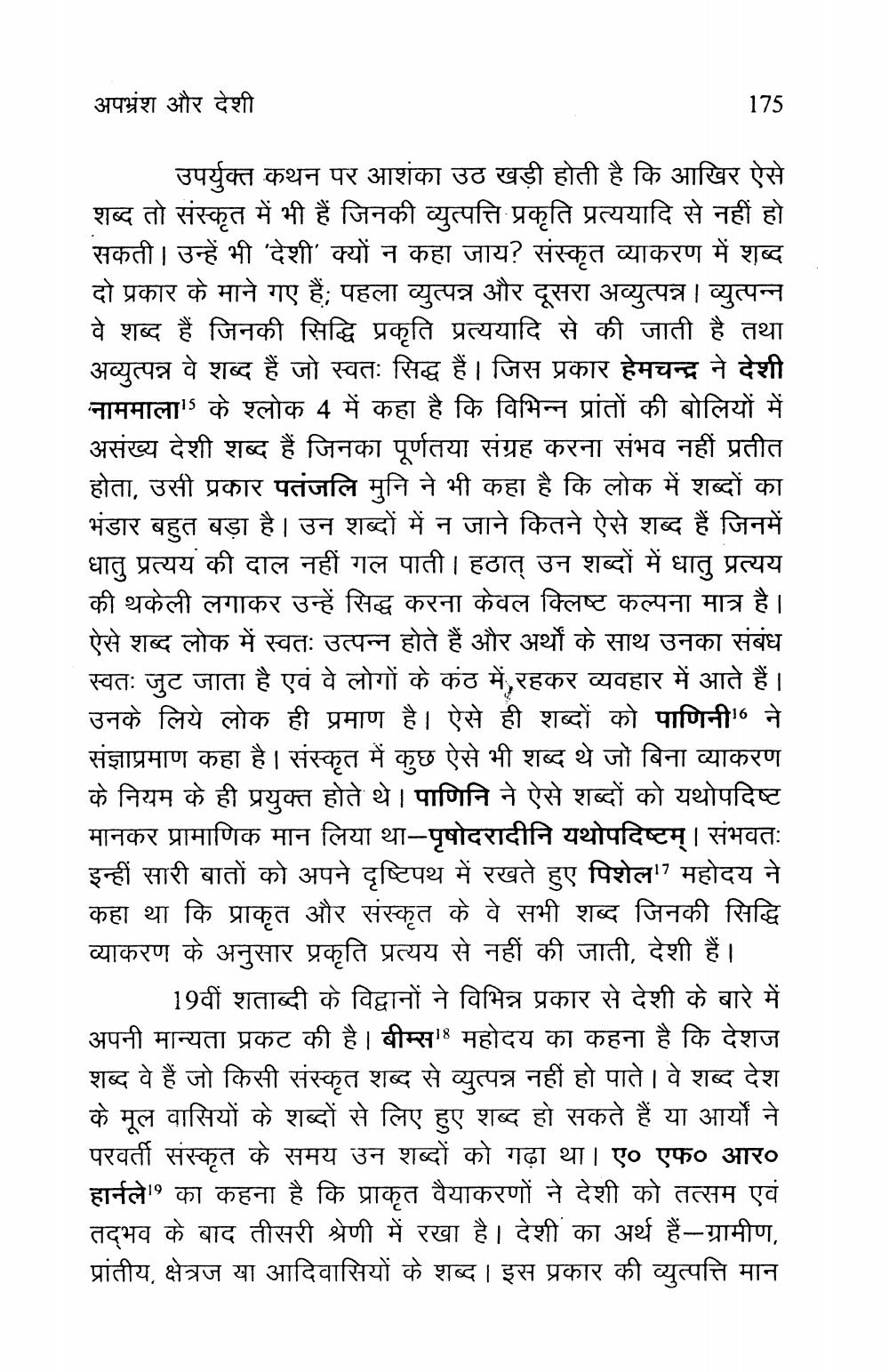________________
अपभ्रंश और देशी
175
उपर्युक्त कथन पर आशंका उठ खड़ी होती है कि आखिर ऐसे शब्द तो संस्कृत में भी हैं जिनकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्ययादि से नहीं हो सकती। उन्हें भी 'देशी' क्यों न कहा जाय? संस्कृत व्याकरण में शब्द दो प्रकार के माने गए हैं; पहला व्युत्पन्न और दूसरा अव्युत्पन्न । व्युत्पन्न वे शब्द हैं जिनकी सिद्धि प्रकृति प्रत्ययादि से की जाती है तथा अव्युत्पन्न वे शब्द हैं जो स्वतः सिद्ध हैं। जिस प्रकार हेमचन्द्र ने देशी नाममाला' के श्लोक 4 में कहा है कि विभिन्न प्रांतों की बोलियों में असंख्य देशी शब्द हैं जिनका पूर्णतया संग्रह करना संभव नहीं प्रतीत होता, उसी प्रकार पतंजलि मुनि ने भी कहा है कि लोक में शब्दों का भंडार बहुत बड़ा है। उन शब्दों में न जाने कितने ऐसे शब्द हैं जिनमें धातु प्रत्यय की दाल नहीं गल पाती। हठात् उन शब्दों में धातु प्रत्यय की थकेली लगाकर उन्हें सिद्ध करना केवल क्लिष्ट कल्पना मात्र है। ऐसे शब्द लोक में स्वतः उत्पन्न होते हैं और अर्थों के साथ उनका संबंध स्वतः जुट जाता है एवं वे लोगों के कंठ में,रहकर व्यवहार में आते हैं। उनके लिये लोक ही प्रमाण है। ऐसे ही शब्दों को पाणिनी ने संज्ञाप्रमाण कहा है। संस्कृत में कुछ ऐसे भी शब्द थे जो बिना व्याकरण के नियम के ही प्रयुक्त होते थे। पाणिनि ने ऐसे शब्दों को यथोपदिष्ट मानकर प्रामाणिक मान लिया था-पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् । संभवतः इन्हीं सारी बातों को अपने दृष्टिपथ में रखते हुए पिशेल17 महोदय ने कहा था कि प्राकृत और संस्कृत के वे सभी शब्द जिनकी सिद्धि व्याकरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय से नहीं की जाती, देशी हैं।
19वीं शताब्दी के विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से देशी के बारे में अपनी मान्यता प्रकट की है। बीम्स महोदय का कहना है कि देशज शब्द वे हैं जो किसी संस्कृत शब्द से व्युत्पन्न नहीं हो पाते। वे शब्द देश के मूल वासियों के शब्दों से लिए हुए शब्द हो सकते हैं या आर्यों ने परवर्ती संस्कृत के समय उन शब्दों को गढ़ा था। ए० एफ० आर० हार्नले' का कहना है कि प्राकृत वैयाकरणों ने देशी को तत्सम एवं तद्भव के बाद तीसरी श्रेणी में रखा है। देशी का अर्थ हैं-ग्रामीण, प्रांतीय, क्षेत्रज या आदिवासियों के शब्द । इस प्रकार की व्युत्पत्ति मान