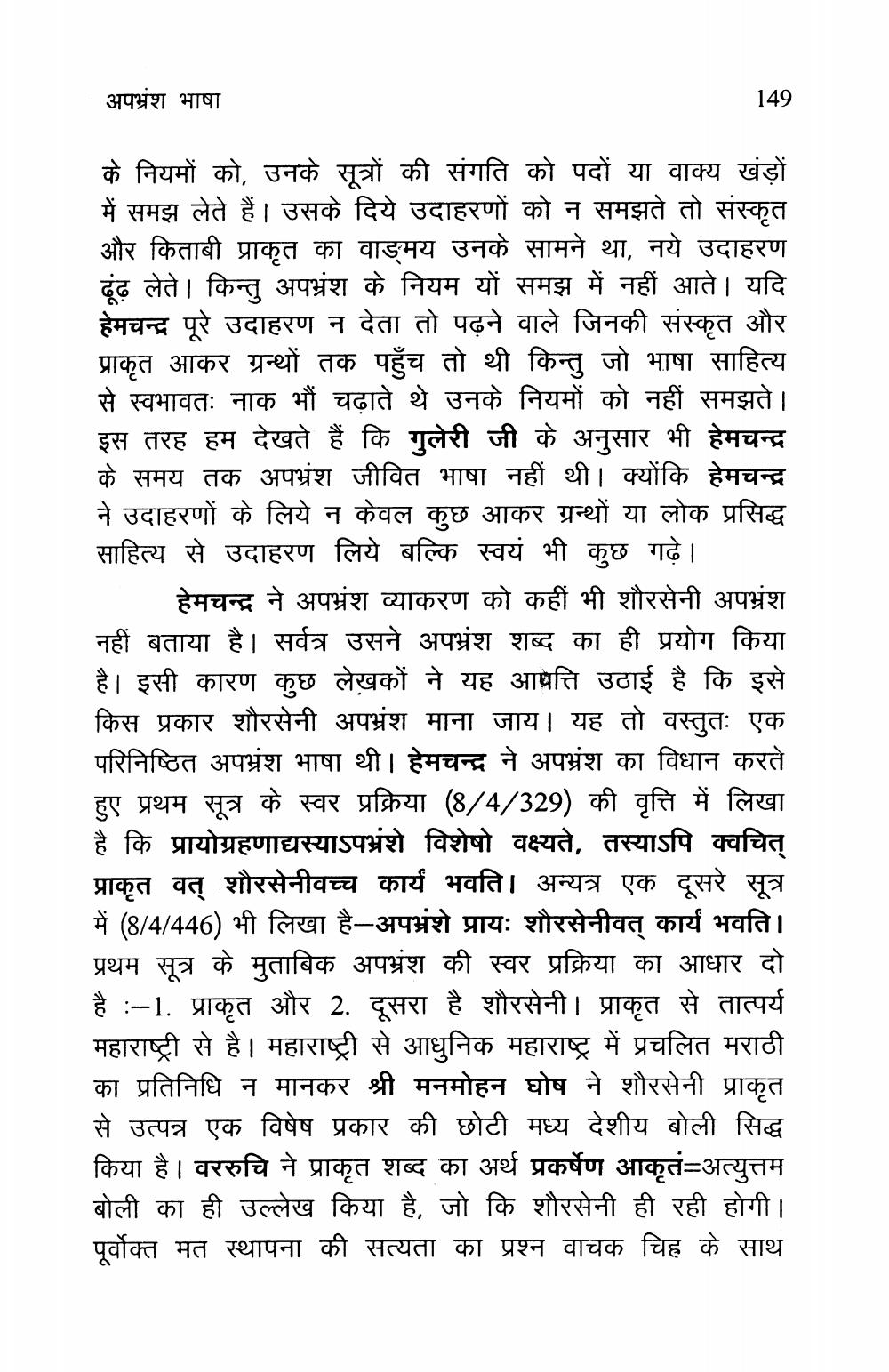________________
अपभ्रंश भाषा
149
के नियमों को, उनके सूत्रों की संगति को पदों या वाक्य खंड़ों में समझ लेते हैं। उसके दिये उदाहरणों को न समझते तो संस्कृत और किताबी प्राकृत का वाङ्मय उनके सामने था, नये उदाहरण ढूंढ लेते। किन्तु अपभ्रंश के नियम यों समझ में नहीं आते। यदि हेमचन्द्र पूरे उदाहरण न देता तो पढ़ने वाले जिनकी संस्कृत और प्राकृत आकर ग्रन्थों तक पहुँच तो थी किन्तु जो भाषा साहित्य से स्वभावतः नाक भौं चढ़ाते थे उनके नियमों को नहीं समझते। इस तरह हम देखते हैं कि गुलेरी जी के अनुसार भी हेमचन्द्र के समय तक अपभ्रंश जीवित भाषा नहीं थी। क्योंकि हेमचन्द्र ने उदाहरणों के लिये न केवल कुछ आकर ग्रन्थों या लोक प्रसिद्ध साहित्य से उदाहरण लिये बल्कि स्वयं भी कुछ गढ़े।
हेमचन्द्र ने अपभ्रंश व्याकरण को कहीं भी शौरसेनी अपभ्रंश नहीं बताया है। सर्वत्र उसने अपभ्रंश शब्द का ही प्रयोग किया है। इसी कारण कुछ लेखकों ने यह आपत्ति उठाई है कि इसे किस प्रकार शौरसेनी अपभ्रंश माना जाय। यह तो वस्तुतः एक परिनिष्ठित अपभ्रंश भाषा थी। हेमचन्द्र ने अपभ्रंश का विधान करते हुए प्रथम सूत्र के स्वर प्रक्रिया (8/4/329) की वृत्ति में लिखा है कि प्रायोग्रहणाद्यस्याऽपभ्रंशे विशेषो वक्ष्यते, तस्याऽपि क्वचित् प्राकृत वत् शौरसेनीवच्च कार्यं भवति। अन्यत्र एक दूसरे सूत्र में (8/4/446) भी लिखा है-अपभ्रंशे प्रायः शौरसेनीवत् कार्यं भवति। प्रथम सूत्र के मुताबिक अपभ्रंश की स्वर प्रक्रिया का आधार दो है :-1. प्राकृत और 2. दूसरा है शौरसेनी। प्राकृत से तात्पर्य महाराष्ट्री से है। महाराष्ट्री से आधुनिक महाराष्ट्र में प्रचलित मराठी का प्रतिनिधि न मानकर श्री मनमोहन घोष ने शौरसेनी प्राकृत से उत्पन्न एक विषेष प्रकार की छोटी मध्य देशीय बोली सिद्ध किया है। वररुचि ने प्राकृत शब्द का अर्थ प्रकर्षेण आकृतं अत्युत्तम बोली का ही उल्लेख किया है, जो कि शौरसेनी ही रही होगी। पूर्वोक्त मत स्थापना की सत्यता का प्रश्न वाचक चिह के साथ