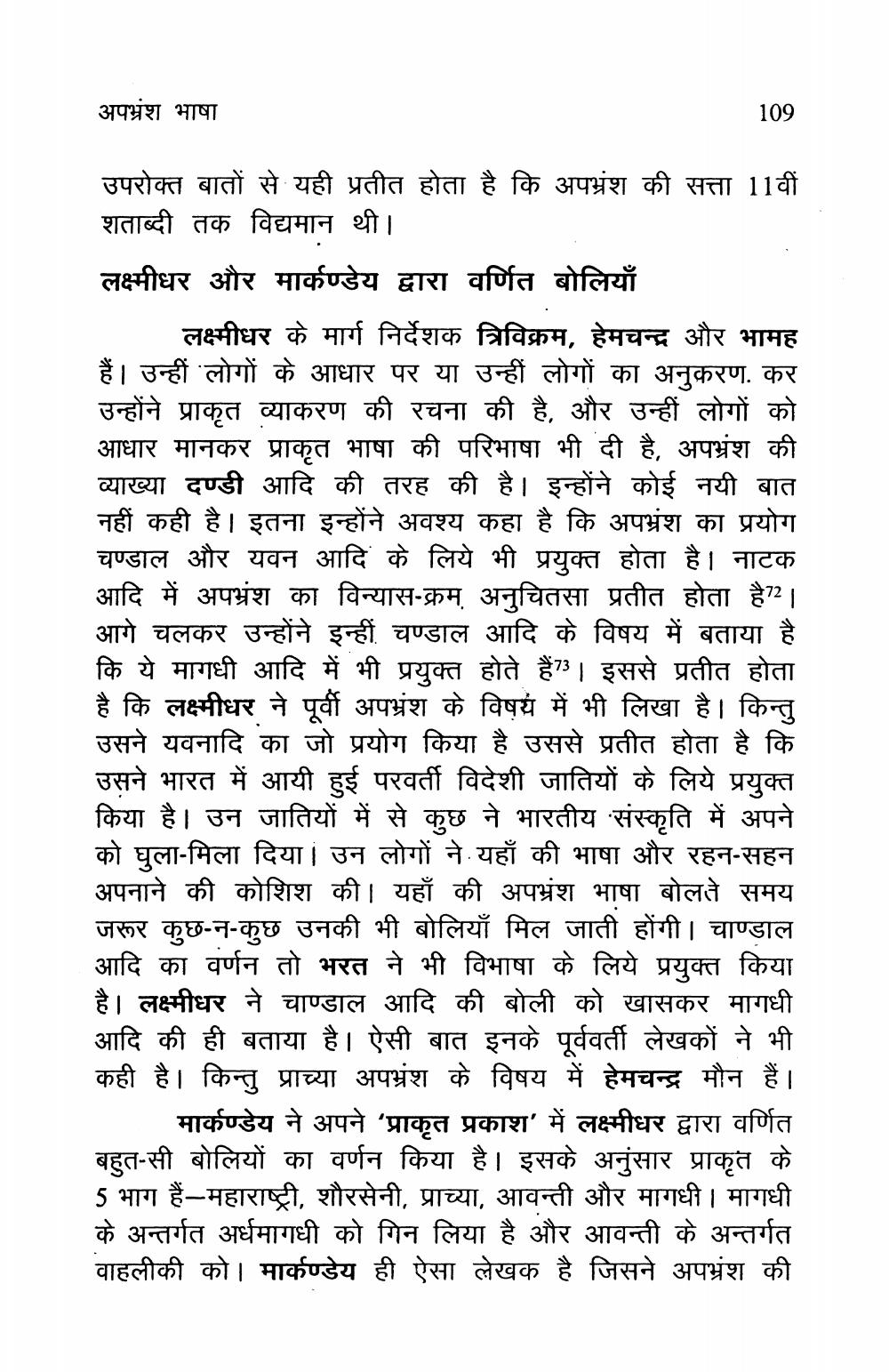________________
अपभ्रंश भाषा
109
उपरोक्त बातों से यही प्रतीत होता है कि अपभ्रंश की सत्ता 11वीं शताब्दी तक विद्यमान थी ।
लक्ष्मीधर और मार्कण्डेय द्वारा वर्णित बोलियाँ
लक्ष्मीधर के मार्ग निर्देशक त्रिविक्रम, हेमचन्द्र और भामह हैं। उन्हीं लोगों के आधार पर या उन्हीं लोगों का अनुकरण कर उन्होंने प्राकृत व्याकरण की रचना की है, और उन्हीं लोगों को आधार मानकर प्राकृत भाषा की परिभाषा भी दी है, अपभ्रंश की व्याख्या दण्डी आदि की तरह की है। इन्होंने कोई नयी बात नहीं कही है। इतना इन्होंने अवश्य कहा है कि अपभ्रंश का प्रयोग चण्डाल और यवन आदि के लिये भी प्रयुक्त होता है। नाटक आदि में अपभ्रंश का विन्यास-क्रम अनुचितसा प्रतीत होता है 72 | आगे चलकर उन्होंने इन्हीं चण्डाल आदि के विषय में बताया है कि ये मागधी आदि में भी प्रयुक्त होते हैं । इससे प्रतीत होता है कि लक्ष्मीधर ने पूर्वी अपभ्रंश के विषय में भी लिखा है । किन्तु उसने यवनादि का जो प्रयोग किया है उससे प्रतीत होता है कि उसने भारत में आयी हुई परवर्ती विदेशी जातियों के लिये प्रयुक्त किया है। उन जातियों में से कुछ ने भारतीय संस्कृति में अपने को घुला- मिला दिया । उन लोगों ने यहाँ की भाषा और रहन-सहन अपनाने की कोशिश की । यहाँ की अपभ्रंश भाषा बोलते समय जरूर कुछ-न-कुछ उनकी भी बोलियाँ मिल जाती होंगी । चाण्डाल आदि का वर्णन तो भरत ने भी विभाषा के लिये प्रयुक्त किया है । लक्ष्मीधर ने चाण्डाल आदि की बोली को खासकर मागधी आदि की ही बताया है। ऐसी बात इनके पूर्ववर्ती लेखकों ने भी कही है। किन्तु प्राच्या अपभ्रंश के विषय में हेमचन्द्र मौन हैं। मार्कण्डेय ने अपने ‘प्राकृत प्रकाश' में लक्ष्मीधर द्वारा वर्णित बहुत-सी बोलियों का वर्णन किया है। इसके अनुसार प्राकृत के 5 भाग हैं - महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, आवन्ती और मागधी । मागधी के अन्तर्गत अर्धमागधी को गिन लिया है और आवन्ती के अन्तर्गत वालीकी को । मार्कण्डेय ही ऐसा लेखक है जिसने अपभ्रंश की
1