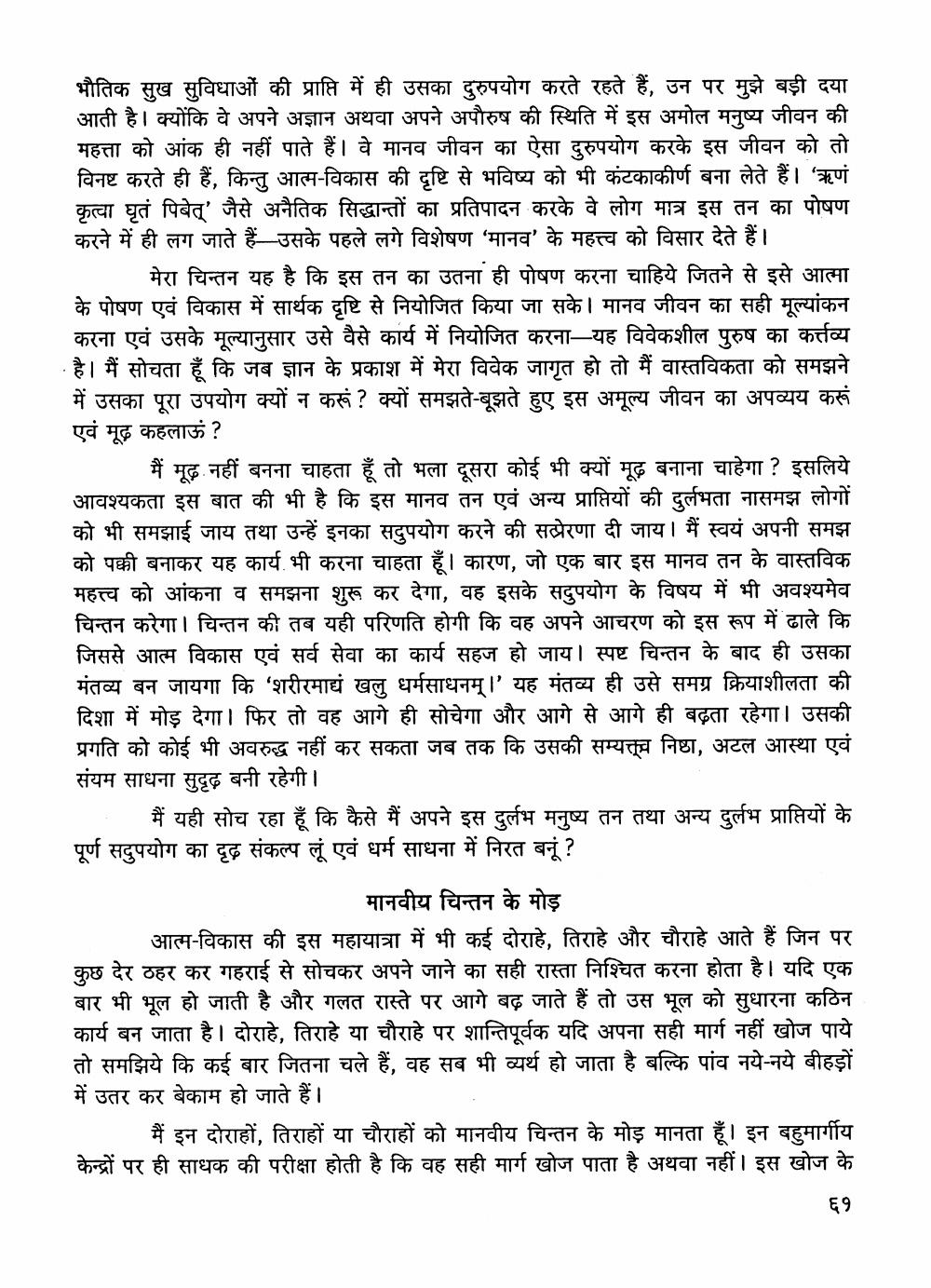________________
भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति में ही उसका दुरुपयोग करते रहते हैं, उन पर मुझे बड़ी दया आती है। क्योंकि वे अपने अज्ञान अथवा अपने अपौरुष की स्थिति में इस अमोल मनुष्य जीवन की महत्ता को आंक ही नहीं पाते हैं। वे मानव जीवन का ऐसा दुरुपयोग करके इस जीवन को तो विनष्ट करते ही हैं, किन्तु आत्म-विकास की दृष्टि से भविष्य को भी कंटकाकीर्ण बना लेते हैं। 'ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्' जैसे अनैतिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करके वे लोग मात्र इस तन का पोषण करने में ही लग जाते हैं उसके पहले लगे विशेषण 'मानव' के महत्त्व को विसार देते हैं।
मेरा चिन्तन यह है कि इस तन का उतना ही पोषण करना चाहिये जितने से इसे आत्मा पण एवं विकास में सार्थक दृष्टि से नियोजित किया जा सके। मानव जीवन का सही मूल्यांकन करना एवं उसके मूल्यानुसार उसे वैसे कार्य में नियोजित करना—यह विवेकशील पुरुष का कर्तव्य है। मैं सोचता हूँ कि जब ज्ञान के प्रकाश में मेरा विवेक जागृत हो तो मैं वास्तविकता को समझने में उसका पूरा उपयोग क्यों न करूं? क्यों समझते-बूझते हुए इस अमूल्य जीवन का अपव्यय करूं एवं मूढ़ कहलाऊं?
__मैं मूढ़ नहीं बनना चाहता हूँ तो भला दूसरा कोई भी क्यों मूढ़ बनाना चाहेगा? इसलिये आवश्यकता इस बात की भी है कि इस मानव तन एवं अन्य प्राप्तियों की दुर्लभता नासमझ लोगों को भी समझाई जाय तथा उन्हें इनका सदुपयोग करने की सत्प्रेरणा दी जाय । मैं स्वयं अपनी समझ को पक्की बनाकर यह कार्य भी करना चाहता हूँ। कारण, जो एक बार इस मानव तन के वास्तविक महत्त्व को आंकना व समझना शुरू कर देगा, वह इसके सदुपयोग के विषय में भी अवश्यमेव चिन्तन करेगा। चिन्तन की तब यही परिणति होगी कि वह अपने आचरण को इस रूप में ढाले कि जिससे आत्म विकास एवं सर्व सेवा का कार्य सहज हो जाय। स्पष्ट चिन्तन के बाद ही उसका मंतव्य बन जायगा कि 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् ।' यह मंतव्य ही उसे समग्र क्रियाशीलता की दिशा में मोड़ देगा। फिर तो वह आगे ही सोचेगा और आगे से आगे ही बढ़ता रहेगा। उसकी प्रगति को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सम्यक्त्व निष्ठा, अटल आस्था एवं संयम साधना सुदृढ़ बनी रहेगी।
मैं यही सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन तथा अन्य दुर्लभ प्राप्तियों के पूर्ण सदुपयोग का दृढ़ संकल्प लूं एवं धर्म साधना में निरत बनूं ?
मानवीय चिन्तन के मोड़ आत्म-विकास की इस महायात्रा में भी कई दोराहे, तिराहे और चौराहे आते हैं जिन पर कुछ देर ठहर कर गहराई से सोचकर अपने जाने का सही रास्ता निश्चित करना होता है। यदि एक बार भी भूल हो जाती है और गलत रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं तो उस भूल को सुधारना कठिन कार्य बन जाता है। दोराहे, तिराहे या चौराहे पर शान्तिपूर्वक यदि अपना सही मार्ग नहीं खोज पाये तो समझिये कि कई बार जितना चले हैं, वह सब भी व्यर्थ हो जाता है बल्कि पांव नये-नये बीहड़ों में उतर कर बेकाम हो जाते हैं।
मैं इन दोराहों, तिराहों या चौराहों को मानवीय चिन्तन के मोड़ मानता हूँ। इन बहुमार्गीय केन्द्रों पर ही साधक की परीक्षा होती है कि वह सही मार्ग खोज पाता है अथवा नहीं। इस खोज के
६१